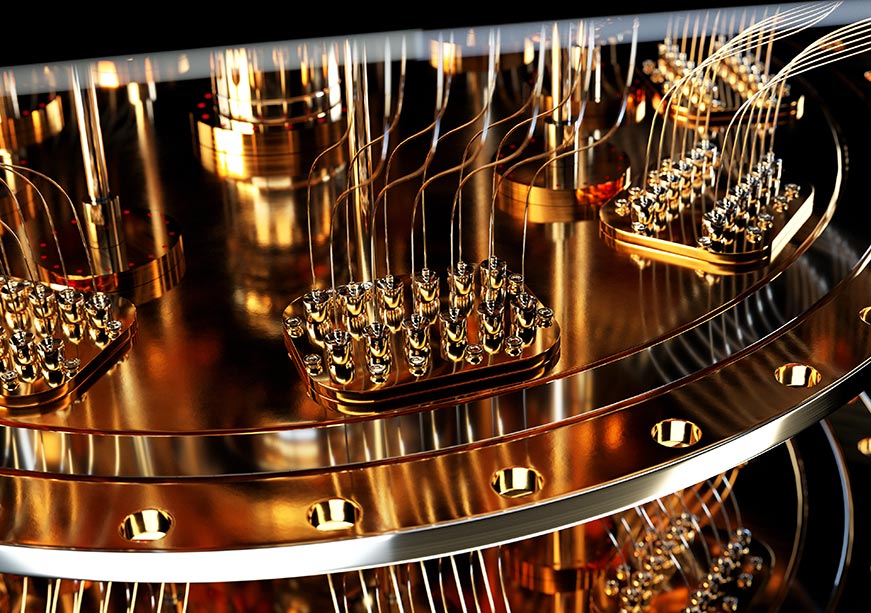प्रस्तावना
भारत की विदेश नीति अब रणनीतिक रूप से पुनः संगठित हो गई है और इसमें अब यूनाइटेड स्टेट्स (US) के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर जोर दिया जा रहा है. इस द्विपक्षीय साझेदार को बेहद अहम माना जाता है, जिसमें दोनों साझेदार साझा-चिंताओं की वजह से एक-दूसरे से जुड़े हैं. साझा चिंताओं में अनिवार्य रूप से आतंकवाद का विरोध करने अथवा मुकाबला करने की चिंता शामिल है. निश्चित ही US-भारत के बीच आतंकवाद विरोध को लेकर हो रहा कन्वर्जेन्स दोनों की लगातार मज़बूत होती जा रही साझेदारी की आधारशिला है. हालांकि विश्लेषक अक्सर इस मज़बूत हो रही साझेदारी के लिए अन्य मानकों पर भी ध्यान देने की सिफ़ारिश करते रहते हैं. इन मानकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती, उसकी आबादी तथा चीन के ख़िलाफ़ संतुलन बनाए रखने में भारत की उपयोगिता का समावेश है. इसके अलावा इन विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही देशों के बीच लोकतंत्र मज़बूत होने के कारण भी संबंधों में मज़बूती देखी जाती है. लेकिन US में 9/11 तथा भारत में नवंबर 2008 के आतंकी हमलों के बाद से ही आतंकवाद विरोध को लेकर सहयोग ही एक ऐसा मुद्दा है, जो दोनों देशों के संबंधों में अहम कड़ी बना हुआ है.
US तथा भारत के बीच आतंकवाद विरोध समन्वय एक डायनैमिक प्रोसेस यानी गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें अहम जानकारी साझा करने, ख़तरों का आकलन करने और हिंसक कट्टरपंथियों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस यानी ख़ुफ़िया जानकारी एकत्रित करना शामिल है.
इस ब्रीफ में इस सहयोग की अहमियत पर प्रकाश डालकर इंटेलिजेंस को साझा करने के साथ साझा सैन्य अभ्यास और बहुराष्ट्रीय साझेदारियों जैसे आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्यबल तथा क्वॉड अभ्यास में शिरकत करने को लेकर अहम क्षेत्रों की पहचान की गई है. इस ब्रीफ में आतंकवाद विरोध की कन्वर्जेन्स यानी सम्मिलन के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी बात की गई है.
भारत-US साझेदारी के स्तंभ
इंटेलिजेंस साझाकरण तथा सहयोग
US तथा भारत के बीच आतंकवाद विरोध समन्वय एक डायनैमिक प्रोसेस यानी गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें अहम जानकारी साझा करने, ख़तरों का आकलन करने और हिंसक कट्टरपंथियों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस यानी ख़ुफ़िया जानकारी एकत्रित करना शामिल है. इसी तरह का एक समन्वय हाल ही में मार्च 2024 के सिक्योरिटी डायलॉग[1] को कहा जा सकता है. इसमें दोनों ही देशों ने US की मिट्टी पर खालिस्तान समर्थक तत्वों की मौजूदगी को लेकर साझा चिंता व्यक्त करते हुए मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण को लेकर बातचीत की गई. इसके अलावा एक और अहम बात पर दोनों देशों के बीच 2020 में सहमति बनने के बाद बेसिक एक्सचेंज एंड को-ऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो-स्पेटियल को-ऑपरेशन को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इसके चलते भारत की GEOINT डाटा का उपयोग करने, उसे एकत्रित करने और उसे प्रोसेस करने की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिशों को बल मिला है.[2] 2015 में दोनों देशों ने द जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंर्फोमेशन एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए.[3] इसी प्रकार 2018 में कम्युनिकेशंस कॉम्पैटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट[4] पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी पारस्परिकता और भी मज़बूत हुई. इसमें ख़ुफ़िया जानकारी को साझा करने का भी समावेश है. अपने स्तर पर ही 2016 में दोनों देशों के बीच हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट्स में लॉजिस्टिकल सहायता और ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने के मुद्दे पर ध्यान दे दिया गया था.[5] इसी तरह 2019 का इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी तथा ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने के क्षेत्र में समन्वय को प्रोत्साहित करता है.[6] ये हालिया उदाहरण इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने और आतंकवाद की उभरती युद्ध-नीति को मज़बूत करने को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं.
साझा सैन्य अभ्यास और ऑपरेशंस
भारत तथा US के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें युद्ध अभ्यास (2015), मालाबार (2015), रेड फ्लैग (2016), वज्र प्रहार (2017), टाइगर ट्रायंफ (2019), कोप इंडिया (2020), मिलन-24 (2024) तथा सी डिफेंडर्स (2024) ये सारे अभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं.[7] इन अभ्यासों की वजह से पारस्पारिकता में इज़ाफ़ा होता है और आपसी भरोसा बढ़ने के लिए पोषक माहौल तैयार होता है. इसके अलावा यह दोनों देशों के बीच कूटनीतिक अलाइनमेंट यानी तालमेल को भी दर्शाता है. समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद विरोधी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रीत करने से क्षमता वृद्धि होने के साथ-साथ यह संदेश भी जाता है कि दोनों देशों के रक्षा उद्देश्य साझा है और वे इसे लेकर प्रतिबद्ध है. इसके अलावा इन अभ्यासों को प्रभावी कूटनीतिक संकेत भी माना जाता है, जिसकी वजह से भारत-US के बीच क्षेत्रीय तथा वैश्विक हितधारकों के साथ साझेदारी और भी मज़बूत होकर उनके रिश्ते गहरें होते है.
वर्तमान चुनौतियां
विगत कुछ वर्षों में आतंक-विरोधी उपायों को बढ़ाने की कोशिशों में तेज़ी आने के बाद इस क्षेत्र में प्रगति दिखाई दे रही है. मोदी-बाइडेन साझेदारी को हालांकि साझा उद्देश्य को पूरा करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ये चुनौतियां इन उद्देश्य की राह में रोड़ा बनी हुई हैं. ये चुनौतियां इन देशों के विभिन्न विरोधियों की अपनी-अपनी धारणाओं को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक कारकों की वजह से उभरती हैं. लेकिन एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो ये चुनौतियां ऐसी नहीं हैं कि इनसे निपटा ही न जा सके. व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर इन्हें प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है.
रचनावाद एवं विदेश नीति के बीच होने वाले इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन का विश्लेषण करने वाले विद्वानों का तर्क है कि US एक प्रमुख वैश्विक ताक़त होने की वजह से अक्सर ‘‘मापदंड संशोधनकर्ता’’ की भूमिका अदा करता है और वह अपने हितों को देखकर अंतरर्राष्ट्रीय आदर्शों को आकार देता है.[8] अमेरिकन एक्सेप्शनिलज्म यानी अमेरिकी अनूठावाद ही इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है. इस प्रवृत्ति की वजह से ही US वैश्विक स्तर पर मौजूद कानूनी मानक ढांचे में सुधार की मांग करने पर मजबूर होता है. इसी बीच भारत का आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण US के दृष्टिकोण से भिन्न है, क्योंकि भारत भी एक क्षेत्रीय ताक़त का दर्ज़ा रखता है और उसका भू-राजनीतिक संदर्भ भी भिन्न है. भारत को जहां मुख्यत: क्षेत्रीय समूहों लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद[9] का ही सामना करना पड़ता है, वहीं US को ट्रांसनेशनल खिलाड़ी जैसे अल-क़ायदा और इस्लामिक स्टेट (ISIS) से दो-दो हाथ करने होते हैं.[10] आतंकवादी इकाईयों की शिनाख़्त करने में कुछ मात्रा तक संरेखन होने के बावजूद नीतिगत स्तर पर भिन्नताएं, विशेषत: अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को लेकर, अब भी मौजूद हैं.
उदाहरण के लिए अपने ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए अफ़ग़ानिस्तान में भारत की प्राथमिकता स्थिरता एवं सुरक्षा है. दूसरी ओर US को अफ़ग़ानिस्तान में व्यापक भू-राजनीतिक कारकों पर ध्यान देना है, जो उसके तालिबान के साथ हुए शांति समझौते में परीलक्षित होते हैं.[11] पाकिस्तान को लेकर भारत की वर्तमान सरकार थोड़ा सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाने की वकालत करती है. इसका कारण यह है कि वह इस बात से आशंकित है कि सतर्कता में ढील देने पर सीमा-पार आतंकवाद का ख़तरा बढ़ जाएगा और भारत की सीमा में कट्टरपंथ को अपने पैर जमाने का अवसर मिल जाएगा. दूसरी ओर पाकिस्तान को लेकर US ट्रांसनेशनल दृष्टिकोण अपनाता है और उसे आतंकवाद-विरोध के लिए आर्थिक तथा रक्षा प्रोत्साहन मुहैया करवाता है. US ने पाकिस्तान को F-16 युद्धक विमान भी मुहैया करवाए हैं.[12] इसके अलावा वह इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ भी दोबारा जुड़ गया है.[13]
पाकिस्तान को लेकर भारत की वर्तमान सरकार थोड़ा सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाने की वकालत करती है. इसका कारण यह है कि वह इस बात से आशंकित है कि सतर्कता में ढील देने पर सीमा-पार आतंकवाद का ख़तरा बढ़ जाएगा और भारत की सीमा में कट्टरपंथ को अपने पैर जमाने का अवसर मिल जाएगा.
ईरान के साथ US अपनी ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी के तहत निपटता है. उसने ट्रंप शासनकाल के दौरान भारत को ईरान से तेल का आयात रोकने को कहा था. इसके बदले में US ने कहा था कि वह मसूद अजहर को UN प्रतिबंधों के तहत नामजद करने में सहयोग करेगा. उस वक़्त US का उद्देश्य ईरान के परमाणु विकास को रोकना और आतंकवादी प्रॉक्सी यानी छद्म समूहों के लिए समर्थन ख़त्म करना था.[14] इसके मुकाबले बाइडेन प्रशासन ने कम दबाव डालने वाला दृष्टिकोण अपनाया है. लेकिन प्रतिबंधों की वजह से परमाणु डील अब भी अटकी हुई है. साझा लक्ष्य होने के बावजूद क्षेत्रीय गतिशीलता को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों में मतभिन्नता साफ़ दिखाई देती है.
रणनीति में अंतर
US तथा भारत के आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण में अनेक अंतर इस वजह से भी दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ही देश अपनी रणनीति तैयार करने के लिए अलग रवैया अपनाते हैं और इसी हिसाब से प्रयास करते हैं. उनके दृष्टिकोण को बहुराष्ट्रीय-कूटनीतिक बनाम एकतरफा-सैन्य कार्रवाई की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है. एक ओर जहां वैश्विक ताक़त के रूप में US एकतरफा तथा सैन्य रवैया अपनाना चाहता है, वहीं आतंकवाद के विरोध को लेकर भारत का रवैया उसके क्षेत्रीय स्टेटस और विशिष्ठ सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पक्षपातपूर्ण कहा जा सकता है. भारत का रवैया बहुराष्ट्रीय तथा कूटनीतिक रणनीति की ओर झुकता दिखाई देता है.
भारत अक्सर अपने पड़ोसियों तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ साझा सुरक्षा चिंताओं का हल निकालने तथा आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के मसले पर बातचीत करता रहता है. उदाहरण के लिए भारत ने हमेशा ही सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लगातार कूटनीतिक समर्थन की मांग की है. इतना ही नहीं वह अंतरराष्ट्रीय फोरम और सहयोगात्मक पहल जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन तथा ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन के साथ बातचीत करते हुए वह सुरक्षा पर मंडराने वाले ख़तरों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस-शेयरिंग तथा विशेषज्ञता को महत्वपूर्ण बताकर उसका उपयोग करता है. इसके विपरीत US आतंकवाद के विरोध के लिए एकतरफा तथा सैन्य-केंद्रीत रवैया अपनाता है.
अपनी लंबी दूरी की सैन्य क्षमताओं और वैश्विक पहुंच की वजह से US अक्सर ट्रांसनेशनल आतंकी संगठनों जैसे अल-कायदा, ISIS के ख़िलाफ़ लक्षित सैन्य तथा काइनेटिक यानी गतिज कार्रवाई करता है. इसमें वह अफ़ग़ानिस्तान, सीरिया तथा ईराक के मामले में ड्रोन हमले का उपयोग करता है तो विभिन्न क्षेत्रों में आतंकी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए वह स्पेशल ऑपरेशंस रेड जैसे ऑपरेशन जिरोनिमो, ऑपरेशन रेड डॉन का उपयोग करते हुए अल-कायदा के मुखिया अयमान अल-जवाहिरी का ख़ात्मा करता है. कुल-मिलाकर भारत तथा US दोनों ही आतंकवाद का मुकाबला करने के साझा लक्ष्य पर काम करते हैं, लेकिन भू-राजनीतिक संदर्भ जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताएं और रणनीतिक क्षमताओं की वजह से दोनों का रवैया अलग-अलग होता है.
दृष्टिकोण में यह अंतर इन दोनों देशों के ग़ाज़ा एवं अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनाए जाने वाले भिन्न परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है. ऐतिहासिक रूप से US को इज़राइल का कट्टर समर्थक माना जाता है. वह उसे सैन्य सहायता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के बाद से ही हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कूटनीतिक समर्थन भी देता आया है. लेकिन राफ़ा में चलाए जा रहे अभियान को लेकर US राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच चल रहा विवाद US-इज़राइल के बीच "विशेष संबंधों" में गिरावट को दर्शाता है. इसके बावजूद यह कहना उचित होगा कि इज़राइल को समर्थन करने के मामले में US ने कमोबेश निरंतरता ही बरती है. उधर अपने स्तर पर मोदी सरकार ने इज़राइल का सहयोगी होने के बावजूद हमास के ख़िलाफ़ कम ही बात की है. मोदी सरकार ने आपसी बातचीत के रास्ते शांति बहाली करते हुए एक स्थायी दो राष्ट्र समाधान की पैरवी की है. दो राष्ट्र समाधान के सुझाव का कुछ US प्रशासनों ने समर्थन किया है, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं देखी जाती.
अफ़ग़ानिस्तान के मामले में विशेषत: सितंबर 2001 में हुए हमले के बाद से ही US का दृष्टिकोण सैन्य हस्तक्षेप का रहा है. उसका उद्देश्य यहां मौजूद आतंकी नेटवर्क को ख़त्म करके तालिबान की सरकार को हटाना है. आज US ने "ओवर द होराइजन" यानी क्षीतिज के परे अपनी सैन्य क्षमताओं का उपयोग करते हुए अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने की कोशिश की है.
मोदी सरकार ने आपसी बातचीत के रास्ते शांति बहाली करते हुए एक स्थायी दो राष्ट्र समाधान की पैरवी की है. दो राष्ट्र समाधान के सुझाव का कुछ US प्रशासनों ने समर्थन किया है, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं देखी जाती.
इसी बीच भारत सरकार का अफ़ग़ानिस्तान में दृष्टिकोण विकास, क्षमता वृद्धि और क्षेत्रीय कूटनीति पर आधारित है. भारत ने वहां बुनियादी ढांचे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा में निवेश किया है ताकि अफ़ग़ानिस्तान में स्थिरता एवं आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित किया जा सकें.
निष्कर्ष
मोदी और बाइडेन ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक मज़बूत गठजोड़ स्थापित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हासिल की है. मोदी की अगुवाई में सरकार ने आतंक-विरोधी पहल को मज़बूत करने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं. अब इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रीत किया जाना चाहिए. दोनों ही देशों को अपनी साझेदारी की बहुआयामी प्रकृति को ध्यान में रखकर इसे पुख़्ता करने की आवश्यकता को समझना होगा. इसके लिए एक विस्तृत एवं समावेश रणनीति आवश्यक है जो संबंधित एजेंसियों के बीच अबाधित समन्वय स्थापित करने में सफ़ल हो सके.
भारत-US आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों देशों की नीतियों में अनुरूपता की कमी पर ध्यान दिया जाए. हाल में हुई बैठकों में इसे लेकर तालमेल दिखाई दिया है, लेकिन इसे लेकर की गई पहल बेहद धीमी है. दोनों ही देशों को अपने आतंकवाद विरोधी एजेंडा में उसी तरह का संस्थानीकरण बढ़ाना होगा, जैसा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में बढ़ाता हुआ दिखाई देता है. US ने दक्षिण एशिया में अपनी नीति में डी-हाइफनेशन किया है यानी वह अब भारत तथा उसके पड़ोसियों के बारे में अलग-अलग विचार करने लगा है. ठीक इसी तरह उसे संस्थात्मक, विभाग स्तरीय कड़ियों को आगे बढ़ाना होगा. US होमलैंड सिक्योरिटी प्रशासन आतंकवाद विरोधी समन्वय में ठोस आधार मुहैया करवा सकता है.
US ने दक्षिण एशिया में अपनी नीति में डी-हाइफनेशन किया है यानी वह अब भारत तथा उसके पड़ोसियों के बारे में अलग-अलग विचार करने लगा है. ठीक इसी तरह उसे संस्थात्मक, विभाग स्तरीय कड़ियों को आगे बढ़ाना होगा.
कानून प्रवर्तन के मसले पर दोनों देश के नेताओं ने और नज़दीकी के साथ काम करने का फ़ैसला किया है. उन्होंने क्वॉड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र एवं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे समूहों में भी टीम भावना के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है. उनका लक्ष्य क्षेत्रीय सुरक्षा में इज़ाफ़ा करते हुए एक ख़ुला और स्वतंत्र भारत-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है जो समावेशी होने के साथ ही उसके समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम भी हो.[15]
भारत की ओर से अपनाई गई युद्ध अभ्यास 2019 तथा क्वॉड सदस्य देशों की आतंकवाद विरोधी टेबलटॉप एक्सरसाइज जैसी पहल के कारण यह साफ़ है कि वह भारत-प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद विरोध समन्वय की नई संभावनाओं की ख़ोज कर रहा है.[16] US के साथ अपने संबंधों को संस्थागत करने के लिए भारत को अपने आतंकवाद विरोधी उपकरण का विकेंद्रीकरण करना होगा. इसके लिए वह अमेरिकी मॉडल से प्रेरणा ले सकता है. उसे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र (NSA) के तहत एक डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (DNI) का पद स्थापित करना चाहिए, ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी ख़ुफ़िया जानकारी जुटाने एवं जानकारी का प्रसार करने की प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जा सके. ऐसा होने पर NSA के कार्यालय पर पड़ने वाला दबाब कम होगा और ऑपरेशनल कुशलता भी बढ़ेगी.[17]
भारत में एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र की स्थापना को लेकर पहले किए गए प्रयासों का विरोध होने की वजह से इसमें सफ़लता नहीं मिली है. लेकिन NSA की देखरेख में काम करने वाले चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर की नियुक्ति से इसी तरह के उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है. ऐसा होने पर राज्य से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में खलल भी नहीं पड़ेगा.[18] संस्थागत कड़ियों, भारत-प्रशांत डानैमिक्स तथा नवोचार के मॉडल को अपनाने में प्राथमिकता देकर भारत तथा US एक मज़बूत और टिकाऊ साझेदारी को फलने-फुलने का मौका दे सकते हैं. यह आतंकवाद विरोधी साझेदारी क्षेत्रीय जटिलताओं और व्यापक राष्ट्रीय मतभेदों से परे होगी.
क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के बीच कॉमन ग्राउंड ख़ोजने के लिए एक-दूसरे के परिप्रेक्ष्य को सुक्ष्मता के साथ समझना आवश्यक है. फिर चाहे एकतरफा अथवा बहुराष्ट्रीय, कूटनीतिक या सैन्य दृष्टिकोण हो यह आवश्यक है कि वर्तमान में चल रहे समन्वय को आगे बढ़ाते हुए आतंकवाद की ओर से पेश होने वाली बहुआयामी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए साझा प्रतिबद्धता आवश्यक है. उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने और भारत-US के बीच पनप रही साझेदारी को मज़बूत बनाने के लिए भविष्य में कूटनीतिक सिफ़ारिशों का आधार लिया जा सकता है.
एक ओर जहां स्थापित सलाहकार मंच कुशलतापूर्वक काम कर रहे है, वहीं आतंकवाद विरोधी सहयोग को अन्य मुद्दों से जुड़े विवादों से दूर रखने को लेकर अनेक चुनौतियां दिखाई देती हैं. उदाहरण के लिए डाटा लोकलाइजेशन के मुद्दे पर द्विपक्षीय मतभेदों की वजह से सहयोग चैनल्स को उन्नत करने का काम अटका हुआ है. दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को दूर करने के लिए संस्थागत कड़ियां स्थापित करनी होगी.
Endnotes
[1] “Joint Statement of the 20th U.S.- India Counterterrorism Joint Working Group (CTJWG) and 6th Designations Dialogue,” Ministry of External Affairs.
[2] Ministry of Defence, Government of India, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm. aspx?PRID=1667841
[3] Rakesh Sood, comment on “The India-US Defence Partnership is Deepening,” Observer Research Foundation, comment posted on October 30, 2020, https://www. orfonline.org/research/the-india-us-defence-partnership-is-deepening
[4] Ankit Panda, “What the Recently Concluded US-India COMCASA Means,” The Diplomat, September 9, 2018.
[5] Ministry of Defence, Government of India, https://archive.pib.gov.in/newsite/ PrintRelease.aspx?relid=149322
[6] Ministry of Defence, Government of India, https://archive.pib.gov.in/newsite/ PrintRelease.aspx?relid=149322
[7] Congressional Research Service, Government of the United States, “India-US: Major Arms Transfers and Military Exercise,” December 14, 2023, https://sgp.fas.org/crs/ row/IF12438.pdf
[8] Ian Hurd, “Breaking and Making Norms: American Revisionism and Crises of Legitimacy,” International Politics, 44 (2007): 194.
[9] Soumya Chaturvedi, “Is Terrorism Declining in India?,” The Diplomat, January 8, 2021, https://thediplomat.com/2021/01/is-terrorism-declining-in-india/
[10] Robin Wright et al., “The Jihadi Threat SIS, Al Qaeda, and Beyond,” United States Institute of Peace and Wilson Center, 2016, https://www.usip.org/sites/default/ files/The-Jihadi-Threat-ISIS-Al-Qaeda-and-Beyond.pdf
[11] Kashish Parpiani and Prithvi Iyer, “Towards an India-US Consensus on Counterterrorism Cooperation,” ORF Occasional Paper No. 240, Observer Research Foundation, April 2020, https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/04/ ORF_Occasional_Paper_240_India-US-Counter_terrorism_NEW.pdf
[12] Shamil Shams, “US Approves Support for Pakistan’s F-16s,” DW News, July 27, 2019, https://www.dw.com/en/us-approves-support-for-pakistans-f-16s-amid-afghanistan-outreach/a-49766828
[13] “Pakistan to Rejoin Frozen US Military Training,” Arab News, December 24, 2019, https://www.arabnews.pk/node/1603271/pakistan
[14] Shubhajit Roy, “US to India: Helping You on Masood Azhar, So End Iran Oil Imports,” The Indian Express, April 24, 2019, https://indianexpress.com/ article/india/us-to-india-helping-you-on-masood-azhar-so-end-iran-oil-imports-5691315/
[15] “Joint Statement of the 20th US- India Counterterrorism Joint Working Group,” U.S. Department of State, March 7, 2024, https://www.state.gov/joint-statement-of-the-20th-u-s-india-counterterrorism-joint-working-group/
[16] National Investigation Agency (Ministry of Home Affairs), https://nia.gov.in/ writereaddata/Portal/News/503_1_Pr.pdf
[17] Parpiani and Iyer, “Towards an India-US Consensus on Counterterrorism Cooperation”
[18] Parpiani and Iyer, “Towards an India-US Consensus on Counterterrorism Cooperation”
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.



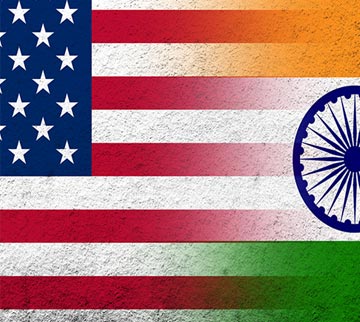

 PREV
PREV