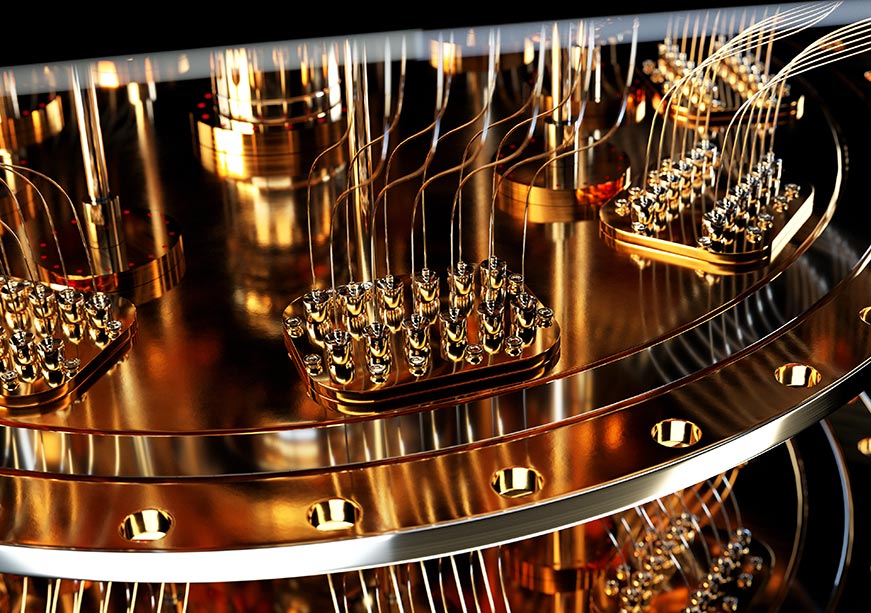प्रस्तावना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी उभरती हुई तकनीकी इक्कीसवीं सदी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होंगी. वर्चुअल रियलिटी (VR) ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCIs)जैसे अग्रणी तकनीकों में तेज़ी से हो रहा विकास दुनिया की हर सरकार के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहा है. तकनीकी क्षेत्र में नई खोज की बहुत तेज़ गति, एआई को विकसित करने वाले और गैर विशेषज्ञों द्वारा अपने उत्पाद बेचने की अराजक और सनसनीखेज़ विपणन नीतियों पर चर्चा करने का वक्त आ गया है. इन उभरती तकनीकों से समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में जो प्रभाव पड़ेगा, उस पर सार्थक सामाजिक-राजनीतिक बहस की मांग होनी चाहिए. हालांकि नीति निर्माताओं और विश्लेष्कों के सामने भी एक अनूठी चुनौती है. उन्हें ऐसी उभरती तकनीकों पर चर्चा करनी है, जो लगातार विकसित हो रही हैं.
तकनीकी विकास की तेज़ दर और मानव जाति के तकनीकी भविष्य पर अलग-अलग और व्यापक राय की वजह से सामाजिक-राजनीतिक चर्चा में विज्ञान कथाओं की प्रासंगकिता और बढ़ेगी. इस क्षेत्र में काम कर रहे शोधकर्ता एक तरफ ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंट एआई का सपना कभी पूरा नहीं होगा. लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं.
ये मुद्दा सबसे पहले 2017 में तब सामने आया जब यूरोपीय संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति पर बहस चल रही थी. इस चर्चा के बाद एआई पर दुनिया का पहला नीति दस्तावेज़ सामने आया, जिसमें एआई के संभावित प्रभावों पर बात हुई और यूरोपीय संसद ने रोबोटिक्स के लिए अपने नागरिक कानूनों को अपनाया.[1]
बहस की शुरूआत में विज्ञान कथाओं को कई संदर्भों का ज़िक्र हुआ. जैसे कि मैरी शेली की फिल्म फ्रैंकस्टीन, चेकोस्लॉवाकिया के लेकर कारेल कैपेक द्वारा 1921 में 'रोबोट' शब्द के इस्तेमाल और 1943 में प्रकाशित इसाक असिमोव की लघु कहानी रनअराउंड में बताए गए रोबोटिक्स के तीन नियमों पर बात हुई. बहस के दौरान संसद ने यूरोपीय कमीशन से एक ऐसा नागरिक कानून नियम का प्रस्ताव पेश करने की अपील की, जिसमें "लंबी अवधि में रोबोट्स को एक विशिष्ट कानूनी पहचान" देने की बात हो.[2] ये अनुरोध इस धारणा को ध्यान में रखते हुए किया गया कि भविष्य में रोबोट एक कर्मचारी के तौर पर एआई के ढांचे के तहत संचालित हो रहे होंगे. रोबोट्स के अंदर थोड़ी चेतना आ जाएगी और उन्हें AI के साथ मिला दिया जाएगा. यूरोपीय संसद ने ये भी सिफारिश की थी कि इसाक असिमोव के रोबोटिक्स के तीन कानूनों को "रोबोट के डिज़ाइनर्स, निर्माताओं और संचालित करने वालों पर लागू माना जाए. इसमें वो रोबोट भी शामिल हों, जिनके अंदर स्व शिक्षा और पूर्ण स्वायत्ता की विशेषता है".[3] यूरोपीय संसद में हुई बहस को सात साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक ना तो संवेदनाओं वाले रोबोट बनाए जा सके हैं, ना ही एक मज़बूत एआई ढांचा विकसित हो पाया है. अगर विज्ञान कथाओं को छोड़ दें तो भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है. यूरोपीय संसद में हुई बहस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपेक्षित शासन की कोशिशों पर अग्रिम तकनीकों का किस तरह सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है. इस लेख में ये भी दलील दी गई है कि तकनीकी-सांस्कृतिक गेसॉल्ट पर उनके प्रभाव की वजह से विज्ञान कथाओं के नैरेटिव को नीति ढांचे और उभरती तकनीकों के बारे में जानकारी देने में इस्तेमाल किया जा सकता है.
तकनीकी विकास की तेज़ दर और मानव जाति के तकनीकी भविष्य पर अलग-अलग और व्यापक राय की वजह से सामाजिक-राजनीतिक चर्चा में विज्ञान कथाओं की प्रासंगकिता और बढ़ेगी. इस क्षेत्र में काम कर रहे शोधकर्ता एक तरफ ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंट एआई का सपना कभी पूरा नहीं होगा.[4] लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं. जैसे कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ज्यॉफ्री हिंटन. हिंटन 2018 के ट्यूरिंग अवॉर्ड के विजेता है. [a] उन्हें अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर भी कहा जाता है. हिंटन ने एआई क्षेत्र में तेज़ी से विकास और इससे पैदा होने वाले ज़ोखिमों पर चिंता जताते हुए गूगल से अपने पद से इस्तीफा दे दिया.[5] इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा था कि महामारी और युद्ध के ख़तरों के साथ-साथ एआई से मानव जाति के विलुप्त होने के ख़तरों को कम करना भी वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए.[6] एआई को लेकर इन दो चरम सीमाओं के बीच लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ है. जीपीटी-4 जैसे टेक्स्ट जेनरेशन प्लेटफॉर्म ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. इमेज जेनरेशन के लिए DALL-E और मिडजर्नी जैसे ऐप विकसित किए गए हैं. मार्क ज़ुकरबर्ग भी रीयल टाइम फोटोरियलिस्टिक अनुभव के लिए मेटावर्स लेकर आए हैं.[7] इस उद्योग के दिग्गज भी ये मान रहे हैं कि अगले एक दशक के भीतर इस बात की पूरी संभावना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एआई प्लेटफॉर्म से स्वायत्त बनने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं.[8] ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक मंच पर आए और इन अग्रिम तकनीकों का विश्लेषण कर उन्हें नियमित करने पर चर्चा करें.
नीति तय करने वाले गलियारों में इस बात का अहसास बढ़ रहा है कि जितने व्यापाक पैमाने पर और जिस रफ़्तार से नए तकनीकी मंच उभरकर सामने आ रहे हैं, वैसे में वैज्ञानिक परिकल्पना और विज्ञान कथाओं से अपेक्षाओं में अंतर करना मुश्किल हो गया है.[9] इसके अलावा जिस गति से नई तकनीकी खोजें हो रही हैं, उसने नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के सामने ये चिंता पैदा कर दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों पर इनका क्या प्रभाव होगा. उदाहरण के लिए जेनेरेटिव एआई के क्षेत्र में जिस तेज़ी से विकास हो रहा है, उसे देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस ने सितंबर 2023 में एआई के नियमन फोरम का आयोजन किया. इसमें टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटावर्स के सीईओ समेत कई दिग्गज़ शामिल हुए.[10] इसके अलावा अक्टूबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि एआई का विकास तो हो लेकिन साथ ही इसके संभावित ज़ोखिमों का भी ध्यान रखा जाए.[11] लेकिन इस वक्त चीन एआई से जुड़ी ज़्यादातर तकनीकों का अगुआ बना हुआ है. 2021 में कंप्यूटिंग तकनीकी के विकास के बाद से चीन सरकार ने सोशल मीडिया और सर्च इंजन को लेकर नियम और एल्गोरिदम अनुशंसाएं प्रकाशित की हैं. चीन ने 2022 में कृत्रिम रूप से बनाए गए कंटेंट के लिए नियम बनाए. 2023 में उसे चैट जीपीटी जैसे जेनेरेटिव एआई प्लेटफॉर्म के नियमन की नीति बनाई.[12] पारंपरिक नीति निर्धारण के ढांचे के अलावा ये लेख इस बात का भी दावा करता है सांस्कृति उत्पाद, खासकर विज्ञान कथाओं का नैरेटिव तकनीकी संस्कृति या 'इंजीनियरिंग संस्कृति' से भी गहरे रूप से जुड़ी है.[13] ये विज्ञान कथाएं सामाजिक-राजनीतिक बहस को आकार देने और वैश्विक तौर पर तकनीकी खोजों के लिए सैंडबॉक्स की तरह काम कर सकती हैं.
एक विधा के रूप में विज्ञान कथाओं का उभरती तकनीकी को लेकर कल्पना और चिंतन के ज़रिये सामाजिक धारणाओं और नीतिगत विचारों को प्रभावित करने का समृद्ध इतिहास रहा है. आम तौर में ये माना जाता है कि विज्ञान कथा के ज़रिये तकनीकी को बढ़ाचढ़ाकर और सनसनीखेज़ करके दिखाया जाता है. लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि इन विज्ञान कथाओं से हमें भविष्य में विकसित हो सकने वाली तकनीकी और उसके भीतर मौजूद गुप्त ख़तरों और पूर्वाग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. इस बात का उदाहरण जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में मिलता है. हालांकि उस किताब में पैनोप्टीकॉन जैसी निगरानी राज्य की तकनीक अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर सरकार के ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण से पैदा होने वाले ख़तरों का रूपक तो बन ही गया है. इसी तरह टर्मिनेटर सीरीज़ की फिल्म के स्काईनेट में एआई के चित्रण ने लोगों की चेतना में मशीन आधारित भविष्य की धारणा को शामिल कर लिया है, खासकर लोकप्रिय मीडिया में. इसी का असर है कि अब लोग AI क्षेत्र में विकसित किए जा रहे स्वायत्त हथियारों के नियमन की मांग कर रहे हैं.[14] हालांकि एआई के विद्रोह का विचार अब भी उतना ही अटकलबाजियों वाला है, जितना 1980 के दशक में था लेकिन दुनियाभर में सांस्कृतिक चेतना में इनकी स्थायी मौजूदगी तकनीकी ढांचे के विकास में नैरेटिव की गंभीरता को दिखाते हैं. इस तरह की विज्ञान कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं “क्योंकि वो दुनिया को लेकर हमारी समझ और इसके पुनर्निमाण का आधार हैं. क्योंकि कहानियां, कल्पनाएं, उस पर चिंतन-मनन करना और भौतिकता सब एक-दूसरे से घनिष्ठ तरीके से जुड़े हैं.”[15] ये दमदार नैरेटिव ना सिर्फ़ हमें आकर्षित करते हैं बल्कि तकनीकी विकास के दीर्घकालिक सामाजिक-सांस्कृतिक और नैतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं. ये नीतिगत विमर्श में विज्ञान कथा विधा के योगदान को दिखाता है. इस लेख में यही तर्क दिया गया है कि नीतिगत फैसलों को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने और तकनीकी की अवधारणा और विकास में विज्ञान कथाएं किस तरह अनूठी भूमिका निभा सकती हैं.
विज्ञान कथाएं और तकनीकी अविष्कार
वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ विज्ञान कथाओं को अक्सर मौजूदा वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और भविष्य की तकनीक या टेक्नोलॉजी को लेकर जनता की उम्मीदें कम करने के रूप में देखते हैं. ये सच है कि कई भविष्यवादी कल्पनाएं अवास्तविक हैं, उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है लेकिन इस विधा का उद्देश्य भविष्यवाणी करना नहीं संभावित भविष्य की खोज करना है, जो उभरते तकनीकी रूझानों के लिए रचनात्मक क्षेत्र के रूप में काम करता है. उदाहरण के लिए 2011 में समीक्षकों द्वारा सराही गई ब्लैक मिरर सीरीज में वर्चुअल रियलिटी, सोशल मीडिया, रोबोट डॉग और ड्रोन जैसे मौजूदा तकनीकों की बात की गई थी और वर्तमान रूझानों के हिसाब से उग्र भविष्य का अनुमान लगाया गया था.[16] हालांकि, ये विधा सिर्फ सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणियों तक ही सीमित नहीं है. इसकी वजह से कई अविष्कार भी हुए. फिर चाहे वो रोज़मर्रा के काम में आने वाले मोबाइल फोन की बात ही क्यों न हो. मोटोरोला के मार्टिन कूपर फ्लिप फोन के डिज़ाइन का श्रेय स्टार ट्रेक के कम्युनिकेटर को देते हैं. इस तरह अगर देखा जाए तो विज्ञान कथाएं मानव कल्पना की सीमा को कुछ नया और कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं जिससे वास्तविक दुनिया में तकनीकी अविष्कार हों.[17]
विज्ञान कथाओं से विज्ञान का प्रेरित होना कोई नई बात नहीं है. उन्नीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में ही ये दिखने लगा था. उदाहरण के लिए अमेरिकी अविष्कारक साइमन लेक ने 1898 में अर्गोनॉट नाम की पहली ऑपरेटिंग पनडुब्बी बनाई. साइमन लेक का कहना था कि उन्हें इसकी प्रेरणा जूल्स वर्ने की किताब “ट्वेंटी थाउज़ेंड लीग्स अंडर द सी” किताब से मिली. इस किताब को पढ़कर उनमें पानी के अंदर यात्रा करने और वहां की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई.[18] अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर भी विज्ञान कथाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है. खासकर जूल्स वर्ने और एचजी वेल्स की कहानियों का रॉकेट के क्षेत्र में काम करने वाले शुरूआती वैज्ञानिकों कॉन्स्टेंटिन त्स्लोकोव्सकी, हर्मन ओबर्थ और रॉबर्ट गोडार्ड पर गहरा असर पड़ा. जूल्स वर्ने की 1866 में प्रकाशित किताब फ्रॉम अर्थ टू मून पढ़कर त्स्लोकोव्सकी को रासायनिक ईधन वाले मल्टीस्टेज रॉकेट का इस्तेमाल करके पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने वाले पलायन वेग को हासिल करने वाले वृद्धिशील गतिवर्द्धन का विचार मिला. वर्ने की किताबों ने हरमन ओबर्थ को भी प्रभावित किया. हालांकि उनका काम सैद्धांतिक ही रहा.[19] इसके विपरीत रॉबर्ट गोगार्ड दुनिया का पहला तरल ईधन वाला रॉकेट बनाने में कामयाब हुए. 1926 में इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया. बाद में गोगोर्ड ने कहा कि एचजी वेल्स की किताब 'वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स' पढ़ने के बाद उन्होंने अपना जीवन अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को समर्पित करने का फैसला किया.[20]
विज्ञान कथाओं से विज्ञान का प्रेरित होना कोई नई बात नहीं है. उन्नीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में ही ये दिखने लगा था. उदाहरण के लिए अमेरिकी अविष्कारक साइमन लेक ने 1898 में अर्गोनॉट नाम की पहली ऑपरेटिंग पनडुब्बी बनाई. साइमन लेक का कहना था कि उन्हें इसकी प्रेरणा जूल्स वर्ने की किताब “ट्वेंटी थाउज़ेंड लीग्स अंडर द सी” किताब से मिली.
20वीं सदी के आगे बढ़ने के साथ-साथ विज्ञान कथाओं और तकनीकी का ओवरलैप भी बढ़ता गया. खासकर 1980 के दशक में कंप्यूटर, दूरसंचार और जनसंचार के माध्यमों के बढ़ने के बाद इसमें और तेज़ी आई. इसी दौरान विज्ञान कथाओं की नई चीजें मुख्यधारा में शामिल होने लगीं. पहले हम आकाशगंगा, ‘दूर’, ‘बहुत दूर’ की काल्पनिक बातें करते थे. अब उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस और इंटरनेट ने ले ली. इस उभरती हुई उपविधा को ‘साइबरपंक’ कहा गया. इस बार काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं और फिल्में भी बन चुकी हैं. [b] अब अंतरिक्ष से ज़्यादा बातें शहरों में तकनीकी विकास की कल्पनाओं को लेकर होती हैं. खासकर पश्चिमी देशों में. इस चीज पर सबसे ज़्यादा काम सिलिकॉन वैली में हुआ है क्योंकि 20वीं सदी में तकनीकी अविष्कार की धुरी सिलिकॉन वैली ही है. भारत में साइबरपंक की कहानियां कभी-कभार ही आईं, वो भी 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और सूचना-प्रौद्योगिकी सेक्टर में आए उछाल के बाद[21]. अगर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम की बात करें तो अमिताभ घोष की किताब कलकत्ता क्रोमोसोम्स (1995) मंजुला पद्मनाभन की हार्वेस्ट (1997) सुमित बसु की द सिमोकिन प्रोफेसीज़ (2001) और अनिल मेनन की बीस्ट विद अ बिलियन फीट (2008) का ध्यान आता है. पश्चिमी वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति अभी एक विकासशील अर्थव्यवस्था की है. ऐसे में इस सदी में भारत की विज्ञान कथाओं में औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण और तकनीकी विकास की ज़रूरत और नव सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के बीच संघर्ष वाला नैरेटिव दिखता है.[22] अगर पश्चिमी देशों के कुछ प्रमुख साइबरपंक कामों को देखें जो वैश्विक सांस्कृतिक और तकनीकी गेस्टाल्ट पर हावी थे तो वो हैं ट्रॉन (1982), ब्लेड रनर (1982), द टर्मिनेटर (1984), रोबोकॉप (1987), और मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी (1999-2003). ये सब नैरेटिव एक ऐसे बड़े पैमाने पर शहरी डायस्टोपियन दुनिया में दिखाए गए, जहां बड़े-बड़े शहरों को शक्तिशाली कंपनियां नियंत्रित कर रही हैं. इन कंपनियों के पास इतने सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक अधिकार हैं, जितने सरकारों के पास भी नहीं हैं. कहानियों में भी ऐसा समाज दिखाया गया है, जहां ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस और कृत्रिम अंगों पर निर्भर पात्र एक साथ मौजूद हैं.
इस उपविधा का डिजिटल तकनीक के भविष्य और आजकल आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी शब्दों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है. उदाहरण के लिए 2018 में यूरोपीय संसद में AI पर हुई चर्चा को ही ले लीजिए. इसमें कहा गया है कि “AI पर आधारित सिस्टम पूरी तरह सॉफ्टवेयर पर आधारित हो सकते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में काम कर सकते हैं.”[23] यहां ‘वर्चुअल वर्ल्ड’ शब्द का इस्तेमाल होना दिलचस्प है क्योंकि ये शब्द अस्तित्व में ही नहीं था. ये शब्द इंटरनेट और कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित सूचना के स्थान संबंधी गुण को बताता है. हालांकि ऐसी कोई जगह या “दुनिया” नहीं है, जहां डिजिटल जानकारी मौजूद हो. ये धारणा विलियम गिब्सन के 1984 में प्रकाशित उपन्यास न्यूरोमैंसर से आई, जिसने ‘साइबर स्पेस’, सुपर इंटेलिजेंट AI और वर्चुअल रियलिटी जैसी धारणाओं को मुख्यधारा की संस्कृति में स्थापित किया.[24] गिब्सन 1980 के बाद से ही सिलिकॉन वैली को तकनीकी संस्कृति से जुड़े थे. उनका तकनीकी विशेषज्ञों और उद्यमियों से विचारों का आदान-प्रदान होता रहता था. इन लोगों में जारोन लानियर भी शामिल थे, जिन्हें वर्चुअल रियलिटी पर सबसे पहले काम करने का श्रेय जाता है. लानियर ने भी ये बात स्वीकार की है कि उनके काम पर गिब्सन की कथाओं का असर पड़ा. ये बात भी विज्ञान कथाओं और तकनीकी विकास के बीच की पारस्परिक आदान-प्रदान को दिखाती है.[25]
स्टीफेंसन के साहित्य में साइबरपंक के एआई और वर्चुअल रियलिटी जैसे जो तत्व थे. उसने उनके प्रभाव को साहित्य जगह से आगे तक फैलाया. स्टीफेंसन के उपन्यास स्नो क्रैश की कहानी निकट भविष्य में अमेरिका में आभासी वास्तविकता के प्रभुत्व वाले क्षेत्र मेटावर्स में घटती हैं.
गिब्सन के साइबरपंक साहित्य से प्रेरित होकर मार्क पीस ने 1990 के दशक की शुरूआत में जब VRML (वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज) को विकसित किया था, तब उसका उद्देश्य इंटरनेट का एक स्थानिक आयाम देना था.[26] VRML को हाइपरटेक्स्ट्स, यूआरएल और वेबपेजों के इंटरनेट के वेब में ग्राफिक रूप से तीसरा आयाम जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था. हालांकि, तकनीकी दिक्कतों और लागत की कठिनाइयों की वज़ह से इस पर काम आगे नहीं बढ़ सका लेकिन ये विचार ज़िंदा रहा. कहा जाता है कि ये विचार नील स्टीफेंसन की रचनाओं स्नो क्रैश (1992) और क्रिप्टोनोमिकॉन (1999) से प्रभावित था. स्टीफेंसन के साहित्य में साइबरपंक के एआई और वर्चुअल रियलिटी जैसे जो तत्व थे. उसने उनके प्रभाव को साहित्य जगह से आगे तक फैलाया. स्टीफेंसन के उपन्यास स्नो क्रैश की कहानी निकट भविष्य में अमेरिका में आभासी वास्तविकता के प्रभुत्व वाले क्षेत्र मेटावर्स में घटती हैं. इस कथा का नायक वास्तविक दुनिया में एक माफिया के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाले और मेटावर्स में एक योद्धा और एक हैकर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है. यहां वो एक युवा स्केटबोर्ड कूरियर से मिलता है. दोनों एक साथ मिलकर एक साज़िश का पर्दाफाश करते हैं. ये साज़िश एक नई ड्रग और 'स्नो वायरस' नाम के एक कंप्यूटर वायरस के इर्द-गिर्द घूमती है. ये वायरस मेटावर्स और वास्तविक दुनिया दोनों ही जगह उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है. जैसे-जैसे वो इस साज़िश की जड़ तक पहुंचते हैं, वो प्राचीन सुमेरियन संस्कृति और भाषा से इसके रिश्तों का खुलासा करते हैं. भाषा, ज्ञान और नियंत्रण से जुड़े विषयों पर नई जानकारी सामने लाते हैं. ये उपन्यास एक ऐसे डिस्टोपियन दुनिया को दिखाता है, जहां कोई केंद्रीय सरकार नहीं है और दुनिया कॉर्पोरेट के फ्रेंचाइज़ी राज्यों में बंटी है. गूगल के जिओ डिवीज़न के पूर्व निदेशक जॉन हैंके ने स्नो क्रैश को 'अर्थ व्यूअर' की प्रेरणा का श्रेय दिया. अर्थ व्यूअर को ही बाद में गूगल अर्थ के रूप में विकसित किया गया.[27] इसके अलावा जेफ़ बेजोस की एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन में भी स्टीफेंसन के रोल को 'भविष्यवादी' बताया गया है. ये तकनीकी अविष्कारों और काल्पनिक कथाओं में स्टीफेंसन के प्रभाव को दर्शाता है. स्नो क्रैश में 'मेटावर्स' शब्द का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टीफेंसन का मौलिक योगदान है. उन्होंने इंटरनेट को व्यापक रूप में देखा. विज्ञान कथाओं को तकनीकी नीतियों के साथ मिलाने में उनका योगदान इस क्षेत्र में उनके प्रभाव को दिखाता है.
समकालीन उदाहरण
ये संयोग ही है कि 1990 के दशक में जब स्टीफेंसन ने इमर्सिव मेटावर्स की अवधारणा दी, उसी वक्त ग्राफ़िक यूज़र इंटरफ़ेस (GUIs) और 1989 में सर टिम बर्नर्स ली द्वारा निर्मित वर्ल्ड वाइड वेब का उदय हो रहा था.[28] GUI प्लेटफॉर्म की मदद से ये दिखाया गया कि स्टीफेंसन की कथाओं में भविष्य का जो साइबर स्पेस दिखाया गया है, वहां रहने और उसका अनुभव करने पर कैसा महसूस होगा. चूंकि, स्टीफेंसन की बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग की थी. यही वजह है कि मेटावर्स का उनका चित्रण बहुत समृद्ध था. मार्क पीस ने 1999 में एमआईटी के फोरम में स्नो क्रैश के कुछ हिस्सों की तुलना "विस्तृत सॉफ्टवेयर डिज़ाइन" से की.[29] अपने काम के लिए स्टीफेंसन को न सिर्फ़ कई साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुए बल्कि उन्होंने अवधारणा का एक ऐसा ढांचा बनाया, जिससे इंजीनियर और टेक्नोलॉजी का विकास करने वाले डेवलपर प्रेरणा ले सकते हैं.
अपने प्रकाशन के बाद से ही स्नो क्रैश ने सिलिकॉन वैली की संस्कृति पर काफी प्रभाव डाला है. पत्रकारों का कहना है कि यहां शायद ही कोई उद्यमी हो जो स्नो क्रैश के विचार से अछूता हो.[30] यहां तक कि साल 2000 में गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने भी माना कि इस किताब ने उन्हें भी बहुत प्रभावित किया क्योंकि इसने अपने वक्त से एक दशक पहले ही तकनीकी विकास का पूर्वानुमान लगा लिया था.[31] लेकिन स्टीफेंसन के काम पर सबसे बड़ी मुहर तब लगी, जब फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग ने दिसंबर 2021 में ये एलान किया कि वो वास्तविक मेटावर्स बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं. ज़ुकरबर्ग ने कहा कि वो ऐसा मेटावर्स बनाना चाहते हैं "जिसमें इंटरनेट सम्मिलित हो. जहां उपयोगकर्ता अनुभव ना लें बल्कि उपयोगकर्ता खुद अनुभव हो".[32] अनुभवात्मक इंटरनेट पर ज़ोर दिया जाना 1990 के दशक में स्टीफेंसन के नज़रिये से मेल खाता है. इस परियोजना पर काम कर रहे कंपनी के वैज्ञानिक डीन एकल्स ने कहा कि एक वक्त पर मार्क ज़ुकरबर्ग ने सभी प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए स्नो क्रैश किताब को पढ़ना अनिवार्य कर दिया था.[33] स्नो क्रैश के प्रति इसी आकर्षण ने 2014 में मेटा को वर्चुअल रियलिटी कंपनी ओकुलस को 3 अरब डॉलर में अधिग्रहित करने के लिए प्रेरित किया.[34]
2021 में ज़ुकरबर्ग की मेटावर्स परियोजना की घोषणा ने प्रचार और अटकलों को बढ़ावा दिया. 2022 में मेटावर्स फैशन वीक हुआ, जिसमें डिजिटल फैशन दिखाया गया.[35] ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक मेटावर्स गेमिंग, ऑनलाइन रिटेल और मार्केटिंग के ज़रिये 5 ट्रिलियन डॉलर की कमाई कर सकता है.[36] फिर भी अक्टूबर 2022 तक मेटा के स्टॉक 70 प्रतिशत तक गिर गए. इसकी एक वज़ह ज़ुकरबर्ग के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता थी.[37] वहीं उपभोक्ताओं की चिंता के केंद्र में मेटावर्स के शुरूआती अवतार थे, जो कार्टून जैसे लग रहे थे.[38] मेटा फोटोरियालिज़्म को बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है. अवतारों पर असली चेहरे जैसे भाव लाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है. ये सब स्टीफेंसन की स्नो क्रैश के समानांतर है.[39] अक्टूबर 2023 में एक पॉडकास्ट 'मेटावर्स पर पहले इंटरव्यू' में ज़ुकरबर्ग ने मेटा की फेशियल ट्रैकिंग तकनीकी दिखाई. इससे दर्शक भी प्रभावित हुए. इंटरव्यू लेने वाला भी वर्चुल बातचीत की जीवंत गुणवत्ता से हैरान रह गए. इसने मेटावर्स पर लोगों की रुचि को पुनर्जीवित किया.[40] इस इंटरव्यू का मक़सद अगली पीढ़ी के डिजिटल सामाजिक संपर्कों की झलक पेश करना था, जहां वर्चुअल स्पेस में सार्थक, अंतरंग और गंभीर बहस हो सकगी. इस इंटरव्यू में ज़ुकरबर्ग ने कहा कि बुनियादी AI मॉडल वर्चुअल रियलिटी तकनीकी के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे. पिछले साल लोगों को झुकाव एआई की तरफ रहा, इसमें मेटा को बाज़ार में अपनी नीति में बदलाव करने का मौका दिया. पिछले साल की तुलना में कंपनी के शेयर भी 250 प्रतिशत बढ़ चुके हैं.[41] 25 अक्टूबर को ख़त्म हुई तीसरी तिमाही में मेटा का राजस्व 34 बिलियन डॉलर से अधिक था जो पिछले साल से 23 प्रतिशत ज़्यादा था. अब तक जिस तरह मेटावर्स को मज़ाक बनाया जा रहा था, उसमें भी कमी आई क्योंकि बाज़ार में जेनरेटिव AI का तूफान आ गया. ज़ुकरबर्ग ने भी एक 'आतंरिक क्रांति' की शुरूआत की और कंपनी में एआई के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया. फरवरी 2023 में मेटा ने ओपन सोर्स Llama 2 LLM बनाया.[42] सितंबर 2023 तक ज़ुकरबर्ग ने एआई और वीआर संबंधी उत्पादों की एक श्रृंखला पेश की. जैसे कि रेबैन के साथ सहयोग कर स्मार्ट चश्मे बनाए. मेटोवर्स को लेकर व्यर्थ की बयानबाजी की जगह ठोस उत्पादों में निवेश बढ़ाया गया. मेटा कंपनी के ऐप्स (इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और फेसबुक) की एआई क्षमताओं का विस्तार किया है.[43] हालांकि ज़ुकरबर्ग द्वारा प्रदर्शित फेशियल ट्रैकिंग तकनीकी को अभी अपनाना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए फेस स्कैन और फोटोरियलिस्टिक बातचीत के लिए लंबे सेटअप की ज़रूरत होती है.[44] लेकिन जिस तरह मेटा के नए उत्पादों पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और एप्पल कंपनी भी विज़न प्रो हेडसेट के साथ वीआर और एआर तकनीकी के क्षेत्र में उतर गई है, उससे यही लगता है कि इस तकनीकी का भविष्य व्यावहारिक है. चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ वीआर और एआई तकनीकी के विकास ने उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं को भी हैरान किया है. ऐसे में इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म्स की गूंज दुनियाभर में सुनाई दे रही है. उदाहरण के लिए चीन की सरकार ने 2021 में अपने इलेक्ट्रॉनिक सूचना उद्योग को विकसित करने के लिए मेटावर्स को चौदहवें पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है.[45] इतना ही नहीं सितंबर 2023 में चीन के उद्योग और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने 2023 तक तीन से पांच मेटावर्स से संबंधित कंपनियों को विकसित करने के लिए तीन साल के निवेश और विकास योजना की घोषणा की है. इसके साथ ही 2025 तक तीन से पांच उद्योग क्लस्टर ज़िले भी बनाए जाएंगे.[46]
अक्टूबर 2023 में एक पॉडकास्ट 'मेटावर्स पर पहले इंटरव्यू' में ज़ुकरबर्ग ने मेटा की फेशियल ट्रैकिंग तकनीकी दिखाई. इससे दर्शक भी प्रभावित हुए. इंटरव्यू लेने वाला भी वर्चुल बातचीत की जीवंत गुणवत्ता से हैरान रह गए. इसने मेटावर्स पर लोगों की रुचि को पुनर्जीवित किया.
वीआर, एआर और AI का भविष्य का आकार कैसे होगा, इस पर अभी बहस जारी है. लेकिन उनके विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर इसके असर में विज्ञान कथाओं के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है. पहली पनडुब्बी, सब-ऑर्बिटल रॉकेट और मेटावर्स की अवधारणा जैसे ऐतिहासिक अविष्कारों में विज्ञान कथाओं का भी हाथ है. ये इंजीनियरों को भविष्यवाणी करने की बज़ाए कल्पनाओं को आकार देने का रास्ता बताती हैं. इस विधा की असली ताकत उभरती तकनीकों के संभावित इस्तेमाल में शामिल है.
फीडबैक लूप्स, साइंस फिक्शन प्रोटो-टाइपिंग और नीति
पिछले अंश में विज्ञान कथा और तकनीकी विकास के बीच फीडबैक लूप के जो उदाहरण बताए वो दो सामान्य श्रेणियों में आते हैं. पहला लूप, जो नए तकनीकी प्लेटफॉर्म्स के विकास की तरफ ले जाते हैं. दूसरा लूप, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी से अलग होते हैं. वर्ने और वेल्स की लिखी विज्ञान कथाओं से प्रभावित होकर पनडुब्बी और रॉकेट के निर्माण से पानी के नीचे सफर और अंतिरक्ष में खोज के नई वैश्विक उद्योग खड़े हुए. दूसरी तरफ स्टार ट्रैक कम्युनिकेटर, वीआर प्रोग्रामिंग की भाषाएं और मेटावर्स जैसी विज्ञान कथा अवधारणाओं को एक तरह से दोहराव भी कह सकते हैं क्योंकि ये दूरसंचार, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसी मौजूदा तकनीकों का विस्तार है. दूसरी वाली स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों फीडबैक लूप में ये अधिक सामान्य है.
2000 के दशक के उत्तरार्ध से विज्ञान कथा और तकनीकी के बीच दोहराव को लेकर एक नए तरह का शोध विकसित हो रहा है. इस संबंध का विष्लेषण करने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी शोधकर्ता ब्रायन डी जॉनसन ने “साइंस फिक्शन प्रोटोटाइपिंग” की अवधारणा विकसित की है.[47] इस अवधारणा का उद्देश्य एक ऐसा तरीका विकसित करना था, जिससे फैक्ट और फिक्शन को मिलाकर भविष्य में होने वाले तकनीकी अविष्कारों और भावी टेक्नोलॉजी इंटरफेस का पूर्वानुमान लगाया जा सके.[48] साइंस फिक्शन प्रोटोटाइपिंग के उदाहरण पिछले लेख के पहले के हिस्से में देखे जा सकते हैं. जब स्टार ट्रैक की ओरिजिनल सीरीज़ प्रसारित (1966-1969) हुई थी, तब दूरसंचार अस्तित्व में था. फ्लिप टॉप कम्युनिकेटर को कई तरह की चीजों में काम आ सकने वाली तकनीकी के रूप में प्रस्तुक करके इस सीरीज़ ने मोटोरोला के प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स को एक कामयाब उत्पाद के निर्माण में सक्षम बनाया. इसी तरह स्नो क्रैश ने मेटावर्स नाम का एक वीआर स्पेस प्रस्तुत किया, जिससे वैश्विक स्तर पर कई व्यापारिक लेनदेन और गतिविधियां घटित हुईं. स्टार ट्रैक की तरह स्नो क्रैश में मेटावर्स एक आदर्श तकनीकी मंच था और जो सब जगह उपलब्ध था. कहानी में दिखाया गया है कि वर्चुअल रियलिटी का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. फिर चाहे वो मनोरंजन की गतिविधियां हों, सामाजिक समारोह हों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर आपस में संवाद आदि करना हो. ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मेटावर्स के लिए ज़ुकरबर्ग का जो दृष्टिकोण है, वो स्टीफेंसन से प्रभावित है और ये साइंस फिक्शन प्रोटोटाइपिंग का अच्छा उदाहरण है.
अगर आसान शब्दों में समझें तो साइंस फिक्शन प्रोटो-टाइपिंग का अर्थ “नियंत्रित कल्पना” और “मौके को पहचानने की प्रक्रिया” से हैं, जो बेचने लायक उत्पाद बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं.[49] विज्ञान और टेक्नोलॉजी विचारक क्रिस्टोफ अर्न्स्ट ने “उत्पाद विकास का दर्पण उल्टा पूरक” कहा है.[50] इसी तरह फिल्म निर्माता और विज्ञान सलाहकार भी काल्पनिक तकनीकों का साहित्यिक और सिनेमाई प्रतिनिधित्व बनाते हैं. ऐसा करने का उनका मक़सद दर्शकों के बीच ऐसी तकनीकी को बढ़ावा देना और ऐसे टेक्नोलॉजी उत्पादों के शोध और विकास के लिए पैसे जुटाना होता है.[51] इस प्रक्रिया के दौरान काल्पनिक तकनीकों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य इनके अज्ञात इस्तेमाल के मामलों और “भविष्य के बाज़ारों” का पता लगाना होता है.[52] विज्ञान और तकनीकी अध्ययन के विशेषज्ञ डेविड एक किर्बी के मुताबिक विज्ञान कथाओं में काल्पनिक तकनीकों का चित्रण तीन चीजों के हेरफेर पर आधारित है. ये तीन चीज़ें हैं आवश्यकता, नुकसान रहित और व्यावहारिकता.[53] विज्ञान कथाओं में कुछ काल्पनिक तकनीकों की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसे समाज के लिए आवश्यक बनाकर पेश किया जाता है. ये बताया जाता है कि इतनी आबादी में कुछ खास लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी ज़रूरी है.[54] उदाहरण के लिए स्टार ट्रैक के कम्युनिकेटर सामरिक और रणनीतिक योजना बनाने के लिए अनिवार्य है. न्यूरोमैंसर में एआई और साइबर स्पेस को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया है. मेटावर्स को सामाजिक और व्यापारिक संवाद की प्राथमिक जगह बताया गया है.
साइंस फिक्शन प्रोटोटाइपिंग और नीति
विज्ञान कथा प्रोटोटाइपिंग की एक अहम विशेषता ये होती है कि इससे शोधकर्ताओं और इंजीनियरों को नियंत्रित कल्पना की प्रक्रिया के ज़रिये इनकी आवश्यकता, हानिरहित और व्यावहारिकता का पता चल जाता है. उदाहरण के लिए 2023 में किए गए एक एथोनॉग्राफिक अध्ययन में एआई के 20 शोधकर्ताओं से ये सवाल पूछा कि उनके काम पर विज्ञान कथाओं का कितना प्रभाव पड़ा. स्टडी पेपर के हिसाब से उनके जवाब को तीन श्रेणियों में बांटा गया. नैतिक सोच, शिक्षण शास्त्र और पूर्वानुमानित मॉडलिंग. विज्ञान कथाओं में काल्पनिक तकनीकों की ज़रूरत और व्यावहारिकता तकनीकी का विकास करने वाले डेवलपर्स को ये जानने का मौका देता है कि जो काम वो कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो सकता है और क्या हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था ऐसी है, जो इसका सामना करने में सक्षम है.
विज्ञान कथाओं में कुछ काल्पनिक तकनीकों की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसे समाज के लिए आवश्यक बनाकर पेश किया जाता है. ये बताया जाता है कि इतनी आबादी में कुछ खास लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी ज़रूरी है. उदाहरण के लिए स्टार ट्रैक के कम्युनिकेटर सामरिक और रणनीतिक योजना बनाने के लिए अनिवार्य है.
साक्षात्कार में शामिल शोधकर्ताओं ने माना कि विज्ञान कथाएं उन्हें अलग-अलग मुद्दों पर सोचने को मज़बूर करती हैं. जैसे कि फेशियल रेकॉगनिशन तकनीकी और फिज़ियोलॉजी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को लेकर वो AI से जुड़े सुरक्षा और ज़ोखिमों के बारे में सोचते हैं.[55] विज्ञान कथा प्रोटोटाइपिंग साहित्यिक और वैज्ञानिक विद्वानों को शैक्षणिक मॉडल और शिक्षा से जुड़ी रूपरेखा बनाने की अनुमति देते हैं. इससे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में नैतिक दृष्टिकोण विकसित होता है.[56] अपनी इन विशेषताओं के आधार पर विज्ञान कथाएं पूर्वानुमानित मॉडलिंग के लिए ज़रूरी उपकरण प्रदान करती हैं. इससे पाठकों को संभावित सामाजिक-आर्थिक भविष्य की जांच करने का मौका मिल जाता है. चीन के विज्ञान कथा लेखक और अर्थशास्त्री हाओ जिनफैंग के लघु उपन्यास 'फोल्डिंग बीज़िंग' को ही ले लीजिए. इस कहानी में बीज़िंग को बहुत ज़्यादा भविष्यवादी शहर के रूप में दिखाया गया है. शहर की आबादी को इस आधार पर तीन हिस्सों में बांटा गया है कि उन्हें सतह में कितना वक्त बिताने की मंजूरी है. उम्मीद के मुताबिक आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हिस्सा गरीबों का है, जिन्हें थर्ड स्पेस कहा गया है. इसमें सफाई कर्मचारी, छोटे दुकानदार और मज़दूर शामिल हैं. इन्हें सतह पर सबसे कम समय बिताने की अनुमति है. थर्ड स्पेस में शामिल लोगों द्वारा जो काम किए जाते हैं वो स्वचालित यानी ऑटोमेटेड नहीं हैं क्योंकि इन्हें रोज़गार मुहैया कराया जाना है. वैज्ञानिक और निवेशक काऊ फू ली ने हाओ की इस कहानी का ज़िक्र करते हुए स्वाचालन यानी ऑटोमेशन के संभावित ख़तरों को लेकर चेतावनी दी. इससे कई लोगों का काम छिन सकता है, खासकर जो श्रम प्रधान समाज है.[57] 2019 में काऊ फू ली ने चेतावनी दी थी कि जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स आर्थिक विस्थापन का रास्ता बना रहे हैं.
हाल के वर्षों में ऐसी कई नीतिगत पहल हुईं हैं, जिनका इरादा विज्ञान कथाओं के इस्तेमाल के ज़रिये ये बताना था कि उभरती हुई तकनीकों को कैसे परिभाषित, विनियमन और मूल्यांकन किया जाए. अमेरिका स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड इमेजिनेशन ने स्टीफेंसन जैसे लेखकों के साथ मिलकर शैक्षणिक और शोध के क्षेत्र में नई पहल की है. इसका उद्देश्य सांस्कृतिक लक्ष्यों और उम्मीदों के साथ फीडबैक लूप्स के बारे में बताना है. इसके साथ ही वैज्ञानिक अविष्कारों और विज्ञान कथाओं के संबंध को रेखांकित करना भी है.[58] कई विद्वानों और शिक्षकों ने विज्ञान कथाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की परियोजनाएं शुरू की हैं. शोधकर्ता इसाबेल ओलिवेरा मॉरिस, राफाएला मेगालाहेस आयर्स और आंद्रिया कार्ला डी सूज़ा गोएस ने इस बात को नोट किया कि 2017-2019 के बीच जब 14 से 16 साल के बच्चों के लिए अलग-अलग विषयों में उपदेशात्मक कार्यक्रम लागू कर जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 को पढ़ना अनिवार्य किया गया तो बायोलॉजी, आर्ट और फिलोसॉफी के छात्रों में इस विषय को लेकर जुड़ाव भी बढ़ा और उन्हें प्रेरणा भी मिली.[59] अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षक जियुन बैंग ने अपनी कक्षा में 'द एक्सपेंस' विज्ञान कथा सीरीज़ पर चर्चा की. इस सीरीज़ में अंतरग्रहीय मानव समाज में बदले राजनीतिक गुटों और गठबंधनों पर बात की गई है. जियुन बैंग के मुताबिक इस विज्ञान कथा पर चर्चा के बाद उनके छात्रों की तार्किक क्षमता और जागरूकता में वृद्धि हुई. 2017 में कानूनी विद्वान एडम जार्डिन ने गैर मानवीय व्यक्तित्व अधिकार के दो मामलों को पढ़ाने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्लेनेट ऑफ एप्स (1968) फिल्म का इस्तेमाल किया.[60] उनके मुताबिक ऐसा करने से छात्रों को कानूनी सिद्धांत आसानी से समझ आ गए, साथ ही इसने ये भी दिखाया कि अगर कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो कानून इस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकता है और कैसे बातचीत कर सकता है. इसी तरह साहित्यिक विचार अनास्तसिया पीज़ ने कहा कि पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में उनकी नैतिकता पर क्लास के दौरान वो विज्ञान कथा लेखकों उर्सला के ली गुईन, स्टैनिस्लाव लेम, टेड चियांग और स्ट्रार ट्रैक सीरीज़ में शामिल नैतिकता के मामलों का अध्ययन कराती हैं.[61] इतना ही नहीं 2012 से 2014 के बीच यूरोपीयन यूनियन की 'शिक्षा में विज्ञान कथाएं' परियोजना ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि विज्ञान की पढ़ाई में विज्ञान कथाओं को शामिल करने से फायदा मिलता है. चारलम्बोस व्रसीदास, लूसी अवरामिडो, कैटरीना थ्योडोरिडो, सोतिरिस थेमिस्टोक्लेवियॉस और पेट्रोल पनाऊ जैसे शोधकर्ताओं का मानना है कि पढ़ाई में विज्ञान कथाओं का इस्तेमाल करने से छात्रों में विज्ञान को लेकर रुचि बढ़ती है, वो खुद को इस विषय में पूरी तरह डुबा देते हैं. काल्पनिक तकनीकी कल्पनाओं ने छात्रों को वैज्ञानिक विकास और मानसिक तौर पर उसके चित्रण करने में मदद की है.[62]
अगर सरकारी नीति के क्षेत्र को लेकर बात करें तो ब्रिटेन का लीवरहल्म सेंटर AI के लिए वैश्विक पहल की वकालत कर रहा है. इसका उद्देश्य ये पहचान करना है कि एआई शासन की नीतियों पर सांस्कृतिक ढांचे, जैसे कि विज्ञान कथा जो सांस्कृतिक धारणाओं को प्रभावित करती है, का क्या असर होता है.[63] उदाहरण के लिए लीवरहल्म सेंटर के शोधकर्ताओं स्टीफन केव और कांता दिहाल ने लोकप्रिय सार्वजनिक सांस्कृतिक चेतना में उन्नत AI और बुद्धिमान मशीन से जुड़ी चार जोड़े आशाओं और डर का अध्ययन किया. ये चार जोड़े हैं: जीवन के विस्तार की संभावना (अमरता) बनाम अपनी पहचान ख़त्म होने का डर (अमानवीयता); काम और रोज़गार की ज़रूरत में कमी की संभावना बनाम अपने बेकार हो जाने का ख़तरा; अपनी इच्छाएं जल्द पूरी होने की संभावना बनाम सभी इंसानों का एक-दूसरे से अलग हो जाने का डर; एआई द्वारा भू-राजनीतिक प्रभुत्व का प्रस्ताव बनाम इसके मानवता के ख़िलाफ हो जाने का डर (विद्रोह).[64] सार्वजनिक चेतना पर विज्ञान कथाओं के सीधे पड़ने वाले असर को देखते हुए फरवरी 2023 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय और रक्षा विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला ने 'स्टोरीज़ फ्रॉम टुमारो : एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज थ्रू यूज़फुल फिक्शन' नाम से एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया.[65] इस दस्तावेज़ में काल्पनिक लेखन को विस्तृत शोध के साथ जोड़ा गया. शोधकर्ताओं के इंटरव्यू लिए गए. जिसमें भविष्य की तकनीकों को लेकर व्यापाक ज्ञान मुहैया कराया गया. इस दस्तावेज़ को रक्षा मंत्रालय की नीतियों और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रणनीतियों के पूरक के रूप में प्रकाशित किया गया.
साइंस फिक्शन प्रोटोटाइप शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को उभरती हुई तकनीकों के परिणामों का अंदाज़ा लगाने का मौका देते हैं. ये नैतिक विचार-विमर्श के लिए कड़ी परीक्षा, नए शैक्षणिक मॉडल्स के लिए उत्प्रेरक और भविष्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का पूर्वानुमान लगाने के उपकरण के तौर पर काम करता है.
तकनीकी अविष्कार और विज्ञान कथाओं के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं, वो सांस्कृतिक लक्ष्यों और शासन को लेकर अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं. साइंस फिक्शन प्रोटोटाइप शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को उभरती हुई तकनीकों के परिणामों का अंदाज़ा लगाने का मौका देते हैं. ये नैतिक विचार-विमर्श के लिए कड़ी परीक्षा, नए शैक्षणिक मॉडल्स के लिए उत्प्रेरक और भविष्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का पूर्वानुमान लगाने के उपकरण के तौर पर काम करता है.
आगे की राह के लिए क्या सिफ़ारिशें?
हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां तकनीकी विकास की गति बहुत तेज़ हो रही है. वर्तमान वास्तविकताओं और विज्ञान कथाओं के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि विज्ञान कथाओं से हमें जो काल्पनिक दूरदर्शिता मिलती है, उसी हिसाब से हम अपनी दूरगामी नीतियां बनाएं. इस विधा में अविष्कार और टेक्नोलॉजी विकास को आकार देने वाली इतनी संभावनाएं हैं, जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है. अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए साइंस फिक्शन प्रोटोटाइपिंग एक प्रभावशाली उपकरण है क्योंकि इसकी मदद से हम भविष्य की अपेक्षित तकनीकी और उससे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं. नीचे लिखी गईं सिफारिशें साइंस फिक्शन और वास्तविक दुनिया की रणनीतियों को एकीकृत कर उभरती हुई तकनीकों से पेश आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं.
शोध और विकास के काम में साइंस फिक्शन प्रोटोटाइपिंग को बढ़ावा देना
शोध संस्थाओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों, खासकर स्टार्टअप्स (क्योंकि बड़ी और पुरानी कंपनियों की तुलना में स्टार्टअप्स का काम करने का तरीका ज़्यादा लचीला होता है) को विज्ञान कथाओं के प्रोटोटाइप को अपने अनुसंधान में शामिल करने के लिए अनुदान और दूसरे तरह के प्रोत्साहन देने चाहिए. स्टार्टअप्स नई तकनीकी का पता लगाने, भविष्य में होने वाले अविष्कारों के परिणामों का अंदाज़ा लगाने में विज्ञान कथाओं में रचनात्मक स्वतंत्रता का फायदा उठा सकते हैं. इससे ऐसे उत्पादों और समाधानों का विकास हो सकता है, जो शायद अनुसंधान और विकास के पारंपरिक नज़रिये का पालन करने से नहीं उभर सकते. इससे स्टार्टअप कंपनियां बाज़ार में भूचाल पैदा कर तकनीकी उन्नति से आर्थिक लाभ भी कमा सकती हैं.
उभरती तकनीकों के लिए नैतिक दिशानिर्देश तय करना
किर्बी ने साइंस फिक्शन प्रोटोटाइपिंग को प्रभावित करने वाली जो चार वजहें बताई थीं, उसके आधार पर उभरती तकनीकों के लिए एक व्यापाक नैतिक दिशानिर्देश बनाए जाने की ज़रूरत है. विज्ञान कथाओं से प्रभावित होकर काम करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. चूंकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) विज्ञान और संस्कृति पर ध्यान देता है तो उभरती तकनीकों और साइंस फिक्शन पर आधारित प्रोटोटाइप के लिए नैतिक दिशानिर्देश बनाने के काम का नेतृत्व यूनेस्को को करना चाहिए. विश्व आर्थिक मंच भी अपने अलग-अलग कामों के लिए जाना जाता है. इसलिए इस मंच को भी अपनी सालाना बैठक में दिग्गज कारोबारियों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के अपने नेटवर्क को इस बात के लिए मनाना चाहिए वो अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन नैतिक दिशानिर्देशों को लागू करें.
शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विज्ञान कथाओं को शामिल करना
सरकारों को चाहिए कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स (STEM) की शिक्षा में विज्ञान कथाओं को पूरक पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल करें. इससे छात्रों में नैतिक बहस और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा. इस लेख में पहले बताई गई केस स्टडीज़ को उपदेशात्मक कार्यक्रमों में लागू किया जा सकता है. हालांकि, ऐसी शैक्षणिक सामग्री और कहानियों के साथ जो संदर्भ दिए जाते हैं, वो उस हिसाब से हों, जिन देशों में ये कार्यक्रम लागू किया जाना है. ऐसी सामग्री के चयन के लिए शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच सहयोग हो सकता है, जिसका उद्देश्य सीखने और नई खोज को बढ़ावा देना होना चाहिए. यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विज्ञान कथाओं और काल्पनिक नैरेटिव को बढ़ावा देकर टेक्नोलॉजी अवधारणा और वैज्ञानिक जटिलताओं को प्रदर्शित किया जा सकता है. STEM शिक्षा के संदर्भ में विज्ञान कथाओं को पढ़ाने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन कर सकते हैं. इसका उद्देश्य तकनीकीविदों और नीति निर्माताओं की एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ावा देना होना चाहिए, जिन्हें ना सिर्फ अपने विषय की जानकारी हो बल्कि वो उभरती तकनीकों और समाज पर उसके व्यापक प्रभाव को लेकर दार्शनिक और नैतिक तौर पर भी जानकारी रखते हों.
नीति निर्माताओं और रचनात्मक उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाना
भारत में जो विज्ञान कथाएं लिखी गईं, उसमें एक तनाव ये दिखा कि भारत को औद्योगिक और तकनीकी रूप से विकसित तो देखना चाहते हैं लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि भविष्य को लेकर पश्चिमी देशों का जो नज़रिया है, उसके विकृत रूप की छाया भारत पर ना पड़े. इन चिंताओं को दूर करने के लिए स्टार्टअप्स पर केंद्रित संस्थाएं जैसे कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन को रचनात्मक उद्योग, जिसमें लेखक, फिल्मकार और लेखक शामिल हैं, के साथ साझेदारी स्थापित करनी चाहिए. सरकारी एजेंसी और फिल्मकारों के बीच इस सहयोग से ऐसी सामग्री तैयार की जा सकेगी, जिससे जनता के बीच तकनीकी विमर्श बढ़े लेकिन अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखा जाए. इन कोशिशों को अमेरिका और ब्रिटेन के सेंटर फॉर साइंस एंड द इमेजिनेशन की तरफ से की जा रही पहल की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है. थिंक टैंक या फिर संयुक्त परियोजनाएं शुरू की जा सकती है, जो इस काम के लिए संग्रह, फिल्में और शैक्षणिक श्रृंखलाओं का निर्माण करेंगे. इनका इस्तेमाल नीतियों को बनाने और जनता से जुड़ने के लिए किया जा सकता है.
विज्ञान कथाओं को सम्मलित कर सबूतों पर आधारित नीति बनाना
सरकारें अपने नीति अनुसंधान के एजेंडे को काल्पनिक कथाओं के साथ एकीकृत कर सकती हैं. विज्ञान कथा लेखकों और नीति निर्माता विशेषज्ञों को शामिल कर टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है, जो नीतिगत फैसलों का प्रभाव का अनुमान लगा सकें. संयुक्त राष्ट्र और जी-20 जैसे संगठन भी इस दृष्टिकोण को अपनाकर अपने नीति मसौदे और विचारों का परीक्षण कर सकते हैं. ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के 'स्टोरीज फ्रॉम टुमारो' दस्तावेज़ जैसी नीतिगत पहल इस मामले में फैसला करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती है. इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि नियम और रणनीतियां उभरती तकनीकों के हिसाब से हो, साथ ही वो सामाजिक मूल्यों को भी दर्शाएं.
उभरती टेक्नोलॉजी के नैतिक नियमन के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना
उभरती हुई तकनीकों के लिए नियम बनाने और उन्हें लागू के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए. उदाहरण के लिए अक्टूबर 2023 में ब्रिटेन में AI सुरक्षा पर जो सम्मेलन हुआ, उसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोपीयन यूनियन और चीन के अधिकारी भी शामिल हुए. इस तरह के सम्मेलनों में सहयोगी और विरोधी दोनों तरह के देशों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव देश की सीमाओं से परे होता है. इसे रोकने के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों और तकनीकी की ज़रूरत होती है.
निष्कर्ष
तकनीकी में तेज़ी से बदलाव के इस युग में नीति निर्माण, शोध और शिक्षा में विज्ञान कथाओं को रणनीतिक रूप से शामिल करना आज के वक्त की ज़रूरत है. इस लेख में प्रस्तुत की गई सिफ़ारिशें विज्ञान कथा प्रोटोटाइपिंग की समग्र एकीकरण की वकालत करती हैं. ये सिफ़ारिशें इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि ये तकनीकी अविष्कार ना सिर्फ प्रेरक हों बल्कि नैतिक रूप से सही और शैक्षिक रूप से भी समर्थित हों. नीति निर्माताओं, रचनात्मक उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है जहां टेक्नोलॉजी विकास और सामाजिक मूल्यों के बीच संतुलन हो. ये उपाय उभरती तकनीकों से पैदा होने वाली जटिल चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे. इनसे सामाजिक-आर्थिक समझदारी और मानवीय मूल्यों एवं टेक्नोलॉजी अविष्कारों के बीच एक संतुलन पैदा होगा.
Endnotes
[a] ट्यूरिंग पुरस्कार को अक्सर 'कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज़' भी कहा जाता है. एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा ये अवॉर्ड हर साल उस शख्सियत को दिया जाता है, जिसने कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो. इस पुरस्कार का नामकरण ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग के नाम पर किया गया है. उन्हें कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी माना जाता है.
[b] इसके कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं; विलियम गिब्सन की न्यूरोमैंसर (1984). फिलिप के डिक की डू एन्ड्रॉयड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शिप? (1968). ममोरू ओशी की घोस्ट इन द शेल (1995) और द मैट्रिक्स(1999).
[1] Inga Ulnicane, “Artificial Intelligence in the European Union: Policy, Ethics and Regulations,” in The Routledge Handbook of European Integrations, ed. Gabriel Weber, Ignazio Cabras, and Thomas Hoerber (New York, NY: Routledge, 2022), 254–69.
[2] European Parliament, European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, February 16, 2017, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html#title1.
[3] European Parliament, Follow up to the European Parliament resolution of 16 February 2017 on civil law rules on robotics, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2017/11-20/A8-0005-2017_EN.pdf.
[4] Ragnar Fjelland, “Why General Artificial Intelligence Will Not Be Realized,” Humanities and Social Sciences Communications 7, no. 1 (2020), https://doi.org/10.1057/s41599-020-0494-4.
[5] Zoe Kleinman & Chris Vallance, “Ai ‘godfather’ Geoffrey Hinton Warns of Dangers as He Quits Google,” BBC, May 2, 2023, https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-65452940.
[6] Kate Devlin, “Extinction Risk from AI on Same Scale as Nuclear War, Sunak Warns,” The Independent, October 26, 2023, https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ai-sunak-weapon-war-uk-b2436000.html.
[7] “Mark Zuckerberg: First Interview in the Metaverse | Lex Fridman Podcast #398,” YouTube, September 28, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=MVYrJJNdrEg.
[8] “Yuval Noah Harari and Mustafa Suleyman on the Future of Ai,” The Economist, September 14, 2023, https://www.economist.com/films/2023/09/14/yuval-noah-harari-and-mustafa-suleyman-on-the-future-of-ai.
[9] Lindy Orthia, “Science Fiction as a Potent Policy Tool,” Policy Forum, August 14, 2019, https://www.policyforum.net/science-fiction-as-a-potent-policy-tool/.
[10] Tate Ryan-Mosley, “An inside Look at Congress’s First AI Regulation Forum,” MIT Technology Review, September 25, 2023, https://www.technologyreview.com/2023/09/25/1080104/inside-congresss-first-ai-insight-forum/.
[11] The White House, Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, October 30, 2023, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/.
[12] Matt Sheehan, “China’s AI Regulations and How They Get Made,” Carnegie Endowment for International Peace, July 10, 2023, https://carnegieendowment.org/2023/07/10/china-s-ai-regulations-and-how-they-get-made-pub-90117.
[13] Jaron Lanier, Who Owns the Future? (New York: Simon & Schuster, 2014), 191.
[14] “Drone Wars and ‘Killer Robots,’” Drone Wars UK, November 2, 2023, https://dronewars.net/drone-wars-and-killer-robots/.
[15] Jutta Weber, “Artificial Intelligence and the Socio-Technical Imaginary: On Skynet, Self-Healing Swarms and Slaughterbots,” in Drone Imaginaries: The Power of Remote Vision, ed. Andreas Immanuel Graae and Kathrin Maurer (Manchester: Manchester University Press, 2021), 167–79.
[16] Oihab Allal-Chérif, “‘Black Mirror’: The Dark Side of Technology,” The Conversation, June 4, 2019, https://theconversation.com/black-mirror-the-dark-side-of-technology-118298.
[17] Moe Long, “Real World Tech: How Science Fiction Technology Influences Innovation,” Electropages, January 22, 2020, https://www.electropages.com/blog/2020/01/how-sci-fi-influences-real-world-tech-and-innovation.
[18] Mark Strauss, “Ten Inventions Inspired by Science Fiction,” Smithsonian Magazine, March 15, 2012, https://www.smithsonianmag.com/science-nature/ten-inventions-inspired-by-science-fiction-128080674/.
[19] Michael Benson, “Science Fiction Sent Man to the Moon,” The New York Times, July 20, 2019, https://www.nytimes.com/2019/07/20/opinion/sunday/moon-rockets-space-fiction.html.
[20] Benson, “Science Fiction Sent Man to the Moon”
[21] Sukarno Banerjee, “India,” in The Routledge Companion to Cyberpunk Culture, ed. Anna McFarlane, Lars Schmeink and Graham J. Murphy (New York: Routledge, 2020), 408-414.
[22] Banerjee, “India,” 408-9.
[23] European Commission, Artificial intelligence for Europe, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237.
[24] Mike Featherstone and Roger Burrows, Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment, ed. Mike Featherstone and Roger Burrows (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1996).
[25] Lanier, Who Owns the Future?, 291.
[26] Erik Davis, Techgnosis: Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information (New York, NY: Harmony Books, 1998), 229.
[27] Sam Davies, “The Matrix and the Sci-Fi Stories That Predicted Life in 2021,” BBC, December 8, 2021, https://www.bbc.com/culture/article/20211207-the-matrix-and-the-sci-fi-stories-that-became-a-reality.
[28] Nicholas M. Kelly, “‘Works like Magic’: Metaphor, Meaning, and the GUI in Snow Crash,” Science Fiction Studies 45, no. 3 (November 2018): 69, https://doi.org/10.5621/sciefictstud.45.1.0069
[29] Mark Pesce, Magic mirror: The novel as a software development platform, MIT, 1999, https://web.mit.edu/comm-forum/legacy/papers/pesce.html.
[30] “‘Snow Crash’ is a Cyberpunk Classic,” Wired, July 14, 2023, https://www.wired.com/2023/07/geeks-guide-silo-adaptation/.
[31] “Sergey Brin Biography,” Academy of Achievement, 2000, https://achievement.org/achiever/sergey-brin/.
[32] “Meta,” Meta.com, https://about.meta.com/meta/%C2%A0.
[33] Davies, “The Matrix and the Sci-Fi Stories That Predicted Life in 2021”
[34] Alex Hern, “As Mark Zuckerberg celebrates his 30th birthday, is Facebook maturing too?” The Guardian, May 13, 2014, https://www.theguardian.com/technology/2014/may/13/mark-zuckerberg-30-birthday-facebook-maturing-purchase-whatsapp-oculus.
[35] Kabir Singh Bhandari, "Metaverse Fashion Week: The Future of Fashion Shows,” Entrepreneur, https://www.entrepreneur.com/article/423234
[36] “What is the metaverse?” McKinsey & Company, July 15, 2022, https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-the-metaverse.
[37] Matt Oliver and Gareth Corfield, “Why Mark Zuckerberg’s Metaverse vanity project threatens to destroy Facebook,” Sunday Telegraph, October 27, 2022, https://www.telegraph.co.uk/business/2022/10/27/inside-metaverse-what-exactly-going-zuckerberg/.
[38] Ryan Mac, Sheera Frenkel & Kevin Roose, “Skepticism, confusion, frustration: Inside Mark Zuckerberg’s metaverse struggles,” The New York Times, October 10, 2022, https://www.nytimes.com/2022/10/09/technology/meta-zuckerberg-metaverse.html.
[39] Kelly, ““works like magic”: Metaphor, meaning, and the GUI in Snow Crash,” 69.
[40] Fridman, “Mark Zuckerberg: First Interview in the Metaverse | Lex Fridman Podcast #398”
[41] “AI has rescued Mark Zuckerberg from a metaverse-size hole,” The Economist, October 26, 2023, https://www.economist.com/business/2023/10/26/ai-has-rescued-mark-zuckerberg-from-a-metaverse-size-hole.
[42] “AI has rescued Mark Zuckerberg from a metaverse-size hole”
[43] “AI has rescued Mark Zuckerberg from a metaverse-size hole”
[44] GlobalData Thematic Intelligence, “Will Zuckerberg’s Metaverse Become Our Reality?” Verdict, October 19, 2023, https://www.verdict.co.uk/will-zuckerberg-metaverse-become-our-reality/.
[45] Yi Jing Fly and Laura Grünberg, “What will China’s metaverse look like?” The Diplomat, March 30, 2022, https://thediplomat.com/2022/03/what-will-chinas-metaverse-look-like/.
[46] Giulia Interesse, “China metaverse action plan: Three-year national development strategy," China Briefing News, September 25, 2023, https://www.china-briefing.com/news/china-releases-three-year-action-plan-for-metaverse-industry-development/.
[47] Brian D. Johnson, “Science Fiction Prototyping: Designing the Future with Science Fiction,” Synthesis Lectures on Computer Science 3, no. 1 (2011): 1–190, https://doi.org/10.2200/s00336ed1v01y201102csl003
[48] David A. Kirby, Lab Coats in Hollywood: Science, Scientists, and Cinema (Cambridge, MA: MIT Press, 2011), 175.
[49] Christopher Ernst, “DECONTEXTUALISING ‘SCIENCE FICTION PROTOTYPING,” Interface Critique, 4 (2023): 139.
[50] Ernst, “DECONTEXTUALISING ‘SCIENCE FICTION PROTOTYPING”
[51] Jan Oliver Schwarz and Franz Liebl, “Cultural Products and Their Implications for Business Models: Why Science Fiction Needs Socio-Cultural Fiction,” Futures 50 (2013): 66–73, https://doi.org/10.1016/j.futures.2013.03.006.
[52] Ernst, “DECONTEXTUALISING ‘SCIENCE FICTION PROTOTYPING,” 140.
[53] Kirby, Lab Coats in Hollywood, 196.
[54] Kirby, Lab Coats in Hollywood, 197.
[55] Sarah Dillon and Jennifer Schaffer-Goddard, “What AI Researchers Read: The Role of Literature in Artificial Intelligence Research,” Interdisciplinary Science Reviews 48, no. 1 (2022): 15–42, https://doi.org/10.1080/03080188.2022.2079214.
[56] Dillon and Schaffer-Goddard, “What AI Researchers Read: The Role of Literature in Artificial Intelligence Research,” 34.
[57] Kai-Fu Lee, AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order (Boston, MA: Mariner Books, 2021), 131.
[58] Andrew Dana Hudson, Ed Finn, and Ruth Wylie, “What Can Science Fiction Tell Us about the Future of Artificial Intelligence Policy?” AI & Society 38, no. 1 (2023): 197–211.
[59] Isabella de Oliveira Moraes, Rafaela Magalhães Aires, and Andréa Carla de Souza Góes, “Science Fiction and Science Education: 1984 in Classroom,” International Journal of Science Education 43, no. 15 (2021): 2501–15.
[60] Adam Jardine, “The Pedagogic Value of Science Fiction: Teaching about Personhood and Nonhuman Rights with Planet of the Apes," The University of Notre Dame Australia Law Review 20, no. 6 (2018): 1-41.
[61] Anastasia Pease and Society for Ethics Across the Curriculum, “Teaching Ethics with Science Fiction: A Case Study Syllabus,” Teaching Ethics 9, no. 2 (2009): 75–81.
[62] Charalambos Vrasidas et al., “Science Fiction in Education: Case Studies from Classroom Implementations,” Educational Media International 52, no. 3 (2015): 201–15.
[63] Hudson et al., “What Can Science Fiction Tell Us about the Future of Artificial Intelligence Policy?”
[64] Stephen Cave and Kanta Dihal, “Hopes and Fears for Intelligent Machines in Fiction and Reality,” Nature Machine Intelligence 1, no. 2 (2019): 74–78.
[65] “Stories from the Future: exploring new technology through useful fiction,” Gov.uk, February 28, 2023, https://www.gov.uk/government/publications/stories-from-the-future-exploring-new-technology-through-useful-fiction.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.





 PREV
PREV