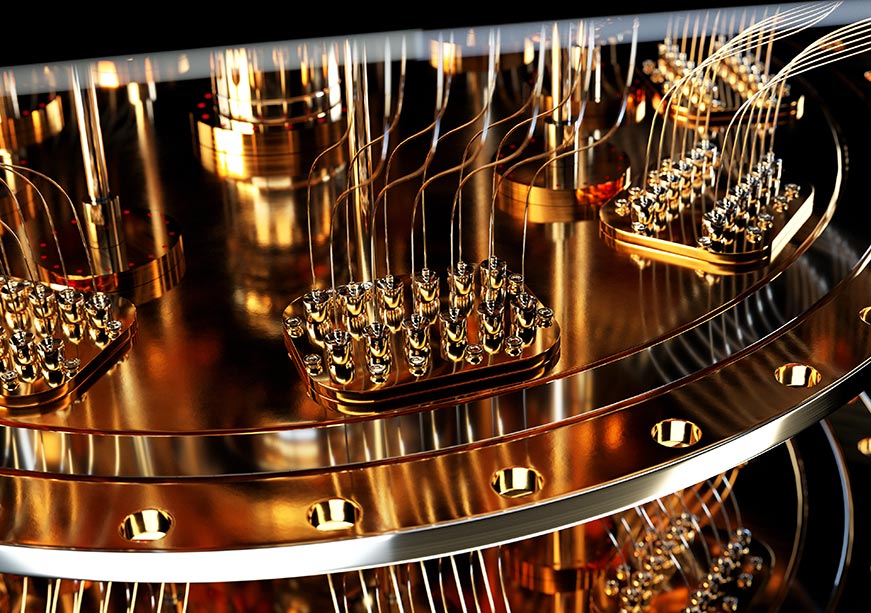इस साल की शुरुआत उन भयानक तस्वीरों के साथ हुई, जब कट्टर दक्षिणपंथियों की एक भीड़ ने अमेरिकी लोकतंत्र के मंदिर कैपिटॉल हिल पर हमला कर दिया था. कई घंटों तक इन दंगाइयों का अमेरिकी संसद की इमारत पर क़ब्ज़ा रहा था. इसके चलते, जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर संसद की मुहर लगने में तो देर हुई ही, दुनिया के सबसे पुराने और ताक़तवर लोकतांत्रिक देश वाली अमेरिका की छवि को भी भारी नुक़सान पहुंचा.
ये घटना बहुत से भारतीयों के लिए भी बड़ा झटका थी, क्योंकि बहुत से भारतीय, अमेरिका के लोकतंत्र और उसके मज़बूत लोकतांत्रिक संस्थानों को ललक भरी नज़रों से देखते हैं और अक्सर उससे प्रेरित भी होते हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिकी संसद पर उपद्रवियों के इस हमले को लेकर चिंता जताई. उन्होंने अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना और सत्ता के शांतिपूर्ण तरीक़े से हस्तांतरण की अपील भी की. हालांकि, भारत में बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमेरिका का लोकतंत्र, जो बाइडेन के नेतृत्व में फिर से अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा. लेकिन, भारत के विदेश नीति के गलियारों में लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि, दुनिया की इकलौती सुपर-पावर अमेरिका में अब विश्व की उदारवादी विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करने की क्षमता बची है या नहीं.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिकी संसद पर उपद्रवियों के इस हमले को लेकर चिंता जताई. उन्होंने अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना और सत्ता के शांतिपूर्ण तरीक़े से हस्तांतरण की अपील भी की.
पश्चिमी ताक़तों के बीच और ख़ास तौर से अमेरिका में एक असरदार नेतृत्व के अभाव के चलते, चीन जैसी तानाशाही ताक़तों ने बिना किसी ख़ास विरोध के दुनिया में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है. विशेष रूप से, हॉन्ग कॉन्ग में लोकतंत्र समर्थकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, साउथ चाइना सी में तनाव, भारत के साथ सीमा पर संघर्ष, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़ा आर्थिक टकराव और कोविड-19 को लेकर आक्रामक रवैया अपनाने के कारण आज इस बात को लेकर भारी चिंता है कि, चीन नियम-क़ायदों पर आधारित व्यवस्था का सम्मान करता है, या नहीं.
क्वॉड (QUAD) जैसी सामरिक पहलों के रफ़्तार पकड़ने से, नियम आधारित व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कुछ उम्मीद तो जगी है. चीन से बढ़ते ख़तरे और अमेरिका की ताक़त में कमी आने के कारण आज ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी ताक़तों को क्वॉड में अधिक प्रभावी भूमिका अपनाने को मजबूर होना पड़ा है, जबकि पहले वो इसके लिए अनिच्छुक थे. और हालांकि, 6 जनवरी की घटनाएं एक बड़ी त्रासदी थीं. लेकिन, उनकी वजह से ही, दुनिया में ऐसे कई क्षेत्रीय प्रयास शुरू होने की उम्मीद है, जिनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत किया जा सके और इसमें तानाशाही ताक़तों की दख़लंदाज़ी पर लगाम लगाई जा सके. हिंद प्रशांत क्षेत्र से बाहर, ट्रंप ने अपने शासन काल के चार वर्षों के दौरान, अमेरिका फर्स्ट की नीतियों को तरज़ीह दी. इसने यूरोपीय संघ के जर्मनी और फ्रांस जैसे सदस्यों को प्रेरित किया कि वो अमेरिका का पिछलग्गू बने रहने के बजाय, स्वतंत्र रूप से ऐसी नीतियों की संभावनाएं तलाशें, जो नियम आधारित व्यवस्था को मज़बूत बना सकें.
चीन के मद्देनज़र भारत भी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इंडोनेशिया, जापान और ब्रिटेन जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ सुरक्षा और सामरिक साझेदारियां विकसित करने में लगा है. भारत द्वारा हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल होने की इजाज़त देना, उसकी स्वायत्त नीति का पक्का सबूत है. हालांकि, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए आज भी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना प्रासंगिक बना हुआ है. लेकिन, 6 जनवरी को वॉशिंगटन में हुई घटनाएं और अमेरिका में लंबे समय से घरेलू उठा-पटक व अस्थिरता को देखते हुए दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए और प्रयास करने को बाध्य होंगे.

लोकतंत्र की रक्षा के अभियान में आई नई जान
लेस्ली विंजामुरी
डायरेक्टर, यूएस ऐंड अमेरिकाज़ प्रोग्राम, चैथम हाउस, ब्रिटेन
डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के पिछले चार वर्षों के दौरान ब्रिटेन ने एक अनुशासित सिपाही की भूमिका निभाई है. ब्रिटेन इस दौरान, ट्रंप के तमाम बयानों को सुनते हुए लगातार ये सोचता रहा कि ट्रंप की हरकतों पर वो कैसी प्रतिक्रिया दे. पहले, पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा-मे और फिर मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अपने देश की प्रतिष्ठा को बचाने के साथ-साथ, एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बनाने का संघर्ष करते रहे, जो ऊट-पटांग बातें करते थे और अक्सर दादागीरी करने वाले दोस्त की भूमिका में नज़र आते थे. लेकिन, ब्रेग्ज़िट पर ट्रंप और बोरिस जॉनसन की राय एक थी. इसके अलावा आयरलैंड की सीमा को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता के माहौल और अमेरिका व ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर बोरिस जॉनसन के पूरी ताक़त झोंक देने से लोगों के ज़हन में सवाल उठे कि क्या पूर्व उप-राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ जाएगी.
6 जनवरी को कैपिटॉल हिल पर हमलों ने हर उस उलझन को ख़त्म कर दिया है, जो बाइडेन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद बोरिस जॉनसन सरकार के सामने खड़ी होने वाली थी. इसकी एक वजह तो ये थी कि ब्रिटेन में ये भय व्याप्त हो गया था कि दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक देश और ब्रिटेन का सबसे सच्चा दोस्त अमेरिका कहीं, भयंकर उथल-पुथल भरे हिंसक राजनीतिक दौर का शिकार न हो जाए. और अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में अवसरों का एक पूरा दशक व्यर्थ चले जाने का डर था.
6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए हमले की एक सकारात्मक बात ये है कि एक ही दिन के अंदर, ब्रिटेन ने अमेरिका को लेकर एकजुट और स्पष्ट रुख़ अपना लिया. ब्रिटेन का ये नया नज़रिया आने वाले हफ़्तों और महीनों में बहुत अहम रहने वाला है. बोरिस जॉनसन, शैडो प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर, स्कॉलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टरजियॉन, पूर्व विदेश सचिव जेरेमी हंट और विदेशी व कॉमनवेल्थ मामलों के शैडो मिनिस्टर लिज़ा नैंडी, सबने अमेरिकी कैपिटॉल पर उपद्रवियों के हमले की एक सुर से कड़ी आलोचना की थी और ज़ोर देकर कहा था कि वो अमेरिका में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का समर्थन करते हैं. अब जो बाइडेन, ब्रिटेन में तमाम राजनीतिक पक्षों को विभाजित करने वाले नहीं, बल्कि उन्हें एकजुट करने वाले अमेरिकी नेता बन गए हैं. ये ट्रंप के शासनकाल के चार वर्षों के ठीक उलट है. क्योंकि ट्रंप ने न केवल अमेरिका को विभाजित किया बल्कि, ब्रिटेन में भी दरार डालने का काम किया था.
6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए हमले की एक सकारात्मक बात ये है कि एक ही दिन के अंदर, ब्रिटेन ने अमेरिका को लेकर एकजुट और स्पष्ट रुख़ अपना लिया. ब्रिटेन का ये नया नज़रिया आने वाले हफ़्तों और महीनों में बहुत अहम रहने वाला है.
अमेरिकी संसद और वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इस हमले से ब्रिटेन में भी मूल्यों पर आधारित विदेश नीति की ओर झुकाव की रफ़्तार बढ़ेगी. इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन और उनकी विदेश नीति से जुड़ी टीम के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. बाइडेन की टीम में ऐसे कई सदस्य हैं, जिनका ब्रिटेन की सत्ता के गलियारों में भी काफ़ी सम्मान है.
अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों का शिखर सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव और ब्रिटेन द्वारा दस लोकतांत्रिक देशों (D 10) का समूह गठित करने के प्रस्तावों पर अब और ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. ये प्रस्ताव अब तक दो एजेंडों के बीच लटकते रहे हैं. एक तरफ़ तो दूसरे देशों में लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की बात है, तो दूसरी तरफ़ लोकतांत्रिक देशों के बीच अपने यहां के लोकतंत्र में आई कमियों को दूर करने के सबक़ साझा करने का तर्क भी दिया जाता है. ये अंतर एक अकादेमिक बहस और बनावटी फ़र्क़ में तब्दील हो सकता है, ख़ासतौर से तब और जब इन देशों के एजेंडे में चीन की चुनौती से निपटना, सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाए. लेकिन, एक बात तो बिल्कुल तय है. 6 जनवरी के हमले ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन अब लोकतंत्र की कमज़ोरियों के बारे में ज़्यादा गंभीरता से विचार करेगा.

ब्राज़ील पर ट्रंप का संक्रामक असर हुआ है
ओलिवर स्टुएंकेल
एसोसिएट प्रोफ़ेसर ऑफ़ इंटरनेशनल रिलेशंस, गेटुइलो वर्गा फाउंडेशन, ब्राज़ील
ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हार एक तबाही से कम नहीं है. 2016 के चुनाव में ट्रंप की जीत ने दो साल बाद, ब्राज़ील में राष्ट्रपति पद के लिए न सिर्फ़ बोल्सोनारो की असभ्य और आक्रामक उम्मीदवारी को जायज़ बना दिया था, बल्कि ट्रंप की अनिश्चित और अस्थिर विदेश नीति ने दुनिया का ध्यान इस कदर अपनी ओर आकर्षित कर लिया था कि लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ब्राज़ील की क्रांतिकारी विदेश नीति की उसे कौन सी क़ीमत चुकानी पड़ी है. इस विदेश नीति के तहत बोल्सोनारो नियमित रूप से अर्जेंटीना, चीन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र और न जाने किस किस पर ज़ुबानी हमले करते रहे. हालांकि, बोल्सोनारो के वफ़ादार समर्थकों के बीच उनकी ये बयानबाज़ी काफ़ी पसंद की जाती है. वैसे तो बोल्सोनारो, पिछले दो वर्षों के दौरान ट्रंप की हवा में बहने का फ़ायदा उठाते रहे. लेकिन, अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ब्राज़ील की भू-मंडलीकरण विरोधी विदेश नीति में और बढ़ोत्तरी होने की आशंका है.
ब्राज़ील में जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि ट्रंप की हार के बाद, बोल्सोनारो अब ज़्यादा व्यवहारिक तरीक़े अपनाएंगे, उनकी उम्मीद अमेरिका में पिछले नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के फ़ौरन बाद ही तब टूट गई थी, जब बोल्सोनारो ने ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए अमेरिका के चुनाव में फ़र्ज़ीवाड़े के इल्ज़ाम दोहराए थे. ब्राज़ील के विदेश मंत्री, अर्नेस्टो हेनरिक़ फ्रागा अराउओ, डोनाल्ड ट्रंप के अंधभक्त हैं. उन्होंने ट्रंप को ‘पश्चिम का मसीहा’ बताते हुए उनकी तारीफ़ की थी. हेनरिक़ ने तो ये चर्चा करने तक से इनकार कर दिया था कि ट्रंप के बाद के दौर में ब्राज़ील को कैसी विदेश नीति अपनानी चाहिए.
बहुत से लोग ये मानते हैं कि बोल्सोनारो के इन बयानों का मक़सद, ब्राज़ील की चुनाव व्यवस्था में वहां की जनता भरोसा डिगाना है. बहुत से विश्लेषक तो ये सोचकर चिंतित हैं कि हो सकता है कि अगर 2022 में ख़ुद बोल्सोनारो चुनाव हारते हैं, तो शायद वो भी नतीजों को स्वीकार न करें.
लोकतांत्रिक तरीक़े से चुने गए नेताओं द्वारा जो बाइडेन को जीत की बधाई देने वाले जायर बोल्सोनारो आख़िरी व्यक्ति थे. वो लगातार अमेरिका के चुनाव में फ़र्ज़ीवाड़े की बातें करते रहे थे. बहुत से लोग ये मानते हैं कि बोल्सोनारो के इन बयानों का मक़सद, ब्राज़ील की चुनाव व्यवस्था में वहां की जनता भरोसा डिगाना है. बहुत से विश्लेषक तो ये सोचकर चिंतित हैं कि हो सकता है कि अगर 2022 में ख़ुद बोल्सोनारो चुनाव हारते हैं, तो शायद वो भी नतीजों को स्वीकार न करें. सबसे ज़्यादा चिंता तो इस बात को लेकर है कि अमेरिका के सैनिक जनरलों के उलट, ब्राज़ील में लोकतंत्र को लेकर सैन्य अधिकारियों का रुख़ दुविधा भरा रहा है.
जायर बोल्सोनारो ने अमेरिकी संसद पर हमले की खुलकर आलोचना करने से भी इनकार कर दिया था, और उनके विदेश मंत्री ने तो अमेरिकी संसद पर हमला करने वालों को ‘अच्छे लोग’ कहा था. इन बयानों से न केवल आने वाले समय में ब्राज़ील की विदेश नीति की दशा-दिशा तय हो जाती है, बल्कि अगले दो सालों के दौरान, ब्राज़ील की घरेलू राजनीति की हवा का रुख़ भी तय हो गया है. जो बाइडेन प्रशासन के लिए, बोल्सोनारो एक दुविधा का नाम है. एक तरफ़ तो जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ युद्ध, ब्राज़ील सक्रिय सहयोग के बिना अधूरा रहने वाला है. जबकि जलवायु परिवर्तन, जो बाइडेन प्रशासन की नीतियों का एक प्रमुख स्तंभ है. इसके अलावा लैटिन अमेरिका में चीन का प्रभाव कम करने में ब्राज़ील की बोल्सोनारो सरकार, अमेरिका की साझीदार साबित हो सकती है. फिर भी, बोल्सोनारो द्वारा ख़ुद को ट्रंपवाद के संरक्षक के रूप में पेश करने और अमेरिका के कट्टर दक्षिणपंथियों द्वारा प्रचारित साज़िश के तमाम क़िस्सों को हवा देने के कारण, अमेरिकी महाद्वीप के दो सबसे बड़े देशों के बीच सक्रिय रूप से आपसी सहयोग की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं.

दक्षिण अफ्रीका के लिए एक सबक़
एलिज़ाबेथ सिडिरोपोउलॉस
चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरेशनल अफेयर्स, साउथ अफ्रीका
1994 में जबसे दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तब से देश में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के दबदबे वाली सरकार, अमेरिका को कई मुद्दों पर साझीदार मानती आयी है. लेकिन, अमेरिका द्वारा दुनिया के तमाम हिस्सों में दख़लंदाज़ी की दक्षिण अफ्रीका की सरकार लगातार आलोचना भी करती रही है. साउथ अफ्रीका, कई बार अमेरिका को साम्राज्यवादी शक्ति कहता रहा है. संयुक्त राष्ट्र में भी अक्सर दोनों देश प्रतिबंधों और मानव अधिकारों को लेकर आमने सामने रहे हैं. इसके अलावा मध्य पूर्व-ख़ास तौर से इज़राइल-फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया और ईरान को लेकर भी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच टकराव होता आया है. इसके साथ-साथ अमेरिका में नस्लवाद और असमानता के मुद्दे, दक्षिण अफ्रीका में भी उठते रहे हैं. इसकी वजह ये है कि ख़ुद दक्षिण अफ्रीका भी नस्लवादी शोषण का शिकार रहा है.
हालांकि, जो बाइडेन प्रशासन का रवैया डोनाल्ड ट्रंप से अलग रहने वाला है. लेकिन, अमेरिकी कैपिटॉल की घटनाओं से विश्व में अमेरिका की साख को झटका लगा है. अमेरिकी संसद पर कट्टरपंथियों के हमले से, अमेरिका के समावेशी लोकतंत्र के बजाय, नस्लवादी समाज होने की सोच मज़बूत हुई है.
अगर, जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका बहुपक्षीयवाद को अपनाता है और तमाम क्षेत्रों से संवाद की कोशिश करता है, तो भी दक्षिण अफ्रीका उसे शक की नज़र से ही देखेगा. फिर चाहे मामला अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या विश्व स्वास्थ्य संगठन का हो-या फिर अमेरिका द्वारा चीन और रूस जैसे जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों से निपटने का तौर तरीक़ा. वैश्विक संस्थानों में, दक्षिण अफ्रीका अपनी स्वतंत्र नीति पर चलने की कोशिश करता रहेगा. दक्षिण अफ्रीका, अन्य नीतियों के अलावा प्रतिबंध लगाने का ख़ास तौर से विरोध करता रहा है (फिर चाहे वो प्रतिबंध ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हों या ईरान के). इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, फिलिस्तीन और सहरावी के आत्म-निर्णय के अधिकार का भी समर्थन करता आया है. वो हर देश द्वारा अपने विकास के लिए सबसे उचित तकनीक (उदाहरण के लिए 5G) चुनने के अधिकार और वैश्विक संस्थाओं में तुरंत सुधार करने का भी समर्थक रहा है. इसके साथ साथ, दक्षिण अफ्रीका इस मजबूरी से भी बचना चाहेगा कि अंतरराष्ट्रीय संवादों में उसे चीन या अमेरिका में से किसी एक पक्ष का चुनाव करना पड़े. दक्षिण अफ्रीका और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को विकास और संघर्ष की चुनौतियों से निपटने में अमेरिका और चीन, दोनों की ही मदद की ज़रूरत है.
अगर, जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका बहुपक्षीयवाद को अपनाता है और तमाम क्षेत्रों से संवाद की कोशिश करता है, तो भी दक्षिण अफ्रीका उसे शक की नज़र से ही देखेगा. फिर चाहे मामला अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या विश्व स्वास्थ्य संगठन का हो-या फिर अमेरिका द्वारा चीन और रूस जैसे जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों से निपटने का तौर तरीक़ा.
हालांकि, 6 जनवरी की घटनाओं में, दक्षिण अफ्रीका को सावधान करने वाले कई सबक़ हैं. पहली बात तो ये दक्षिण अफ्रीका ख़ुद अपने लोकतंत्र को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकता है; उसे अपने लोकतंत्र को भी लगातार पोषित करने की ज़रूरत है. दूसरी बात, घरेलू क़दम विदेश नीति के लिहाज़ से भी अहम होते हैं, क्योंकि ये क़दम दुनिया में उस देश की हैसियत या बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं. इसके अलावा घरेलू हालात के दम पर ही कोई भी देश, अपने मूल्यों के प्रति अन्य देशों का ध्यान आकर्षित कर सकता है. अफ्रीकी महाद्वीप में लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था, जवाबदेही और अच्छे प्रशासन को को बढ़ावा देने में दक्षिण अफ्रीका के अपने हित भी हैं. लेकिन, दक्षिण अफ्रीका को इस मामले में अपने यहां के हालात सुधारने की ज़रूरत है, तभी वो दूसरे देशों के लिए मिसाल बन सकेगा. इसके लिए ज़रूरी है कि दक्षिण अफ्रीका अपने यहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करे, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करे, सामाजिक असमानता की चुनौती का सामना करे, तभी वो उग्र राष्ट्रवादी और जनवादी ताक़तों को कमज़ोर कर सकेगा.

अमेरिका के दुनिया के साथ फिर से जुड़ने और विनम्रता की ज़रूरत है
सेलिम येनेल
प्रेसिडेंट,ग्लोबल रिलेशंस फोरम, तुर्की
अमेरिकी कैपिटॉल पर हमले का वर्णन करने के लिए पहले ही बहुत से विशेषणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन, मेरी नज़र में सबसे उचित शब्द होगा, ‘ख़ौफ़नाक’. ये एक ऐसा मंज़र था, जिसे हम आमतौर पर अलग तरह की हुकूमतों के दौरान देखते हैं.
इसके बावजूद, हमें इस हमले के प्रतिकार को भी सम्मान देना चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को नकारने की कोशिशों के बावजूद, अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था ने अपनी मज़बूती और लचीलेपन का परिचय दिया है. 6 जनवरी के ख़ौफ़नाक नाटक के बावजूद, हमने देखा है कि अमेरिकी लोकतंत्र ने पिछले दो महीनों के दौरान किस तरह से अपनी हिफ़ाज़त की.
इसमें कोई दो राय नहीं कि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के इन ज़ख़्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे. हो सकता है कि बाइडेन, ट्रंप द्वारा ठुकराए गए अंतरराष्ट्रीय समझौतों में दोबारा शामिल होने के अलावा, विदेश नीति के अन्य मसलों पर शायद तुरंत ध्यान न दें. ये भी संभव है कि मोटे तौर पर मार्गदर्शन करने के अलावा, जो बाइडेन अपनी विदेश नीति की टीम को ही ये स्वतंत्रतता दे दें कि वो उनके विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाए.
नए राष्ट्रपति के लिए ये साबित करना सबसे बड़ा काम होगा कि पिछले चार वर्ष अमेरिका की विदेश नीति के अपवाद थे. बाइडेन को दुनिया को ये यक़ीन दिलाना होगा कि उनके देश की नीति में कोई संरचात्मक बदलाव नहीं आया है.
6 जनवरी की घटनाओं के चलते हो सकता है कि जो बाइडेन, मानव अधिकारों और अन्य स्वतंत्रताओं को विदेश नीति का हथियार बनाने में हिचकें. इस मामले में कुछ विनम्रता उनके काम आ सकती है. नए राष्ट्रपति के लिए ये साबित करना सबसे बड़ा काम होगा कि पिछले चार वर्ष अमेरिका की विदेश नीति के अपवाद थे. बाइडेन को दुनिया को ये यक़ीन दिलाना होगा कि उनके देश की नीति में कोई संरचात्मक बदलाव नहीं आया है. बाइडेन को दुनिया को दिखाना होगा कि अमेरिका में लोकतंत्र के मूलभूत गुण, क़ानून का राज, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की आज़ादी आज भी बुनियादी सिद्धांत बने हुए हैं.
दुनिया के तमाम अन्य देशों की तरह तुर्की भी, अमेरिका की नई सरकार के साथ तालमेल बिठाएगा. उम्मीद यही है कि अमेरिका एक ऐसी विदेश नीति के रास्ते पर लौटेगा, जिससे दुनिया परिचित है और जिसका अंदाज़ा लगाना संभव है. फिर भी, दुनिया को ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि जो बाइडेन के शासन काल में बराक ओबामा के दौर की नीतियां हू-ब-हू लागू की जाएंगी. इसकी वजह ये है कि बराक ओबामा और उनके तत्कालीन उप-राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे. इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बाइडेन, विदेश नीति के एजेंडे पर अपनी अलग छाप छोड़ेंगे.
अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अमेरिका की भागीदारी और बढ़नी तय है. कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा कि दुनिया में एक ऐसे वैश्विक नेतृत्व का अभाव रहा, जिसकी सख़्त ज़रूरत थी. इस महामारी से निपटने के लिए, विश्व में जिस आपसी सहयोग और सघन अभियान की ज़रूरत थी, उसकी कमी लगातार बनी रही थी. अगर अमेरिका तमाम देशों के साथ गठबंधन बनाने की भूमिका के साथ विश्व पटल पर लौटता है, तो इसका ज़्यादातर देश स्वागत करेंगे.
तुर्की भी नए अमेरिकी प्रशासन के साथ सकारात्मक और असरदार तरीक़े से संवाद करने की कोशिश करेगा. कई विषय ऐसे होंगे, जिसमें क्रिएटिव कूटनीतिक तरीक़े अपनाने होंगे: तुर्की द्वारा रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदना, सीरिया में आतंकवाद से लड़ने के तौर-तरीक़ों पर मतभेद और तुर्की में 2016 के नाकाम तख़्तापलट के मास्टरमाइंड समझे जाने वाले फेतुल्लाह गुलेन का प्रत्यर्पण तो बस ऐसे कुछ गिने चुने मुद्दे हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.








 PREV
PREV