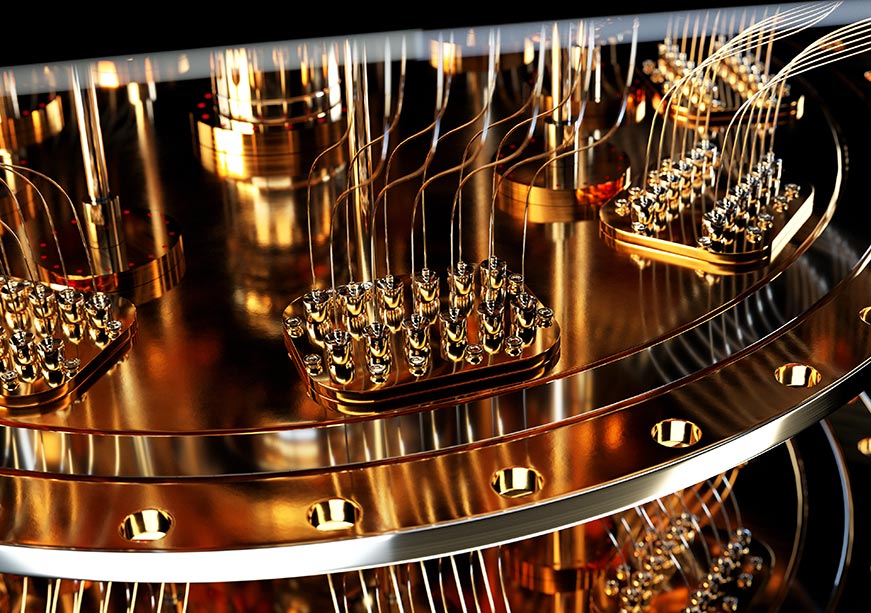बहुत से विकासशील देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ बढ़ाने वाली ग़ैर संक्रामक बीमारियों में तंबाकू का बड़ा योगदान है. तंबाकू का नियमित रूप से इस्तेमाल करना अभी भी जनता की सेहत की एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, ख़ास तौर से भारत और चीन में, जो तंबाकू की खपत की ऊंची दर वाले दुनिया की दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं. युवाओं में ई-सिगरेट के बढ़ते चलन की वजह से इस मसले में नया आयाम जुड़ गया है, जिससे तंबाकू नियंत्रण की कोशिशों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे था. इस बार इसकी थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग की दख़लंदाज़ी से बचाना था. ऐसे में ये बिल्कुल सही वक़्त है, जब हम भारत और चीन में तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण के ऐतिहासिक और तुलनात्मक पहलुओं की पड़ताल करें, क्योंकि ये दोनों देश तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं. इस लेख का मक़सद तंबाकू के उपयोग का विकास और भारत एवं चीन में उसके नियंत्रण के प्रयासों का विश्लेषण करना है, जिसके अंतर्गत प्रमुख बदलावों और मौजूदा चलनों को रेखांकित किया जाएगा.
इस लेख का मक़सद तंबाकू के उपयोग का विकास और भारत एवं चीन में उसके नियंत्रण के प्रयासों का विश्लेषण करना है, जिसके अंतर्गत प्रमुख बदलावों और मौजूदा चलनों को रेखांकित किया जाएगा.
ऐतिहासिक संदर्भ और तंबाकू उत्पादकों की स्थिति
चीन में तंबाकू मिंग राजवंश के शासन काल में पहुंचा था, और सिगरेट और पाइप से धूम्रपान ज़रिए तंबाकू का उपयोग सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अहम हो गया. बीसवीं सदी के दौरान तंबाकू उद्योग का काफ़ी विस्तार हुआ, जिससे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और मज़बूत हो गई. अब चीन दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें चाइना नेशनल टोबैको कॉरपोरेशन (CNTC) मुख्य भूमिका निभाता है. 2021 में चीन ने 938,468 हेक्टेयर में तंबाकू की खेती की थी, जिसमें 2,122,877 टन तंबाकू का उत्पादन हुआ था, इस वक़्त दुनिया भर में जितने इलाक़े में खेती होती है, उसमें से तीस प्रतिशत अकेले चीन में है और तंबाकू के कुल वैश्विक उत्पादन में चीन का योगदान 36.2 प्रतिशत का है (Figure 1). चीन का तंबाकू उद्योग न केवल विशाल घरेलू मांग को पूरा करता है, बल्कि ये निर्यात में भी काफ़ी योगदान देता है. चीन का तंबाकू सेक्टर उसकी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और सरकार के कुल राजस्व में CNTC का योगदान 7 फ़ीसद से अधिक का है.
एक मोटे अनुमान के मुताबिक़, देश में तंबाकू की खेती और इसकी प्रोसेसिंग में लगभग 3.6 करोड़ लोग लगे हुए हैं.
भारत में तंबाकू के इस्तेमाल की शुरुआत मुग़ल दौर में हुई थी और बहुत जल्दी ही ये देश के सांस्कृतिक चलन का हिस्सा बन गया. जैसे कि बीड़ी और हुक्का पीना और तंबाकू के साथ पान खाना. 17वीं सदी आते आते, तंबाकू का भारतीय समाज में काफ़ी अहम स्थान हो गया था. उपनिवेशवादी शासन के दौरान तंबाकू उद्योग बड़ी तेज़ी से फला-फूला और स्वतंत्रता के बाद तंबाकू उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का अहम सेक्टर बन गया. आज भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, फिर चाहे क्षेत्रफल के लिहाज़ से हो या फिर उत्पादन के नज़रिए से. 2021 में भारत में 432,840 हेक्टेयर इलाक़े में तंबाकू की खेती हुई थी और 757,513 टन उत्पादन हुआ था. क्षेत्रफल के लिहाज़ से ये दुनिया का 13 प्रतिशत था, तो उत्पादन के मामले में 12.9 फ़ीसद था. इस उद्योग के अहम खिलाड़ी जैसे कि ITC लिमिटेड का बाज़ार में दबदबा है और खेती एवं निर्माण के ज़रिए ये सेक्टर काफ़ी रोज़गार भी देता है. भारत में तंबाकू की आर्थिक अहमियत इस लिहाज़ से काफ़ी है महत्वपूर्ण है कि इससे करोड़ों किसानों और मज़दूरों की रोज़ी-रोटी चलती है. एक मोटे अनुमान के मुताबिक़, देश में तंबाकू की खेती और इसकी प्रोसेसिंग में लगभग 3.6 करोड़ लोग लगे हुए हैं.
यहाँ ग्राफ़ है...
तंबाकू के उपयोग के मौजूदा आंकड़े और सरकार के क़दम
भारत और चीन में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल को लागू करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है. चीन में तंबाकू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सिगरेट पीने में होता है, जो सांस्कृतिक व्यवहार में बहुत गहरे से रचा बसा है. ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) के आंकड़े बताते हैं कि चीन में 26.6 प्रतिशत वयस्क लोग (50.5 फ़ीसद पुरुष और 2.1 प्रतिशत महिलाएं) सिगरेट पीते हैं. चीन की तंबाकू नियंत्रण की नीतियों को टोबैको मोनोपोली लॉ और तमाम सरकारी और स्थानीय नियमों के ज़रिए लागू किया जाता है. नीतियों को लागू करने में CNTC का काफ़ी प्रभाव है. इस वजह से स्वास्थ्य की चेतावनी और विज्ञापन पर पाबंदी लागू करने जैसे क़दमों को अक्सर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. चीन के जन स्वास्थ्य के अभियानों की कोशिश तंबाकू की खपत और इससे जुड़े स्वास्थ्य के जोखिमों को कम करने की होती है. इनमें मीडिया के अभियान और स्कूल पर आधारित कार्यक्रम शामिल हैं.
ई-सिगरेट का बढ़ता इस्तेमाल, विशेष रूप से युवाओं के बीच चलन ने दोनों ही देशों में तंबाकू नियंत्रण के मंज़र में एक नया आयाम जोड़ दिया है. ई-सिगरेटों का प्रचार, तंबाकू के पारंपरिक उत्पादों की तुलना में सुरक्षित बताकर किया जाता है.
भारत में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) जैसे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यहां तंबाकू का काफ़ी इस्तेमाल होता है. हालांकि इसमें उम्र, लैंगिकता और शहरी एवं ग्रामीण इलाक़ों के बीच काफ़ी अंतर देखने को मिलता है. GATS के 2016-17 के ताज़ा उपलब्ध सर्वेक्षण के मुताबिक़ भारत में 28.6 प्रतिशत वयस्क नागरिक (42.4 प्रतिशत पुरुष और 14.2 फ़ीसद महिलाएं) तंबाकू के उत्पादों का उपयोग करते हैं. सर्वेक्षण के समय ग्रामीण क्षेत्रों में हर तीन में से एक वयस्क (32.5 प्रतिशत) और शहरी इलाक़ों में हर पांच में से एक (21.2) व्यक्ति, तंबाकू का उपयोग कर रहा था. बीड़ी, सिगरेट और धुआं मुक्त तंबाकू, इसकी खपत के प्रमुख तरीक़े हैं. भारत में तंबाकू के इस्तेमाल को सीमित करने के प्रमुख उपायों में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (COPTA) और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) हैं, जिनका लक्ष्य स्वास्थ्य की चेतावनियां देना, विज्ञापन पर रोक लगाना और धुआं मुक्त क़ानून लागू करना है. काफ़ी प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं.
ई-सिगरेट का बढ़ता इस्तेमाल, विशेष रूप से युवाओं के बीच चलन ने दोनों ही देशों में तंबाकू नियंत्रण के मंज़र में एक नया आयाम जोड़ दिया है. ई-सिगरेटों का प्रचार, तंबाकू के पारंपरिक उत्पादों की तुलना में सुरक्षित बताकर किया जाता है. हालांकि, उनके दूरगामी असर अभी स्पष्ट नहीं हैं. चीन में मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों के बीच ई-सिगरेट का चलन बढ़ता जा रहा है. भारत में वैसे तो ई-सिगरेट पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है. लेकिन, चीन में बनी ई-सिगरेट की सड़कों पर उपलब्धता एक अहम नीतिगत चुनौती बनी हुई है. ये नया चलन, युवा आबादी के बीच तंबाकू का इस्तेमाल घटाने के मामले में हुई प्रगति के लिए ख़तरा बना हुआ है.
आगे का रास्ता
तंबाकू नियंत्रण की नीतियों की कड़ाई और उन्हें लागू करने के मामले में चीन और भारत के बीच काफ़ी अंतर है. वैसे तो दोनों ही देशों को इस मामले में कुछ सफलताएं मिली हैं. लेकिन, चीन की तुलनात्मक रूप से तंबाकू पर अधिक आर्थिक निर्भरता, इसकी खपत कम करने की कोशिशों को जटिल बना देती है. दोनों ही देशों में तंबाकू के इस्तेमाल को लेकर जो सांस्कृतिक सोच है, वो भी खपत के पैटर्न और उन्हें कम करने की कोशिशों पर काफ़ी असर डालती है. तंबाकू के इस्तेमाल में सामाजिक आर्थिक कारण भी अहम भूमिका निभाते हैं और दोनों ही देशों में तंबाकू का उद्योग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है.
तुलनात्मक अध्ययनों में पाया गया है कि चीन और भारत दोनों ने ही FCTC को लागू करने के मामले में काफ़ी कोशिशें की हैं. फिर भी उनके सामने अनूठी चुनौतियां रही हैं और सफलता के स्तर भी अलग अलग रहे हैं.
हाल के अध्ययन दिखाते हैं कि चीन की सरकार की कई अहम पहलों के बावजूद वहां तंबाकू का उपयोग कम करने के प्रयासों के मिले-जुले नतीजे ही निकले हैं. चीन ने 2005 में ही WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल पर मुहर लगा दी थी. इसकी वजह से तंबाकू पर टैक्स, विज्ञापनों पर पाबंदी और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध जैसे कई उपाय लागू किए गए थे. हालांकि, इन्हें लागू करनी प्रक्रिया अनियमित रही है, ख़ास तौर से इस उद्योग में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के दबदबे की वजह से. GATS के चीन के 2010 से 2018 के बीच के तुलनात्मक आंकड़ों के मुताबिक़, वयस्कों के बीच तंबाकू के इस्तेमाल का चलन स्थिर बना हुआ है और 2010 में 28.1 प्रतिशत की तुलना में 2018 में ये घटकर 26.6 फ़ीसद रह गया था. मर्दों के बीच धूम्रपान का चलन 52.9 प्रतिशत से घटकर 50.5 फ़ीसद रह गया था. वहीं, महिलाओं के बीच इसके चलन में 2.4 से 2.1 फ़ीसद की मामूली कमी दर्ज की गई थी. चीन की सरकार का हेल्थ चाइना इनिशिएटिव 2030 के एजेंडे का लक्ष्य धूम्रपान के चलन को कम करना है. लेकिन, तंबाकू पर कम टैक्स और पैकेटों पर अस्पष्ट चेतावनी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. इनकी वजह से जन स्वास्थ्य में अहम सुधार लाने के लिए मज़बूत नीतियों और उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने की ज़रूरत बनी हुई है.
वहीं, हाल के मूल्यांकनों से पता चलता है कि क़ानूनी उपायों और जन स्वास्थ्य के कार्यक्रमों के ज़रिए भारत ने तंबाकू के नियंत्रण के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. COTPA और NTCP, दोनों की वजह से तंबाकू के इस्तेमाल के चलन में काफ़ी कमी आई है. GATS के आंकड़े संकेत देते हैं कि 2009-10 में जहां 34.6 प्रतिशत वयस्क तंबाकू इस्तेमाल करते थे. वहीं, 2016-17 में ये घटकर 28.6 प्रतिशत रह गया था. इन प्रगतियों के बावजूद राज्यों के बीच अलग अलग राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भों, तंबाकू के इस्तेमाल की सामाजिक स्वीकार्यता और लागू करने की चुनौतियों की वजह से तंबाकू नियंत्रण के नियम लागू करने के मामले में भी अंतर देखने को मिलता है. आगे प्रगति के लिए नीतियां लागू करने और जनता को जागरूक करने के प्रयासों की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है. इसके साथ साथ भारत में तंबाकू के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है.
तुलनात्मक अध्ययनों में पाया गया है कि चीन और भारत दोनों ने ही FCTC को लागू करने के मामले में काफ़ी कोशिशें की हैं. फिर भी उनके सामने अनूठी चुनौतियां रही हैं और सफलता के स्तर भी अलग अलग रहे हैं. चीन में तंबाकू उद्योग के दबदबे की वजह से FCTC के उपायों का असर सीमित रहा है, जिसकी वजह से धूम्रपान के स्तर में मामूली कमी ही आ सकी है. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि GATS के आंकड़े दिखाते हैं कि धूम्रपान की दर में मामूली कमी ही दर्ज की गई है और चीन में तंबाकू पर कम टैक्स और चेतावनी के कमज़ोर लेबल बने हुए हैं, जिन्हें देखते हुए मज़बूत नीतियां बनाकर उन्हें सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है. इसके उट भारत ने COTPA और NTCP वैधानिक उपायों को लागू करके काफ़ी प्रगति हासिल की है, जिसकी वजह से तंबाकू के इस्तेमाल में उल्लेखनीय ढंग से कमी आई है,. हालांकि, अलग अलग राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भों के चलते राज्यों के बीच ये उपाय लागू करने के अंतर बने हुए हैं. इस बार के वर्ल्ड नो टोबैको डे को मनाते हुए, बच्चों को तंबाकू उद्योग की दखलंदाज़ी से बचाना और ई-सिगरेट की बढ़ती चुनौती से निपटने को तंबाकू नियंत्रण की वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीतियों में सबसे आगे रखा जाना चाहिए.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV