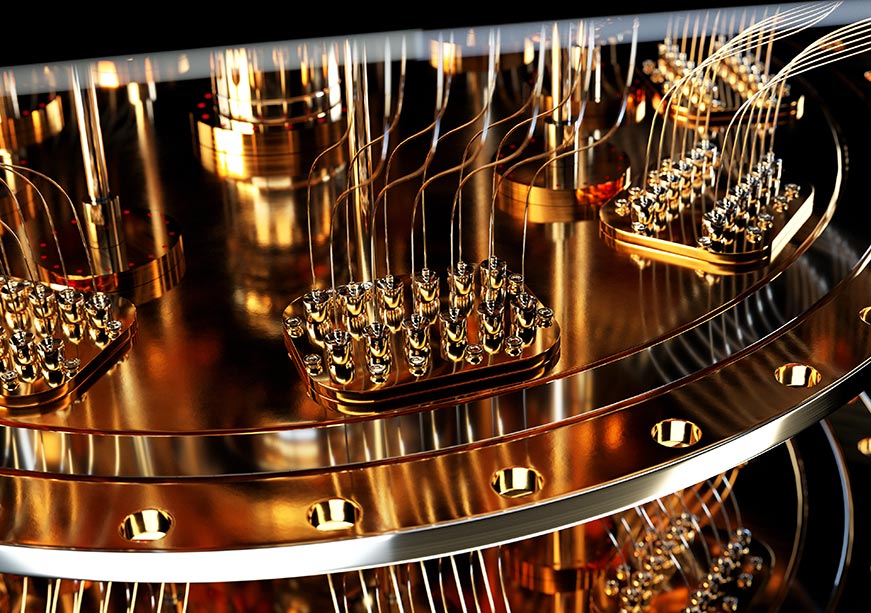हाल ही में क़तर (Qatar) के 45 सदस्यीय शूरा परिषद (Consultative Assembly of Saudi Arabia/Shura Council) के लिए चुनाव आयोजित किए गए, जिसे 2004 के संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया था लेकिन “राष्ट्रीय हित” में बार-बार इस चुनाव को आयोजन कराने में देरी हो रही थी, आखिरकार 2 अक्टूबर को चुनाव कराए गए. ना सिर्फ़ क़तर के अंदर बल्कि बाहर भी इन चुनावों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार और आशावाद का माहौल रहा. इसे लेकर जो आधिकारिक स्थिति थी वह यह कि मुल्क के अंदर लोकतंत्र बहाल करने को लेकर यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इतना ही नहीं, यह क्षेत्र के अन्य अरब देशों के बीच एक प्रगतिशील और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में देखे जाने की कतर की महत्वाकांक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है. क़तर के डिप्टी प्रधानमंत्री शेख अब्दुल रहमान थानी (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani) ने इन सुधारों को ‘नया प्रयोग’ बताया. एक अदने से खाड़ी देश में यह अपने आप में पहला चुनाव था लेकिन वोटरों और काउंसिल के सदस्यों पर कई तरह की पाबंदियां इसकी तुरंत होने वाली नीतियों के असर को सीमित कर देती हैं.
क़तर के डिप्टी प्रधानमंत्री शेख अब्दुलरहमान थानी ने इन सुधारों को ‘नया प्रयोग’ बताया. एक अदने से खाड़ी देश में यह अपने आप में पहला चुनाव था लेकिन वोटरों और काउंसिल के सदस्यों पर कई तरह की पाबंदियां इसकी तुरंत होने वाली नीतियों के असर को सीमित कर देती हैं.
शुरुआत में यह उम्मीद करना जल्दबाजी होगी कि केवल एक सलाहकार निकाय के लिए सफल चुनाव से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन ना किया जाए. सत्ताधारी दल, जो राजनीतिक भागीदारी के लिए बेहद लापरवाह है, जो उनके नियंत्रण को ख़तरा पैदा कर सकता है, जो ख़ुद के एकाधिकार के लिए झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता है. दशकों से उन्होंने अपनी शक्ति को मज़बूत करने के लिए एक ‘लचीलापन रणनीति’ को विकसित किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनका उदय एक कुलीनतंत्र शासक के रूप में हुआ है जिसमें अमीर और उसके परिवार के सदस्य शामिल हैं. इस तरह यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के सुधार से कोई सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलना है. पहले के सुधार वास्तव में सभी क़तर के समान प्रतिनिधित्व के मुख्य मुद्दों को संबोधित नहीं करते थे. इस प्रकार, जब तक सत्ता के मुख्य हिस्सेदार प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा नहीं देते, लोकतंत्र स्थापना की बात महज़ एक बहाना ही रहेगा.
शूरा काउंसिल
1970 में शूरा परिषद की स्थापना की गई, लिहाज़ा इसे नई परिकल्पना नहीं कहा जा सकता है. इसकी शुरुआत में, इस परिषद में शेख परिवार के 15 सदस्य ही शामिल थे. अब शूरा परिषद में 45 सदस्य हैं, जिसमें 30 सदस्यों का चुनाव क़तर की जनता करती है. जबकि 15 बाकी सदस्यों का चुनाव अमीर ख़ुद करते हैं, ये तब हुआ है जबकि चुनाव के बाद “जनहित” के लिए किसी भी कानून द्वारा इसे निर्दिष्ट नहीं किया गया था, यहां तक कि संविधान द्वारा भी यह निर्धारित नहीं किया गया था. मनमाना मतदाता मताधिकार राजनीतिक भागीदारी के सिद्धांत को कमजोर करता है. इसके चलते चुनावों की घोषणा के समय चुनावी समावेशी और नागरिकता के बारे में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बहस छिड़ गई थी. अलमुर्राह कबीले वालों ने नागरिकता कानून के ख़िलाफ़ ज़बर्दस्त विरोध किया था क्योंकि इन लोगों ने कुछ सदस्यों को बेदख़ल कर दिया था.
खाड़ी देशों में इन सुधारों का कोई क्रांतिकारी बदलाव से संबंध नहीं रहा क्योंकि पहले के किए गए सुधारों का कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला था. इसी वजह से ये सुधार महज दिखावा प्रतीत होते हैं जिसका संबंध अगले साल फीफा विश्व कप की मेजबानी से है.
खाड़ी देशों में इन सुधारों का कोई क्रांतिकारी बदलाव से संबंध नहीं रहा क्योंकि पहले के किए गए सुधारों का कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला था. इसी वजह से ये सुधार महज दिखावा प्रतीत होते हैं जिसका संबंध अगले साल फीफा विश्व कप की मेजबानी से है. यह इस क्षेत्र में एक प्रगतिशील और उदार पश्चिमी सहयोगी के रूप में वैश्विक स्तर पर छवि निर्माण की एक कोशिश है. इसलिए, ऐसे सुधारों का राज्य की घरेलू गतिशीलता पर मामूली असर पड़ेगा. अन्य खाड़ी देशों में भी राजनीतिक सुधार हुए हैं लेकिन यह क्षेत्र अभी भी ज़रूरत से ज़्यादा केंद्रीकृत है और यहां कबिलाई राजनीति का प्रभुत्व बना हुआ है. ओमान ने भी अपनी राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाया है; सऊदी अरब राजनीतिक सुधार की राह पर है. कुवैत में एक अधिक जागृत नागरिक समाज की मौजूदगी में संसद है. हालांकि कतर इस दौड़ में काफी देर से शामिल हुआ है और हाल के सुधारों को अन्य जीसीसी सदस्यों की तरह ही लागू करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है. लेकिन कतर के मुकाबले इन देशों में संस्थागत गंभीरता और विविधता ज़्यादा है.
वैसे राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए सुधारों का परीक्षण एक तरफ सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल से संभव है, जो एक ओर परंपराओं बनाम आधुनिकतावाद और दूसरी ओर राजनीतिक सुधार बनाम राज्य की संरचनात्मक संरचना से पैदा होती है. परंपरा, धन और आधुनिकता में संतुलन की चुनौतियों के साथ कतर की राजनीतिक व्यवस्था में अभी भी बदलाव देखा जाना बाकी है. क्योंकि ये सुधार अभी भी उस दिशा में अग्रसर होते नहीं दिख रहे हैं जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और सियासत को चुनौती दे सके.
जबकि सुधारों का इरादा व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए शूरा परिषद का विस्तार करना है और सत्ता के केंद्रीकरण और राजनीतिक हाशिए पर जाने से सवाल यह पैदा होता है कि ये सुधार उनके घोषित इरादे पर कितना खरा उतर सकेंगे. परिषद का स्वरूप सलाहकार जैसा है और मौजूदा स्थितियों को बदलने वाले किसी भी सुझावों को आमीर रद्द करने की एकतरफा शक्ति रखते हैं.
क़तर में लागू किया जाने वाला नागरिकता अधिनियम, सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की जीवन रेखा कही जा सकती है क्योंकि यह ‘रणनीतिक हाशिए पर’ आर्थिक प्रोत्साहन को लोगों के एक छोटे से समूह, जिसका मतलब ख़ुद शासक परिवार है, उस तक सीमित रखने में मदद करता है. यह राष्ट्र के संस्थानों को परिवार के नियंत्रण में रखने में भी मदद करता है, जो उन विशेषाधिकारों का फायदा उठाते हैं जिसके तहत उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और जिसमें मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा, सब्सिडी और शिक्षा भी शामिल है. लेकिन शासन और उसके कार्यों को वैधता प्रदान करने वाला ‘नागरिक मिथक’ इन सुधारों के प्रभाव के बारे में संभावित संदेह को बढ़ावा देता है.
क़तर में लागू किया जाने वाला नागरिकता अधिनियम, सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की जीवन रेखा कही जा सकती है क्योंकि यह ‘रणनीतिक हाशिए पर’ आर्थिक प्रोत्साहन को लोगों के एक छोटे से समूह, जिसका मतलब ख़ुद शासक परिवार है, उस तक सीमित रखने में मदद करता है.
दूसरा सवाल यह है कि क्या इस तरह के विस्तार से नई ताकतों को शामिल किया जाएगा जिससे कि एक नया लोकतांत्रिक ख़ाका तैयार किया जा सके. यह देखा गया है कि पहले किए गए किसी भी सुधार के परिणामस्वरूप अकेले शाही परिवार का ही विस्तार हुआ है, ना कि राजनीतिक भागीदारी इससे बढ़ी है. बावजूद सरकारी पाबंदियों के सफलता से म्युनिसिपल चुनाव कराना, महिला सशक्तिकरण, न्यायिक स्वततंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायिक परिषद, संविधान का निर्माण, शूरा परिषद के विस्तार के लिए राजनीतिक सुधार के जरिए संसद के निर्माण को प्रस्तावित करना, शाही परिवार की असीम शक्तियों में कोई कमी नहीं आई है. कुछ विश्लेषकों ने इसका श्रेय सुधारों के लिए जनता की मांग में कमी को दिया, जिसमें अराजनीतिक जनता उस वास्तविकता को बरकरार रखती है जिसमें राज्य अपने मामलों का संचालन स्वयं करता है.
संविधान बनाम शरिया कानून
क़तर में 2005 से एक संविधान है, लेकिन शरिया कानून अभी भी कानून का मुख्य स्रोत है. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से संविधान अभी भी कमजोर है. यह राजनीतिक दलों के गठन की स्वीकृति नहीं देता है. जैसा कि संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है, साल 2007 से संसद की प्रस्तावित स्थापना पर नए सुधारों की पहल अभी भी ख़ामोश है. ये सुधार कार्यकारी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने जा रहे हैं. अमीर के पास कैबिनेट नियुक्त करने की शक्ति होती है और यही वजह है कि वह एज़ेंडा को नियंत्रित करता है. उसके पास कानूनों को अवरुद्ध करने और लागू करने की शक्ति है और सबसे बढ़कर, वह अपनी इच्छा से शूरा परिषद को भंग कर सकता है.
हाल के सुधार प्रवासी समुदाय, विशेषकर श्रमिकों की दुर्दशा को भी नज़रअंदाज़ करते हैं. हालांकि श्रम कानूनों में समय-समय पर सुधार किए जाते हैं फिर भी प्रवासी श्रमिकों के मूल अधिकारों को बहाल करने में रुचि नहीं दिखती है. जबकि मानव अधिकार संगठनों और नीति प्रहरी के विरोध के बाद भी सैद्धान्तिक तौर पर कफ़ला प्रणाली को 2018 में ही ख़त्म कर दिया गया है.
हाल के सुधार प्रवासी समुदाय, विशेषकर श्रमिकों की दुर्दशा को भी नज़रअंदाज़ करते हैं. हालांकि श्रम कानूनों में समय-समय पर सुधार किए जाते हैं फिर भी प्रवासी श्रमिकों के मूल अधिकारों को बहाल करने में रुचि नहीं दिखती है. जबकि मानव अधिकार संगठनों और नीति प्रहरी के विरोध के बाद भी सैद्धान्तिक तौर पर कफ़ला प्रणाली को 2018 में ही ख़त्म कर दिया गया है. लेकिन भगोड़ों के लिए अभी भी सख़्त पेनाल्टी मौजूद है और श्रम सुधार के जरिए अब तक भगोड़ों को गैर अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जा सका है. यह व्यवस्था अभी तक कायम है और मुल्क में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के शोषण और अत्याचार की वजह बनते हैं. हाल के सुधार श्रम अधिकारों को लेकर भी ज़्यादा कुछ संकेत नहीं देते इसलिए उनकी सफ़लता के आसपास निराशावाद का माहौल है. प्रवासी अधिकारों के प्रोजेक्ट की निदेशक, वाणी सरस्वती का तर्क है कि इस दिशा में सुधारों से कुछ ख़ास बदलाव नहीं आया है क्योंकि इनसे मज़बूरी में किए जा रहे श्रम को अधिक मज़बूत बनाता है.
इन सुधारों को उन चुनौतियों के बीच लागू किया गया था, जबकि क़तर नागरिक स्वतंत्रता, श्रम भेदभाव और जनजातीय संवेदनशीलता के ख़राब रिकॉर्ड से जूझ रहा था. कतर में एक बड़े प्रवासी समुदाय और एक आयातित श्रम बल की मौजूदगी राज्य की जनसांख्यिकी को चुनौती दे रही है. यह सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर तनाव पैदा कर रहा है. नागरिकों का छोटा अल्पसंख्यक समूह जो ज़्यादातर ‘मूल कतर के नागरिकों’ का प्रतिनिधित्व करता है, वह अभी भी राष्ट्र के संस्थानों को नियंत्रित करता है, जिसमें सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और नौकरशाही शामिल हैं. अन्य देशों की तुलना में बड़ी संख्या में श्रम संसाधन के बावजूद यहां कोई राजनीतिक दल और कोई ट्रेड यूनियन नहीं है.
निष्कर्ष
अगर राजनीतिक दल गैर-कानूनी हों तो राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया रुकी हुई ही रहेगी. कतर में भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून को देखते हुए राजनीतिक भागीदारी एक कल्पना जैसी ही प्रतीत होती है. इन सुधारों का मकसद ज़्यादा लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यह एक स्वार्थ से प्रेरित सत्तावादी व्यवस्था है जो दुनिया के बाकी हिस्सों से किसी भी आलोचना को दूर रखने में मदद करती है. इसलिए वास्तविकता यह है कि कतर में एक व्यवस्था है, जिसमें सरकार मतदाताओं का चुनाव करती है, ना कि मतदाता सरकार का चुनाव करते हैं.
सत्ता में बैठे शासक, क़तर के अंदर और अपनी विदेश नीति में यथास्थिति को लेकर संतुष्ट हैं. लेकिन असली मंशा देश का लोकतंत्रीकरण करना नहीं है, बल्कि लंबे समय से लंबित चुनावी वादे को ख़त्म करना और आलोचना को दूर करने के लिए अपनी छवि बचाने की कोशिश करना है.
क़तर वर्तमान में किसी आंतरिक ख़तरे का सामना नहीं कर रहा है और ना ही उसके पड़ोस से ऐसा कोई ख़तरा पैदा हो रहा है. सत्ता में बैठे शासक, क़तर के अंदर और अपनी विदेश नीति में यथास्थिति को लेकर संतुष्ट हैं. लेकिन असली मंशा देश का लोकतंत्रीकरण करना नहीं है, बल्कि लंबे समय से लंबित चुनावी वादे को ख़त्म करना और आलोचना को दूर करने के लिए अपनी छवि बचाने की कोशिश करना है. इसलिए ये सुधार इस क्षेत्र के लिए एक लोकतांत्रिक मिसाल नहीं बनने जा रहे हैं, जब तक कि सत्ताधारी व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार नहीं हो जाता है और इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन के बिना, कतर केवल प्रगतिवादी राजनीतिक सुधार का अहसास कर पाएगा जो उसके पड़ोसी मुल्कों को प्रभावित करने में नाकाम रहेगी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV