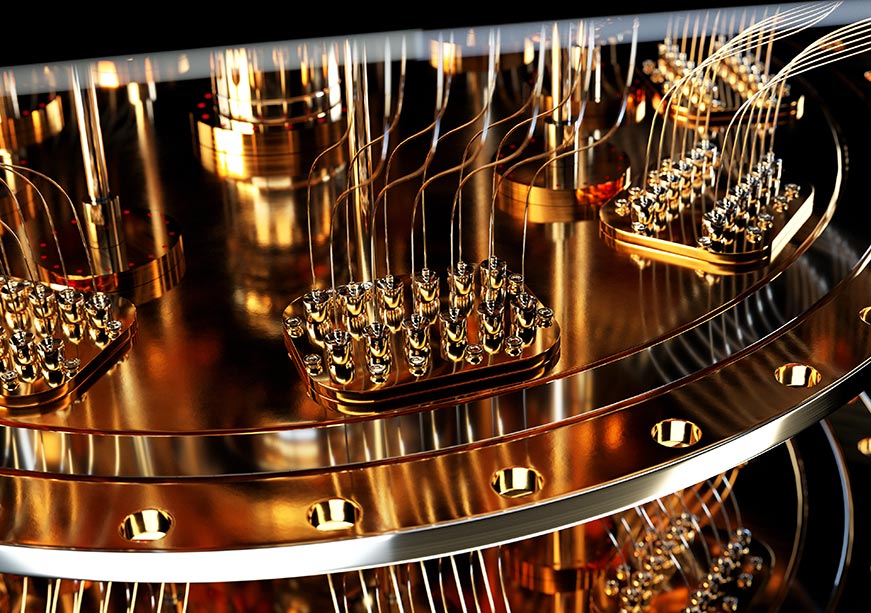Image Source: Getty
जब देशों की आर्थिक हैसियत, ताक़त और दबदबे में बदलाव आता है, तो उनके रिश्तों में भी तब्दीली आती है. ये बदलाव सबसे ज़्यादा बड़ी ताक़तों के साथ रिश्तों में आने वाले परिवर्तन के तौर पर नुमायाँ होता है. इसके उलट, जब बड़ी शक्तियां ख़ुद उभरती हुए शक्तियों के साथ अपने रुख़ में बदलाव लाती हैं, तो वो तभी सफल होती हैं, जब वो उभरती हुई शक्तियों का ख़ुद से सम्मान करने के बजाय रियायत देने को मजबूर होती हैं. वैसे तो अमेरिका पिछले तीन चौथाई सदी से विकास, प्रभाव क्षेत्र और अपनी हार्ड और सॉफ्ट पावर की सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है. लेकिन, दुनिया की सबसे बड़ी ताक़त के साथ रिश्तों के मामले में दो उभरती हुई ताक़तों चीन और भारत का रवैया एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहा है. पिछले तीन दशकों के दौरान चीन ने विकास की जो रफ़्तार दिखाई है, उसमें सबसे बड़ा हाथ तो ख़ुद अमेरिका का ही रहा है, जिसने दुनिया की सुरक्षा की गारंटी लेने वाले देश के तौर पर चीन को आगे बढ़ाया. लेकिन अब चीन और अमेरिका बुनियादी तौर पर एक दूसरे के साथ ताक़त और दबदबे की होड़ में लगे हैं और हर मोर्चे पर ये मुक़ाबला गंभीर ही होता जा रहा है. इस चलन को तेज़ी देने में तीन बड़े कारणों का योगदान रहा है. पहला, अमेरिका के राजनीतिक और सामाजिक चुनावों और चलन में तेज़ी से आ रहे बदलाव ने अपनी सुरक्षा और दुनिया में अपनी भूमिका को लेकर अमेरिका की सोच को बिल्कुल ही बदल डाला है. दूसरा, आज चीन हर अहम मोर्चे पर अमेरिका की बराबरी करने के बेहद क़रीब पहुच रहा है. ऐसे में अमेरिका अपनी नंबर वन की हैसियत बनाए रखने को बेक़रार है और यही बात दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता को रेखांकित करती है. चीन द्वारा अपनी नौसैनिक ताक़त में किए गए इज़ाफ़े और पूरी दुनिया पर कसते उसके आर्थिक शिकंजे ने वैश्विक स्तर पर ताक़त के समीकरणों के मानकों पर पुनर्विचार को बाध्य किया है. आख़िर में, तकनीक के मोर्चे पर एक नई होड़ तेज़ होती जा रही है और अगले कुछ दशकों के दौरान तकनीक का ये मुक़ाबला ही बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता की दशा दिशा तय करेगा. इस मुक़ाबले ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वो उभरती हुई ताक़तों के साथ समन्वय बढ़ाए और उनको सम्मान दे. कुल मिलाकर इन सभी बातों ने सुरक्षा, शक्ति और प्रभाव को लेकर अमेरिका में उपयोगिता पर ज़ोर देने वाली एक नई सोच को जन्म दिया है. अमेरिका में चल रहे इस पुनर्मूल्यांकन के केंद्र में भारत है.
अमेरिका और भारत के संबंधों पर गहरी नज़र रखने वाले पर्यवेक्षकों को ये उम्मीद थी कि वो द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा आयामों को बढ़ाने पर ज़ोर देने के बजाय भारत के साथ रिश्तों पर एक नई छाप छोड़ेंगे.
भारत-अमेरिका संबंध
जब भारत के प्रधानमंत्री इस साल 13-14 फ़रवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे, तो दोस्ती, यादों, संकेतों और यथार्थवाद की एक मिली जुली तस्वीर उभरकर सामने आई. अमेरिका और भारत के संबंधों पर गहरी नज़र रखने वाले पर्यवेक्षकों को ये उम्मीद थी कि वो द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा आयामों को बढ़ाने पर ज़ोर देने के बजाय भारत के साथ रिश्तों पर एक नई छाप छोड़ेंगे. मोदी के बमुश्किल 40 घंटे के अमेरिका दौरे में भारत और अमेरिका के बीच एक नए क़रार (COMPACT यानी कैटालाइजिंग अपॉर्च्यूनिटीज फ़ॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलेरेटेड कॉमर्स ऐंड टेक्नोलॉजी) पर सहमति बनी. इस समझौते का मक़सद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और आविष्कार, आम लोगों के बीच संवाद और बहुपक्षीय सहयोग के लिए तालमेल बढ़ाने के एक नए व्यापक ढांचे को खड़ा करना था.
पिछले दो दशकों से भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध 2005 में हुए फ्रेमवर्क फ़ॉर दि यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप के आधार पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे. इस फ्रेमवर्क में ‘अमेरिका और भारत को तेज़ी से व्यापक, जटिल और सामरिक सहयोग’ की दिशा में आगे बढ़ाने का वादा किया गया था. इसके बाद 2015 में नई रूपरेखा पर दस्तख़त किए गए, जिसने ‘उच्च स्तरीय सामरिक संवाद के मौक़े मुहैया कराने, दोनों देशों के बीच नियमित रूप से तालमेल करने और रक्षा क्षमताओं को मज़बूत बनाने’ का ढांचा उपलब्ध कराया. इस रूप-रेखा को जो हालिया विस्तार दिया गया है, वो भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में आ रहे विस्तार को दिखाता है, ख़ास तौर से संवेदनशील तकनीक देने के मामले में सहयोग और सामरिक रूप से भरोसा करने के मामले में. इस साल जब 2015 में हुए समझौते की अवधि ख़त्म हो रही है, तो भारत और अमेरिका ने 21वीं सदी के लिए ‘भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख रक्षा साझेदारी’ के रूप में अगले दस साल के लिए एक नई रूप-रेखा पर दस्तख़त करने को लेकर सहमति बनी है. अहम बात ये है कि सहयोग की इस नई रूपरेखा में भारत के प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP) की हैसियत को भी शामिल किया गया है, ताकि नई तकनीक तक उसको पहुंच और रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति की गारंटी को भी अगले एक दशक के दौरान लगातार चलने वाली प्रक्रिया बनाया जा सके.
2005 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के जिस मार्ग को खोला गया था, उस पर आगे बढ़ने के लिए हर दस साल में नवीनीकरण की ज़रूरत होती है, ताकि नई प्राथमिकताओं को जगह दी जा सके. इसके ताज़ा स्वरूप में आपसी रक्षा संबंधों के केंद्र में रक्षा औद्योगिक सहयोग, मिलकर उत्पादन करने और एक दूसरे के साथ मिलकर संचालन को बढ़ाने को रखा गया है. भारत की रक्षा ज़रूरतों की आपूर्ति में तेज़ी लाने के लिए जिन प्रमुख योजनाओं पर रज़ामंदी बनी है, उसके तहत भारत और अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो नए हथियारों की ख़रीद को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे. इसके साथ साथ दोनों देश अमेरिका के ‘जैवलिन’ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस साल से भारत में संयुक्त रूप से उत्पादन शुरू करेंगे. इसके अलावा भारत द्वारा छह नए P-8I समुद्री गश्ती विमान ख़रीदने से भी व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षेत्र की गुप्तचरी, निगरानी और सतर्कता बरतने (ISR की क्षमताओं में इज़ाफ़ा होगा.
भारत-अमेरिका सुरक्षा संबंध
ट्रंप के दूसरे प्रशासन ने साफ़ तौर पर भारत के साथ रक्षा संबंधों के मामले में दूरगामी नज़रिया अपनाया है, जिसके तहत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में गहरे संरचनात्मक बदलाव लाकर आपसी सुरक्षा संबंधों को और एकीकृत करने पर योजनाबद्ध तरीक़े से काम किया जाएगा. भारत के प्रमुख रक्षा साझीदार (MDP) के दर्जे का व्यापक रूप से दोहन करने के लिए स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑदराइज़ेशन-1 (STA-1) का इस्तेमाल किया जाएगा; हथियारों और उपकरणों की द्विपक्षीय ख़रीद को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादों और सेवाओं की दोनों तरफ़ से आपूर्ति की एक सुगम व्यवस्था बनाने के लिए रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट (RDP) के लिए बातचीत शुरू की जाएगी, और हथियार देने के नियमों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेग्यूलेशन (ITAR) भी शामिल है. इन सब क़दमों का एक ही मक़सद है कि दोनों देशों के रक्षा इकोसिस्टम एक दूसरे के क़रीब आएं, दोनों देशों की सेनाएं और हथियार एक दूसरे के द्वारा इस्तेमाल हो सकें और रक्षा उपकरणों का मिलकर उत्पादन किया जा सके.
पिछले पांच वर्षों के दौरान युद्ध क्षेत्र और जंग के मैदान से बाहर मिले सबक़ों को देखते हुए मोदी और ट्रंप के लिए अगले एक दशक का रोडमैप पेश करना आवश्यक था. युद्ध और सुरक्षा के मामले में स्वचालित उपकरणों की अहमियत ऐसा ही एक क्षेत्र है. भारत और अमेरिका ने ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री एलायंस (ASIA) के नाम से एक नए गठबंधन का ऐलान किया. ये नया क़दम हिंद प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी और उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है. भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच समुद्री औज़ारों और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस मानवरहित हवाई उपकरणों (UAS) का मिलकर उत्पादन करने की साझेदारी, प्रतिद्वंदियों से मुक़ाबला करने और उन पर दबाव बनाने के लिहाज़ से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है.
युद्ध और सुरक्षा के मामले में स्वचालित उपकरणों की अहमियत ऐसा ही एक क्षेत्र है. भारत और अमेरिका ने ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री एलायंस (ASIA) के नाम से एक नए गठबंधन का ऐलान किया.
शायद सबसे अहम बात तो ये है कि भारत और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के सैन्य बलों की तैनाती और उनको बनाए रखने में मदद करने के इरादे का ऐलान करने सहयोग के नए क्षेत्र के द्वार खोले हैं. ये इस इलाक़े की संयुक्त सुरक्षा के लिए एक अहम सामूहिक वादा है. इन तैनातियों से हिंद प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत और अमेरिका के रुख़ में नया बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके लिए दोनों देश लॉजिस्टिक्स, गोपनीय जानकारियों को साझा करने, संयुक्त रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत के मिशन चलाने और सबसे अहम बात खाड़ी क्षेत्र से लेकर सुदूर पूर्व तक साझा ख़तरों का मुक़ाबला करने में सहयोग बढ़ाया जाएगा.
दोनों देशों के बीच, इसके अलावा भी तकनीक, आविष्कार, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष और आम जनता के बीच संवाद बढ़ाने के मामलों में कई नई घोषणाएं की गईं. ये सब एलान भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा के नए क़रार को ही मज़बूती देने वाले हैं. हालांकि, भारत और अमेरिका के आपसी संबंध और उनके बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के तीन प्रमुख ट्रेंड साझा बयान में एकदम अलग से दिखे. हिंद महासागर, भारत और अमेरिका के सहयोग का प्रमुख क्षेत्र होगा. दोनों देशों ने इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिक वेंचर का एलान किया, जो आर्थिक कनेक्टिविटी और कॉमर्स के क्षेत्र में आपसी तालमेल से निवेश बढ़ाने का एक द्विपक्षीय क़दम है. इसके अलावा मेटा की समुद्र के भीतर 50 हज़ार किलोमीटर लंबी केबल बिछाने की महत्वाकांक्षी परियोजना, ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय सुरक्षा को जोड़ने को लेकर दूरगामी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं. दूसरा, मोदी के अमेरिका दौरे ने ये दिखाया कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रूप-रेखा की अहमियत को लेकर प्रतिबद्धता मज़बूत बनी हुई है. और आख़िर में दोनों देशों के बीच इस नए क़रार में सहमति का एक और बिंदु कनेक्टिविटी की परियोजनाओं का है. भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक के लिए आर्थिक गलियारा (IMEC) बनाने का मक़सद कई क्षेत्रों से होकर गुज़रने वाली कनेक्टिविटी की अगली परियोजना है, जो ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नए रास्ते पर ले जा सकती हैं. हालांकि, इसकी सफलता मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक हालात पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं.
भले ही ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये आशंका जताई जा रही है कि वो वैश्विक सुरक्षा की ज़िम्मेदारियों से अमेरिका को पीछे खींच सकते हैं. लेकिन, हिंद प्रशांत की सुरक्षा और चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौती अमेरिका की प्रमुख वरीयता बनी हुई है और चीन के साथ उसकी सामरिक प्रतिद्वंदिता आगे भी जारी रहेगी.
निष्कर्ष
म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस में भाषण देते हुए अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जे डी वैंस ने ज़ोर देकर ये कहा था कि अमेरिका, यूरोप से ये अपेक्षा करता है कि वो सुरक्षा की ज़िम्मेदारी का बोझ और अधिक उठाए, जिससे अमेरिका को दूसरे अहम क्षेत्रों पर ध्यान देने का मौक़ा मिल सके. वैंस की बातों में जो संदेश था, वो बिल्कुल स्पष्ट है: भले ही ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये आशंका जताई जा रही है कि वो वैश्विक सुरक्षा की ज़िम्मेदारियों से अमेरिका को पीछे खींच सकते हैं. लेकिन, हिंद प्रशांत की सुरक्षा और चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौती अमेरिका की प्रमुख वरीयता बनी हुई है और चीन के साथ उसकी सामरिक प्रतिद्वंदिता आगे भी जारी रहेगी. आत्मविश्वास से भरा ट्रंप प्रशासन, वैश्विक मंच पर अमेरिका की भूमिका को नए सिरे से ढाल तो रहा है. लेकिन, अपने सामरिक मक़सदों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका, भारत को अपने एक प्रमुख साझीदार के तौर पर देखता है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




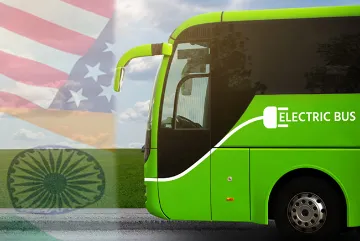

 PREV
PREV