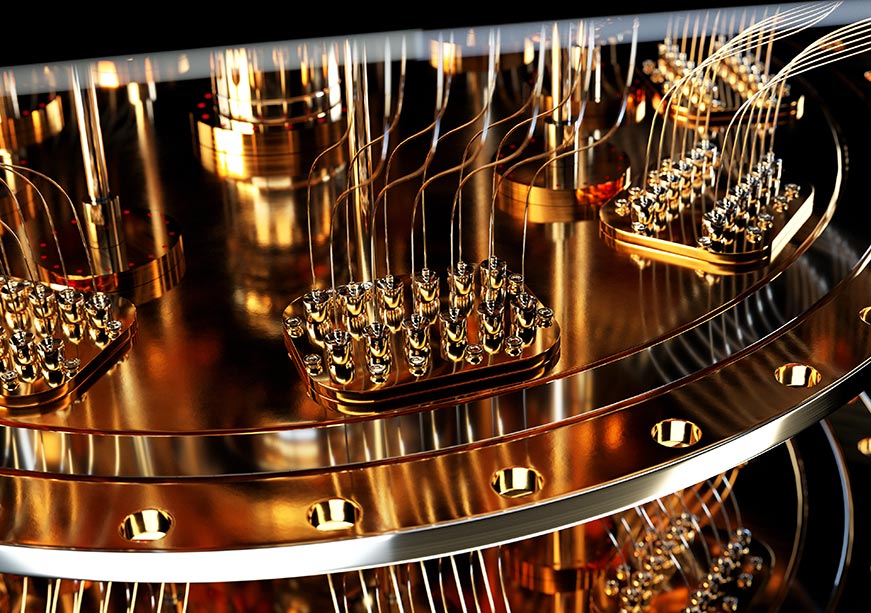जलवायु परिवर्तन के असर के मुताबिक़ ख़ुद को ढालना अब विकल्प नहीं एक ज़रूरत बन गया है, जिससे हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकें. जलवायु संबंधी सभी भयंकर घटनाओं में, भयंकर गर्मी जैसे कि लू चलना, एशिया में तेज़ गति से बढ़ रहा है, जिससे करोड़ों लोगों की जान जोख़िम में पड़ जाती है.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि मई के अंत तक पूरे भारत में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगा. इसके अतिरिक्त ये पूर्वानुमान भी जताया गया है कि भारत के कई हिस्सों जैसे कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में सामान्य से कहीं ज़्यादा भयानक लू चलेगी.
पिछले साल मार्च में पांच दशकों की सबसे भयंकर लू चलने के बाद, 2023 में भी भारत में भयंकर गर्मी का ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है. हालांकि, 2023 के मार्च महीने की शुरुआत मुंबई जैसे शहरों में तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने के कारण भयंकर गर्मी की चेतावनी के साथ शुरू हुआ था. लेकिन, अनपेक्षित चक्रवातीय हवाओं और पश्चिमी विक्षोभों के कारण, भारत के कई इलाक़ों में बेमौसम बरसात और ओले पड़ने की घटनाएं हुईं, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आ गई. मार्च महीने में मध्य भारत में लंबी अवधि के दौरान (LPA) बारिश के औसत से ज़्यादा बरसात हुई थी, जबकि दक्षिणी भारत में ये 100 प्रतिशत को भी पार कर गई. इसके अलावा, मौसम विभाग ने भी अपने गर्मी के मौसम की भविष्यवाणी को नया करते हुए एक अप्रैल को एक सार्वजनिक बुलेटिन जारी किया कि गर्मी के हालात और भी ख़राब होने वाला हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि मई के अंत तक पूरे भारत में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगा. इसके अतिरिक्त ये पूर्वानुमान भी जताया गया है कि भारत के कई हिस्सों जैसे कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में सामान्य से कहीं ज़्यादा भयानक लू चलेगी. हमारे शहर भयंकर गर्मी के इस चक्रवात के केंद्र में होंगे, क्योंकि हर साल ग्रामीण इलाक़ों के करोड़ों लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं. ऐसे में शहर, जलवायु परिवर्तन की शिकार आबादी के गढ़ बनते जा रहे हैं. अब जलवायु परिवर्तन के जोख़िम कम करने और भविष्य में बुरी से बुरी परिस्थितियों के मुताबिक़ ख़ुद को ढालने के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार लचीले शहरों और क़स्बों का निर्माण अति आवश्यक हो गया है.
झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, तुलनात्मक रूप से भयंकर गर्मी के सबसे ज़्यादा शिकार हुए थे. बड़ा सवाल ये है कि क्या हम गर्मी की वो भयंकर मार झेलने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं, जो हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और भविष्य में और भी ज़्यादा क़हर ढाने वाली है?
वैसे तो, लू चलने या हीटवेव की सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की गई कोई परिभाषा नहीं है. लेकिन विश्व मौसम संगठन लू की परिभाषा इस तरह बताता है: ‘पांच या इससे ज़्यादा दिन जब अधिकतम तापमान, औसत से पांच डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा हो.’ वहीं, भारत में लू चलने की परिभाषाकुछ इस तरह है, ‘मैदानी क्षेत्र के किन्हीं दो मौसम विज्ञान केंद्रों में कम से कम दो दिनों तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो, और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो.’ भयंकर हीटवेव की चेतावनी तब जारी की जाती है, जब अधिकतम तापमान औसत से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो या फिर 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो. भारत के मौसम विभाग के क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ऐंड हज़ार्ड एटलस 2021 के मुताबिक़, 1969 से 2019 के दौरान भारत ने हर साल तबाही लाने वाली भयंकर गर्मी के औसतन 130 दिनों का सामना किया है. इसके अतिरिक्त, मध्य और उत्तरी पश्चिमी भारत में लू चलने की अवधि पांच दिन बढ़ गई है. वैसे तो भारतीय उप-महाद्वीप में लोगों को लू का सामना करने का लंबा अनुभव है. लेकिन मौजूदा जलवायु संकट इन तजुर्बे को और अभूतपूर्व ढंग से भयावाह बना रहा है. अध्ययनों के मुताबिक़, सन् 2100 तक सबसे बुरे हालात (RCP 8.5) में गर्मियों के दिनों (अप्रैल से जून के बीच) में लू चलने की घटनाएं तीन से चार गुना बढ़ जाएंगी. वहीं, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि औसत भयंकर गर्मी वाले दिनों की अवधि दो गुना बढ़ जाएगी.
शहरी क्षेत्रों में लू के शिकार होने की बढ़ती कमज़ोरी
ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाक़े लू चलने से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं. शहरों में हीटवेव के दुष्प्रभाव कई क्षेत्रों में नुमायां हो रहे हैं. जैसे कि इंसानों की सेहत, आर्थिक गतिविधियां, पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों की मांग में वृद्धि और जैव विविधता में कमी. 21वीं सदी के दूसरे दशक के दौरान भारत में भयंकर मौसम की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है. इनमें वर्ष 2015 में हैदराबाद, दिल्ली, प्रयागराज और भुबनेश्वर में भयंकर लू चलने की घटनाएं शामिल हैं. पश्चिमी राज्य राजस्थान के छोटे से क़स्बे चूरू में 2016 में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. वहीं, लंबे समय तक पड़े सूखे और भयंकर गर्मी के कारण 2018 में चेन्नई को पानी के संकट का सामना करना पड़ा था. 2022 में दिल्ली, रायपुर, हैदराबाद, मुंबई और दूसरे शहरी इलाक़ों में भयंकर गर्मी के दुष्प्रभाव देखने को मिले थे. झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, तुलनात्मक रूप से भयंकर गर्मी के सबसे ज़्यादा शिकार हुए थे. बड़ा सवाल ये है कि क्या हम गर्मी की वो भयंकर मार झेलने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं, जो हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और भविष्य में और भी ज़्यादा क़हर ढाने वाली है? भारत के शहरी इलाक़ों को वो कौन से क़दम उठाने चाहिए, जिससे पूरे इको-सिस्टम पर भयंकर गर्मी के नकारात्मक असर को कम किया जा सके और कारोबारी मूल्य संवर्धित श्रृंखला को सुरक्षित बनाया जा सके?
भयंकर गर्मी वाले मौसम से निपटने के लिए प्रकृति ने हमेशा ही इंसानों को उपाय उपलब्ध कराए हैं. शहरों में गर्मी पर क़ाबू पाने के लिए पानी और पेड़ों का एक साथ इस्तेमाल ज़रूरी है. जानलेवा तापमान के अनुसार ख़ुद को ढालने के लिए शहरों में किए जा रहे उपायों को, प्रकृति पर आधारित समाधानों (NbS) से मज़बूती दी जा सकती है. इन्हें इको-सिस्टम आधारित उपाय भी कहते हैं. प्रकृति पर आधारित समाधान न केवल हरित मूलभूत ढांचे को सहयोग देते हैं, जो शहरी लचीलेपन को सुधारने के लिए ज़रूरी है. बल्कि, इनसे कई अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी लाभ भी प्राप्त होंगे. क़ुदरत पर आधारित समाधानों के अपनाने के लिए शहरों की योजना बनाने, नीतियां तैयार करने और मूलभूत ढांचा एवं हरित पट्टियां बनाने के तौर तरीक़ों में संस्थागत बदलाव लाना होगा. भारत के शहरी इलाक़ों में दम घोंटने वाली गर्मी का मुक़ाबला करने और प्राकृतिक रूप से इन चुनौतियों से निपटने के लिए तीन नज़रियों की आवश्यकता होगा.
- शहरी हरित क्षेत्रों के दायरे को बढ़ाना: शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (NIUA) की ताज़ा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ रेडीनेस रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत के कुल 126 शहरों में से 65 शहरों को URDPFI के नियमों का पालन करने के लिए अपने नगर निगमों के दायरे में आने वाले हरित क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी. इसकी तुलना में भारत का कोई भी शहर ऐसा नहीं है, जो प्रति व्यक्ति 9 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक को पूरा करता हो. शहरों में ज़मीन की बढ़ती मांग के चलते, उनके हरित क्षेत्र लगातार सिमटते जा रहे हैं. इसका नतीजा ये हुआ है कि शहरों में गर्मी से राहत देने वाले इलाक़े कम हो रहे हैं और भयंकर गर्मी वाले क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं. इसीलिए, ज़रूरी है कि रास्तों में पेड़ लगाने, छतों और दीवारों पर पौधे लगाने, शहरी जंगलों का विस्तार करने, आपन में जुड़े हरित गलियारे तैयार करने, योजनाओं के दायरे में हरित पट्टियां बनाने और दूसरे कई उपायों के ज़रिए मौजूदा हरित क्षेत्रों का रख-रखाव करने के साथ साथ शहरों के हरित क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी की जाए. इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी स्ट्रैटेजी ऐंड एक्शन प्लान (LBSAP) और हर शहर में मौजूद पेड़ों की गिनती करने से स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर उगने वाले पेड़ों की प्रजातियों को बढ़ावा मिलेगा.
- शहरी योजना निर्माण में प्रकृति आधारित समाधानों का समावेश करना: किसी शहर का विकास कैसे होना चाहिए, इसकी नीति निर्धारित करने वाले दस्तावेज़ों में, जहां मूलभूत ढांचे की ज़रूरत है, वहां ये बात भी स्पष्ट की जानी चाहिए कि ज़मीन का इस्तेमाल कैसे हो और अपेक्षित मांग को कैसे पूरा किया जाए. इन्हें मास्टर प्लान या विकास की योजना कहते हैं. हालांकि, मास्टर प्लान में शहरी पर्यावरण और प्राकृतिक क्षेत्रों की समझ बहुत ख़राब है और इनकी ऐतिहासिक रूप से अनदेखी की जाती रही है. ग्रीनफील्ड मुहल्लों और बस्तियों में हरित क्षेत्र का उच्च अनुपात बनाए रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उन मॉडल बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग बाय-लॉज़ संशोधन करके उन गतिविधियों को भी सीमित किया जाए, जिनकी इजाज़त मनोरंजन के लिए तय इलाक़ों में होती है. लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए ज़रूरी है कि आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, इस बात पर सख़्ती से नज़र रखी जाए कि मन बहलाव के लिए निर्धारित ज़मीन के किसी अन्य प्रयोग में बदलाव न हो. इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीरें और रिमोट सेंसिंग के औज़ार इस्तेमाल करते हुए वास्तविक समय में हरित क्षेत्र की निगरानी की जानी चाहिए. योजना बनाने वालों का सिर्फ़ यही मान लेना पर्याप्त नहीं होगा कि प्रकृति आधारित समाधान भी एक विकल्प हैं. उन्हें इन (NbS) समाधानों को सही संदर्भ के आधार पर मास्टर प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे ग़लत बदलाव की कोई गुंजाइश न हो. इसके अतिरिक्त हाई फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) देने से शहरी क्षेत्रों में हरियाली के अधिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है. इसके अलावा, शहरों के इर्द गिर्द के हरित क्षेत्र (इनमें खेती वाली ज़मीन शामिल है) को दूसरी तरह के भूमि प्रयोग में बदलने और शहरी हरित क्षेत्र के लगातार विस्तार से समय के साथ हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और शहरी इलाक़ों में बनने वाले भयंकर गर्मी के क्षेत्रों के नकारात्मक असर में भी कमी आएगी.
- शहरी वित्त और प्रशासन की नई रूप-रेखाओं का इस्तेमाल करके प्रकृति आधारित समाधानों (NbS) को बढ़ावा देना: 74वें संशोधन क़ानून ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को भारत में शहरी पर्यावरण के प्रबंधन में काफ़ी स्वायत्तता दी है. लेकिन, मूलभूत ढांचे के विकास के लिए फंड की व्यवस्था के पर्याप्त इंतज़ाम नहीं किए गए हैं. इसीलिए, संप्रभु हरित बॉन्ड, मिली-जुली पूंजी, स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी जैसे पूंजी जुटाने के दूसरे उपाय भी आज़माए जाने चाहिए. इसके अतिरिक्त शहरों में प्रकृति आधारित समाधानों के असरदार प्रशासन के लिए विभागों और वार्डों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी, जिससे वो हर स्तर पर समुदायों को शामिल करें और आपस में अच्छी जानकारी और उपायों को साझा कर सकें. हर शहर में पर्यावरण समितियों/ जलवायु प्रकोष्ठों के गठन से जलवायु परिवर्तन को सह सकने वाली योजना बनाई जा सकेगी. इसके अलावा भविष्य में लू चलने के बुरे प्रभावों से निपटने और शहरों में इनके लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए आदर्श यही होगा कि अमेरिका के मयामी शहर की तरह भारत में भी दस लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में चीफ हीट ऑफ़िसर नियुक्त किया जाए. इसके रहन-सहन में बदलाव लाकर अतिरिक्त, ‘LiFE’ पहल को शहरी माहौल की मुख्यधारा में लाने से लंबी अवधि में शहरी मूलभूत ढांचे की मांग में कमी लाई जा सकेगी. इसीलिए, शहरों को तेज़ी से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए वक्त की मांग यही है कि विविधता भरे वित्तीय सहयोग के साथ प्रशासन की एक व्यापक रूप-रेखा तैयार की जाए.
भारत के शहरों में भयंकर लू चलने की ख़ामोश तबाही की भयावाहता, अवधि और संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. ऐसे में ये ज़रूरी है कि शहरों के प्रबंधन, उनकी योजना बनाने और निर्माण के तरीक़ों पर पुनर्विचार किया जाए.
भारत के शहरों में भयंकर लू चलने की ख़ामोश तबाही की भयावाहता, अवधि और संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. ऐसे में ये ज़रूरी है कि शहरों के प्रबंधन, उनकी योजना बनाने और निर्माण के तरीक़ों पर पुनर्विचार किया जाए. इसीलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, शहरी परिवेश में प्रकृति को पुनर्परिभाषित करने और हमारी पृथ्वी में भारी निवेश करने से जलवायु परिवर्तन के प्रति ख़ुद को ढालने, दुष्प्रभाव कम करने और सहने की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.






 PREV
PREV