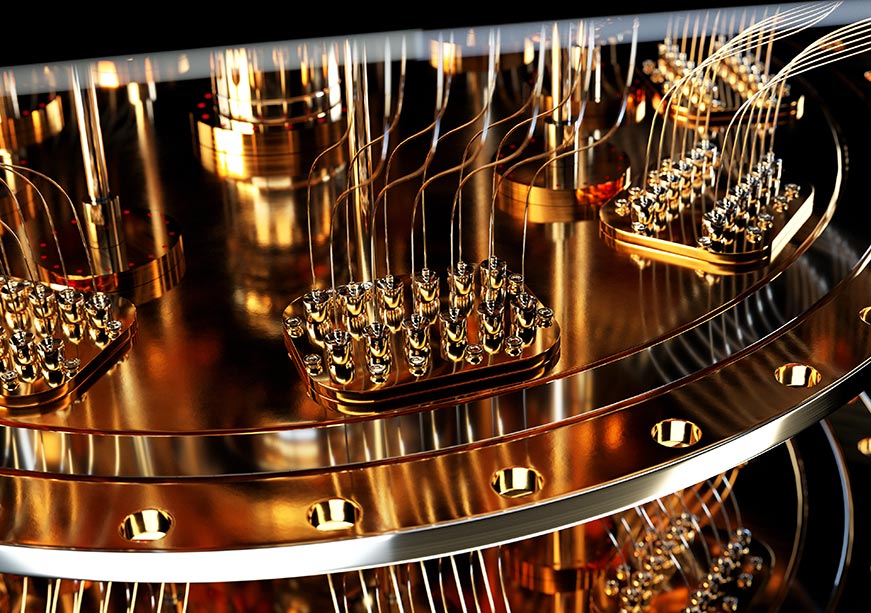दुनिया भर में लगभग पिछले पांच दशकों में पानी के प्रबंधन और इस पर नियंत्रण को लेकर लोगों की धारणाओं एवं विश्वासों में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है. इस बदलाव को आसान शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पहले पारंपरिक तौर पर सोचा जाता था कि पानी एक ऐसा संसाधन है, जिसका उपयोग इंसानों के उपभोग के लिए किया जाता है, लेकिन अब यह सोच बदल चुकी है और अब समग्रता के साथ यह कहा जाने लगा है कि जल प्रबंधन में पारिस्थितिक तंत्र और समाज दोनों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है. यह नए तरह का परिवर्तन जो अभी सामने आ रहा है, साथ ही नई जानकारी और ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हुए एकजुट होकर एक नया आकार ले रहा है, उसे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के सिद्धांतों द्वारा बेहतरीन तरीक़े से वर्णित किया गया है. इस नई सोच के तहत उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट हैं: भोजन और बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के लिए पानी को सुरक्षित करना, पारिस्थितिक तंत्र के लिए पानी को सुनिश्चित करना और विभिन्न सामाजिक ज़रूरतों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना. SDG 6 बेहद स्पष्ट तरीक़े से अपने तमाम प्रकार के लक्ष्यों जैसे कि पीने योग्य पानी प्राप्त करना, स्वच्छता और सफाई प्रदान करना, पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, अपशिष्ट जल का उपचार करना और उसका दोबारा उपयोग करना, पाने के उपयोग की क्षमता में सुधार करना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और पानी से संबंधित इकोसिस्टम की सुरक्षा करने के साथ ही IWRM को भी एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है. यह बेहद दिलचस्प है कि ये जितने भी लक्ष्य हैं, वे IWRM द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के फ्रेमवर्क पर निर्भर हैं. IWRM के सिद्धांतों को निम्नलिखित शीर्षों के तहत स्वीकार करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि मानव ज़रूरतें, पारिस्थितिक आवश्यकताएं, सहकारी सूझबूझ एवं प्रबंधन, बहु-हितधारक संलग्नता और क़ानूनी एवं संस्थागत बचाव.
पहले पारंपरिक तौर पर सोचा जाता था कि पानी एक ऐसा संसाधन है, जिसका उपयोग इंसानों के उपभोग के लिए किया जाता है, लेकिन अब यह सोच बदल चुकी है और अब समग्रता के साथ यह कहा जाने लगा है कि जल प्रबंधन में पारिस्थितिक तंत्र और समाज दोनों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है.
पानी की आपूर्ति बढ़ाने वाले एक पारंपरिक निर्माणवादी इंजीनियरिंग के मॉडल से IWRM में हुआ यह परिवर्तन विवादों से अछूता नहीं है. विभिन्न प्रकार की परस्पर विरोधी कल्पनाओं और अवधारणाओं के आधार पर IWRM के विचार को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में परिकल्पित किया गया है:
a) पानी सिर्फ़ मानव उपयोग के लिए संग्रहित किए जाने वाले भौतिक संसाधनों का भंडार नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वैश्विक जल विज्ञान संबंधी चक्र का एक अभिन्न अंग है: आर्थिक मकसदों के लिए किए जाने वाले जल के भंडारण, परिवर्तन और पानी के उपयोग के लिए व्यापक स्तर पर इंजीनियरिंग निर्माण करने से छोटी अवधि के लिए फायदा होता है, लेकिन इस सबका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और इस इकोसिस्टम पर निर्भर मानव समुदाय पर बड़े पैमाने पर नकारात्मक असर पड़ता है. इसके उलट, IWRM पानी को विशेष रूप से एक प्रवाह के रूप में मान्यता देता है और पारिस्थितिक तंत्र को बरक़रार रखने में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अहम भूमिका को स्वीकार करता है.
b) आर्थिक प्रगति और पानी की आपूर्ति दोनों मुद्दे भिन्न हैं. ऐसे में जबकि नियोक्लासिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आर्थिक प्रगति को संसाधन की उपलब्धता के साथ जोड़ती है, वहीं IWRM इन दोनों बातों को अलग करता है और आपूर्ति की बढ़ोतरी की तुलना में डिमांड-साइड के प्रबंधन की ओर बदलाव पर ज़ोर देता है.
c) नेचुरल इकोसिस्टम के साथ-साथ पानी की मांग की बहुआयामी प्रकृति को स्वीकार करने की ज़रूरत है. ऐसे में जबकि मानव सामाजिक-अर्थव्यवस्था के भीतर पानी की जो मांग है, उसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा है, इस बीच IWRM का विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ अध्ययन करने का मॉडल पानी की ज़रूरतों को लेकर दो वर्गों की प्रतिस्पर्धा के बीच मौज़ूदा प्राथमिकताओं की दुविधा को संबोधित करता है, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज की प्रथामिकता की बात करता है. उल्लेखनीय है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों की बेहतर समझ के ज़रिए इस दुविधा को दूर कर पानी की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जा सकती है.
d) हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की प्रामाणिकता और समग्रता पर विचार करके जल विज्ञान संबंधी प्रवाह पर आने वाले व्यावधानों का आकलन करने हेतु एक एकीकृत और व्यापक नज़रिए के लिए निष्पक्ष विश्लेषण की ज़रूरत है. नया मॉडल प्राकृतिक और सामाजिक वैज्ञानिकों की विभिन्न विषयों की जानकारी रखने वाली एक टीम के माध्यम से एक अंतर्विषयक नॉलेज बेस के निर्माण पर आधारित है. पानी और उससे जुड़ी पारिस्थितिक आर्थिक प्रणालियां मिलीजुली कड़ियों और अन्य प्रणालियों के साथ पारस्परिक संबंधों के कारण बेहद जटिल हैं। ऐसे में किसी एक विषय से जुड़े ख़ास क्षेत्र से संबंधित कोई भी दृष्टिकोण वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए नाकाफ़ी है.
e) बाढ़ और सूखा "आपदा" नहीं हैं, बल्कि इको-हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अभिन्न अंग हैं.
f) परियोजनाओं के मूल्यांकन और जल संसाधनों के कुशल, न्यायसंगत एवं सतत उपयोग के साथ-साथ प्रदूषण से उनकी गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नए और अधिक समग्र सामाजिक व आर्थिक उपकरण विकसित किए जाने चाहिए. पानी के नए अर्थशास्त्र को निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, जो रेडक्शनिस्ट नियोक्लासिकल आर्थिक सोच से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने वाला हो. सामाजिक, पारिस्थितिक और व्यापक नैतिक चिंताओं को मिलाकर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स को नए उभरते उपकरणों में शामिल करने की आवश्यकता है. इस मॉड्यूल में बाद में इस पर भी चर्चा की गई है.
g) शीर्ष से नीचे तक के पारंपरिक संस्थागत प्रशासन के ढांचे को अधिक अपडेटेड और आधुनिक शासन प्रणालियों से बदलने की आवश्यकता है, जो कि लोकतांत्रिक, सहभागी, न्यायसंगत और स्थाई हों.
एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के उल्लिखित सिद्धांतों को विभिन्न स्तरों पर IWRM को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों के तौर पर भी माना जा सकता है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत अभी भी विकसित हो रहे हैं और किसी भी लिहाज़ से फिलहाल संपूर्ण नहीं हैं. यही वो बात है, जो IWRM को एक उभरती हुई और गतिशील व्यवस्था बनाती है. ज़ाहिर है कि वॉटर गवर्नेंस की चुनौतियां दिन-प्रति-दिन और अधिक पेचीदा होती जा रही हैं, ऐसे में संशोधन, संवर्द्धन, परिवर्तन, उन्मूलन और संयोजन के मुद्दे IWRM के केंद्र में रहे हैं और इन पर समय के अनुसार बदलाव होता रहा है. हालांकि, कुल मिलाकर IWRM में "एकीकरण" को मालिन फाल्कनमार्क द्वारा सबसे अच्छे तरीक़े से परिभाषित किया गया है. उन्होंने IWRM को भूमि, पानी और इकोसिस्टम को एकीकृत करने के सिद्धांत के रूप में वर्णित करते हुए इसे तीन E यानी इक्विटी, इकोनॉमिक एफिशियेंसी और इन्वायरमेंटल स्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला बताया है. इनमें से दो चीज़ें यानी सोशल इक्विटी और आर्थिक दक्षता, मानव पर निर्भर हैं, जबकि एक चीज़ यानी पर्यावरणीय स्थिरिता पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है.
यहां इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक मॉडल के रूप में IWRM किसी कार्य पद्धति से जुड़ी नियमावली को स्थापित करने के लिए नहीं है. यह वॉटर गवर्नेंस के उभरते हुए नियमों और नियंत्रण की एक व्यापक रूपरेखा को चिह्नित करने का काम करता है, जो समय के मुताबिक़ होने वाले बदलावों और नई जानकारियों पर निर्भर होती है.
इसलिए, उपरोक्त विवरणों का संज्ञान लेते हुए इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि IWRM वॉटर गवर्नेंस हेतु विशेष मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है. हालांकि, इसके अपने कई प्रबल आलोचक हैं, जिनमें से मार्क जियोर्डानो और तुषार शाह जैसे कुछ आलोचकों ने तो यहां तक कह दिया है कि "...वैश्विक जल प्रबंधन से संबंधित वार्तालाप में IWRM का मौज़ूदा एकाधिकार आज के दौर की पानी की समस्याओं को लेकर व्यावहारिक समाधानों से जुड़ी वैकल्पिक सोच को बंद कर रहा है.” यहां तक कि कुछ वॉटर प्रोफेशनल्स ने उन मुद्दों के एकीकरण से जुड़ी चिंताओं पर सवाल उठाए हैं, जिन्हें IWRM लाने का इरादा रखता है, जबकि कुछ आलोचक इसके परिचालन पर सवाल उठाते हैं. असित बिस्वास कहते हैं, "...IWRM का कोई निश्चित आकार नहीं है और इसमें बुनियादी मुद्दों को लेकर कोई सहमति नहीं है, जैसे कि किन पहलुओं को एकीकृत किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए. अगर ऐसा होता भी है, तो क्या व्यापक अर्थों में इस प्रकार का एकीकरण संभव है".
जल प्रबंधन एक राजनीतिक प्रक्रिया
ज़्यादातर आलोचकों का यह भी कहना है कि IWRM इस सच्चाई को स्वीकार करने में विफल रहता है कि जल प्रबंधन भी एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रतिस्पर्धा, विवाद और समझौता शामिल होता है. इसके साथ ही यह न केवल बड़े पैमाने पर सामाजिक जटिलताओं, प्रक्रियाओं, संस्थागत संदर्भों, शक्ति समीकरणों को रोकने का काम करता है, बल्कि इन सभी प्रक्रियाओं के परस्पर टकराव को एक मुश्किल सच्चाई बनाने से भी रोकता है. यही वजह है कि आलोचक अपनी बात पर अड़े हुए हैं और तर्क दे रहे हैं कि H2O या पानी का मुद्दा, दरअसल H2O-P3 (पीपुल, पॉलिटिक्स और पावर) का मुद्दा है, इसलिए इसका एकीकरण कभी हो ही नहीं सकता है. देखा जाए तो ये जितनी भी आलोचनाएं हैं, वे अलग-अलग सैद्धांतिक प्रतिमानों की वजह से सामने आने वाली एकदम विरोधाभासी चर्चा-परिचर्चाओं से प्रभावित होती रहती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि इनसे पॉलिसी वर्ल्ड को शायद ही कोई रचनात्मक विकल्प उपलब्ध हो पाता है.
देखा जाए तो यही सबसे बड़ी दिक़्क़त है. यहां इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक मॉडल के रूप में IWRM किसी कार्य पद्धति से जुड़ी नियमावली को स्थापित करने के लिए नहीं है. यह वॉटर गवर्नेंस के उभरते हुए नियमों और नियंत्रण की एक व्यापक रूपरेखा को चिह्नित करने का काम करता है, जो समय के मुताबिक़ होने वाले बदलावों और नई जानकारियों पर निर्भर होती है. यही वजह है कि दुनिया भर के विभिन्न जल नीति से जुड़े दस्तावेज़ IWRM की तरफ से प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत ही अपने नीतिगत दिशानिर्देशों को वर्णित करते हैं. इसे भारत में हाल-फिलहाल में कुछ महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक नीतिगत दस्तावेज़ों, जैसे कि नेशनल वॉटर फ्रेमवर्क बिल 2016 का मसौदा, 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज वॉटर रिफॉर्म्स और नेशनल वॉटर पॉलिसी 2020 का मसौदा जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है. ईयू वॉटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव भी IWRM की अहमियत और केंद्रीयता को स्वीकार करता है. उदाहरण के लिए कुछ अन्य देशों में, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस में वॉटर गवर्नेंस के संदर्भ में सामाजिक और पारिस्थितिकीय चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी जल उपयोगों के बीच मौज़ूदा दुविधाओं को एक एकीकृत फ्रेमवर्क के अंतर्गत बेहतर तरीक़े से समझा जा सकता है. यह सामान्य रूप से जल शासन के लिए और विशेष रूप से नदी घाटियों को लेकर एक प्रणालीगत नज़रिए की भी मांग करता है, जो जगह और समय के साथ अन्य भागों में बदलाव पर प्रतिक्रिया देने वाले हर हिस्से के साथ जुड़े हुए हैं.
जल प्रबंधन को लेकर विभाजित नज़रिए की वजह से विश्व के बड़े हिस्से में पानी से जुड़े विवाद चल रहे हैं. इसको लेकर गंभीरता से सोचने की व इन हालातों को बदलने की ज़रूरत है
इसलिए, एक आदर्श के रूप में IWRM विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारियों को एकीकृत करने और एक मज़बूत नींव तैयार करने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करता है. इसे कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जल-खाद्य-ऊर्जा गठजोड़ या एकीकृत नदी बेसिन गवर्नेंस जैसे ज़्यादातर अन्य दृष्टिकोण IWRM के सिद्धांतों पर आधारित हैं. देखा जाए तो IWRM द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं और दिशानिर्देश सुझाए गए हैं, उन्हें चुनौती देने के लिए शायद ही आज कोई वैकल्पिक फ्रेमवर्क मौज़ूद है. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि IWRM को एक कार्यान्वयन के योग्य योजना या फिर प्रबंधन रणनीति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. ज़ाहिर है कि IWRM नियमों या सिद्धांतों का एक समूह है, जिसके आधार पर माइक्रो-वॉटरशेड से लेकर नदी बेसिन तक विभिन्न स्तरों पर बेहतर प्रबंधन रणनीतियों और शासन व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है. जल प्रबंधन को लेकर विभाजित नज़रिए की वजह से विश्व के बड़े हिस्से में पानी से जुड़े विवाद चल रहे हैं. इसको लेकर गंभीरता से सोचने की व इन हालातों को बदलने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है कि IWRM ने दुनिया को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV