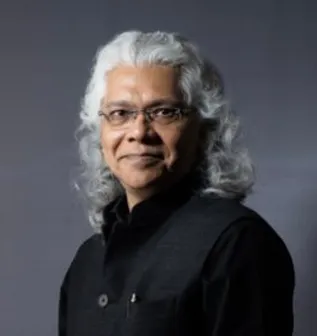31 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संघ (EU) के यूरोपियन सिक्योरिटीज़ ऐंड मार्केट्स अथॉरिटी (ESMA)- जिसकी ज़िम्मेदारी यूरोपीय संघ की वित्तीय व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है- ने भारत के तीसरे देश की छह केंद्रीय समकक्ष संस्थाओं (TC-CCPs) की मान्यता रद्द कर देने का प्रस्ताव रखा. एस्मा (ESMA) का ये आदेश 30 अप्रैल 2023 से लागू होना है. ये आदेश भारत (India) और यूरोपीय संघ (European Union) के मौजूदा आर्थिक संबंधों को चोट पहुंचाने वाला है, और यूरोपीय संघ के इस क़दम को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहा जा सकता है. ESMA ने अपने एक बयान में कहा कि, ‘अर्ज़ियां वापस लेने की आख़िरी मियाद लागू होने तक, ये थर्ड कंट्री सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ (TC-CCPs) यूरोपीय संघ में व्यापार के लिए स्थापित केंद्रों और इसकी मंज़ूरी देने वाले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे.
अगर यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश का कोई निवेशक, भारत में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके निवेश की इजाज़त देने वाले छह भारतीय निगम जो ख़रीद-फ़रोख़्त के बीच का भारत में मिलान करते हैं, उनकी मान्यता रद्द हो चुकी होगी. इससे यूरोपीय संघ के निवेशकों का भारत में निवेश बंद हो जाएगा.
भारत की छह थर्ड कंट्री सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ (TC-CCPs) की मान्यता रद्द करने का ये फ़ैसला, उनकी निगरानी की ज़िम्मेदारी उठाने वाली भारतीय संस्थाओं- क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक; इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSE क्लियरिंग लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के लिए सेबी (सिक्योरिटीज़ ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया); इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन और NSE IFSC क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंट्रल अथॉरिटी (IFSCA) के अधिकारों के ऊपर रोक लगाने जैसा है. दूसरे शब्दों में कहें, तो मान्यता रद्द कर देने का ये फ़ैसला इसलिए किया गया, क्योंकि ESMA और रिज़र्व बैंक, सेबी और IFSCA के बीच ‘आपसी सहयोग के उचित समझौते’ नहीं हुए हैं. यूरोपीय संघ के इस फ़ैसले का उन छह संस्थाओं से कोई मतलब नहीं है, जिनकी मान्यताएं ESMA ने रद्द की हैं.
इसका मतलब ये है कि, अगर यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश का कोई निवेशक, भारत में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके निवेश की इजाज़त देने वाले छह भारतीय निगम जो ख़रीद-फ़रोख़्त के बीच का भारत में मिलान करते हैं, उनकी मान्यता रद्द हो चुकी होगी. इससे यूरोपीय संघ के निवेशकों का भारत में निवेश बंद हो जाएगा.
मान्यता रद्द किए जाने का क़ानूनी अधिकार यूरोपीय संघ के रेग्यूलेशन (EU) नंबर 648/2012 से मिलता है. जिन सटीक प्रावधानों के तहत छह निगमों की मान्यता रद्द की जाएगी, वो अध्याय चार (किसी तीसरे देश से रिश्तों के मामले) की धारा 25 के पैराग्राफ 7 (थर्ड कंट्री सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ CCP) के तहत आते हैं. पैराग्राफ 7 के तहत चार उप प्रावधानों का भी ज़िक्र है. इन के ज़रिए किसी तीसरे देश से आपसी सहयोग की व्यवस्था बनाई जाती है; सुरक्षा में सेंध की जानकारी साझा की जाती है; और आम तौर पर प्रक्रिया संबंधी तालमेल किया जाता है, और ख़ास तौर पर मौक़े पर जाकर निरीक्षण किया जाता है. पैराग्राफ 6 में इन नियमों को किसी तीसरे देश की संस्था द्वारा मानने की बाध्यता का ज़िक्र है.
यूरोपीय संघ के ये नियम G20 के ऊपर हावी हैं. जबकि G20 में बहुपक्षीय वार्ताओं के ज़रिए नियामक व्यवस्थाओं का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है. अब इनके अंदर ओवर द काउंटर (OTC) डेरिवेटिव्स, हेज फंड और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी आती हैं. 26 सितंबर 2009 को पिट्सबर्ग सम्मेलन के बाद G20 देशों के नेताओं ने जो बयान जारी किया था, उसके मुताबिक़, ‘सभी मानक ओटीसी डेरीवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, शेयर बाज़ारों या किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच पर ही किए जाने चाहिए, जहां पर 2012 तक इसके लिए ज़िम्मेदार सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ की उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए.’ इसके अगले साल, 27 जून 2010 को G20 के टोरंटो सम्मेलन की घोषणा ने इस मुद्दे पर और आगे बढ़ने की बात की और कहा कि: ‘हम हेज फंड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और ओवर द काउंटर डेरीवेटिव्ज़ के मामले में पारदर्शिता और नियामक निगरानी बढ़ाने के लिए ठोस उपाय लागू करने की रफ़्तार इस तरह से तेज़ करना चाहते हैं, जो किसी के साथ भेदभाव न करे और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के मुताबिक़ भी हों.
मान्यता रद्द हो जाने का असर क्या होगा?
थर्ड कंट्री सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ज (TC-CCPs) की मान्यता रद्द कर देने का असर सिर्फ़ ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्ज़ पर ही नहीं होने वाला है. भारत के शेयर और बॉन्ड बाज़ार के दरवाज़े भी यूरोपीय संघ के निवेशकों के लिए बंद हो जाएंगे. इससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच पूंजी का प्रवाह तो बाधित होगा. लेकिन, इससे भारत के बाज़ार पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला है. मिसाल के तौर पर, जहां तक शेयर बाज़ार की बात है, तो इस वक़्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निगरानी में जहां 625 अरब डॉलर की संपत्तियां हैं. लेकिन, यूरोपीय संघ के केवल दो ही देश- आयरलैंड और नीदरलैंड्स- ही हैं जो अक्टूबर 2022 में टॉप के दस देशों में शुमार थे; कुल संस्थागत निवेशकों में उनकी साझा हिस्सेदारी सात प्रतिशत से भी कम है.
अगर ये विवाद 30 अप्रैल 2023 तक नहीं सुलझ जाता, तो भारत के ऊपर इसका असर बहुत कम समय के लिए होगा. क्योंकि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के निवेशक, भारत के शेयर बाज़ार में कारोबार नहीं कर पाएंगे. लेकिन, जहां तक स्थायी असर की बात है तो यूरोपीय संघ के निवेशक, दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था से कट जाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया में सबसे अधिक रिटर्न देने वाले बाज़ार तक उनकी पहुंच ख़त्म हो जाएगी.
पूंजी के निर्बाध प्रवाह के चलते बढ़ती पेचीदगियों के चलते नियामक अधिकार क्षेत्र ताक़त की नुमाइश और दबदबा दिखाने का खेल बन चुके हैं. कंपनियां भी कई दशकों से ये तमाशा कर रही हैं और नियामक व्यवस्थाओं को धता बताने की कोशिशें कर रही हैं.
पूंजी के निर्बाध प्रवाह के चलते बढ़ती पेचीदगियों के चलते नियामक अधिकार क्षेत्र ताक़त की नुमाइश और दबदबा दिखाने का खेल बन चुके हैं. कंपनियां भी कई दशकों से ये तमाशा कर रही हैं और नियामक व्यवस्थाओं को धता बताने की कोशिशें कर रही हैं. कंपनियां सबसे अधिक मुनाफ़ा देने वाले अधिकार क्षेत्रों में अपना कारोबार स्थापित करती हैं. सच तो ये है कि जोखिम के प्रबंधन के हथियार के तौर पर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के बोर्ड पहले ही अपना कारोबार अपने लिए मुफ़ीद अधिकार क्षेत्रों में ले जाने की नीतियां तैयार कर रहे होंगे. चाहे वो संस्थाएं हों, बड़ी कंपनियां हों या व्यक्तिगत निवेशक, आज कोई भी भारत की तरक़्क़ी में साझीदार बनने का मौक़ा गंवाना नहीं चाहता है. दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत आज भी निवेश का आकर्षक केंद्र बना हुआ है, और इस दशक के आख़िर तक भारत के ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है, जब वो 2030 से पहले दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.
चीन का ख़तरा और साझा मक़सद तलाशने की कोशिश
कुल मिलाकर ये लड़ाई दो ऐसे पक्षों के बीच में है, जिसमें एक तरफ़ तो नियामक निगरानी के साझा हितों और लोकतांत्रिक संस्थाओं वाले साझा मूल्यों और खुले बाज़ार हैं. वहीं दूसरी तरफ़ यूरोपीय संघ से समर्थन पाने वाले ESMA और भारत के संप्रभु नियामकों रिज़र्व बैंक, सेबी और IFSCA के वित्तीय स्थिरता को लेकर अलग-अलग नज़रिए हैं. ये सीधे-सीधे भू-मंडलीकरण बनाम राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमती उस ताक़त का टकराव है, जो नियम बनाने के अधिकार से जुड़ी है; इस बार भारत को वैश्विक पूंजी से महरूम करने की कोशिश की जा रही है. भारत अब ऐसे खेलों से उकता चुका है.
चूंकि भारत ने, G20 नेताओं के दो बयानों पर दस्तख़त किए हैं. इस लिहाज़ से यूरोपीय संघ के नियमों का पालन होना ही चाहिए. इसी वजह से ESMA बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और भारत को उसी तरह के नियामक निगरानी के अधिकार हासिल करने के लिए संवाद करना चाहिए. एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें यूरोपीय संघ की नियामक संस्थाओं को भारत की नियमन संस्थाओं की निगरानी का अधिकार हो. वहीं भारत को भी यही अधिकार यूरोपीय संघ के नियामक संगठनों पर मिले. ऐसे लेन-देन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति भारत के पास है. अब ऐसे समझौते की बारीकियां तय करने की ही ज़रूरत रह गई है. अब जबकि भारत G20 देशों का अध्यक्ष बनने जा रहा है. तो नियामक संवादों में ये आपसी लेन-देन अब सभी न्यायिक अधिकार क्षेत्रों में लागू होना अनिवार्य किया जाना चाहिए.
यूरोपीय संघ, चीन के जोख़िम की न सिर्फ़ अनदेखी कर रहा है, बल्कि उसे गले लगाने को भी बेताब है. ये चीन के काम करने के तरीक़ों से यूरोपीय संघ के अनजान रहने की हैरान करने वाली हक़ीक़त है. ये इस बात की भी मिसाल है कि यूरोपीय संघ के कुछ नेताओं और संस्थाओं को चीन ने किस तरह अपना बंधक बना रखा है.
इन बातों के अलावा भारत के शेयर बाज़ार दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रशासन की मिसाल हैं. ऐसे में भारत को वित्तीय नियम से बाहर निकालने और उसके बाद पूरे वैश्विक बाज़ार से भारत को अलग थलग करने की तलवार लटकती रहेगी. ये तो उसी तरह है जैसे मिगुएल डे सरवांटेस के उपन्यास, डॉन कहोटी का मुख्य किरदार, जो पवनचक्कियों को दैत्य समझकर उन पर हमला कर देता है. डॉन कहोटी की नज़र में जो हस्ती पवनचक्कियों की थी. वही नज़रिया यूरोपीय संघ के कई अफ़सरों का है. उनकी नज़र में आज का भारत वैसा ही है, जैसा पहले थे. यानी जो पहले था, वही अब है और वही हमेशा बना रहेगा.
ये विडंबना ही है कि यूरोपीय संघ का ज़्यादा बड़ा और वास्तविक रूप से ख़तरनाक दुश्मन तो चीन है. मगर चीन को यूरोपीय संघ ने ख़ुली छूट दे रखी है. चीन की पामच सेंट्रल काउंटरपार्टीज़ हैं, जो पहली पायदान पर हैं (यानी जो ग़ैर संस्थागत रूप से अहम हैं). यानी यूरोपीय संघ ने चीन की संस्थाओं को ठीक वैसा दर्ज़ा दे रखा है, जो अमेरिका, जापान और दुबई की नियामक संस्थाओं को दिया गया है. इन संगठनों में शंघाई क्लियरिंग हाउस, हॉन्ग कॉन्ग सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कंपनी लिमिटेड, HKFE क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओटीसी क्लियरिंग हॉन्ग कॉन्ग लिमिटेड और SEHK ऑप्शंस क्लियरिंग हाउस लिमिटेड हैं. दूसरे दर्ज़े में महज़ एक देश, ब्रिटेन है जिसे संस्थागत रूप से अहम देश का दर्जा दिया गया है.
अपने निवेशकों को चीन के तानाशाह की सनक के हवाले छोड़ना न सिर्फ़ एक पहेली है, जिसे यूरोपीय संघ के निवेशकों को वित्तीय रूप से हल करना है. बल्कि चीन तो यूरोप के लिए सबसे बड़ा संस्थागत जोख़िम है, जिसे मतदाताओं को सियासी तौर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है. चीन द्वारा अपने यहां के उद्यमियों पर की गई कार्रवाई इसकी ताज़ातरीन मिसाल है. इससे भी बुरी बात तो ये है कि हॉन्ग कॉन्ग से क़ाबिल लोगों की भगदड़ मची हुई है. जबकि एक ज़माने में चीन का मुक्त बाज़ार रहा हॉन्ग कॉन्ग एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र की अपनी हैसियत भी गंवा ही रहा है. इन बदलावों के बीच चीन में निवेश करना अनिश्चितता भरा फ़ैसला हो चुका है. अपने आकार और विशाल पैमाने के चलते, चीन के बाज़ार आज व्यापक स्तर के संस्थागत जोख़िम बन चुके हैं. यूरोपीय संघ की अफ़सरशाही को चाहिए कि वो चीन से पैदा होने वाले वित्तीय संकट के इस जोख़िम भरे पहाड़ को लांघ ले. इसके बजाय यूरोपीय संघ के अगुवा लोगों ने भारत की नियामक संस्थाओं पर अपनी निगाह गड़ा दी है, जो यक़ीन से परे की बात है.
यूरोपीय संघ, चीन के जोख़िम की न सिर्फ़ अनदेखी कर रहा है, बल्कि उसे गले लगाने को भी बेताब है. ये चीन के काम करने के तरीक़ों से यूरोपीय संघ के अनजान रहने की हैरान करने वाली हक़ीक़त है. ये इस बात की भी मिसाल है कि यूरोपीय संघ के कुछ नेताओं और संस्थाओं को चीन ने किस तरह अपना बंधक बना रखा है. 30 सितंबर 2020 को यूरोपीय आयोग ने हड़बड़ी में यूरोपीय संघ और चीन के बीच निवेश का व्यापक समझौता कर लिया था. 20 मई 2021 को जाकर यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके इस समझौते को रद्द किया. यूरोपीय संघ को चीन के निर्माण सेक्टर और चीन के बाज़ार का चस्का लगा हुआ है. जो चीन की पूंजी के साथ जुड़कर एक संस्थागत जोख़िम पैदा करते हैं. यूरोपीय संघ को चीन की इस लत से छुटकारा पाने का केंद्र चाहिए और वो ठिकाना भारत है.
इसमें कोई शक नहीं कि नियामक संस्थाओं के टकराव का ये मौजूदा दौर, हमारी कल्पना से भी कम समय में ख़त्म हो जाएगा. यूरोप आज शून्य से लेकर नकारात्मक विकास दर की आशंका झेल रहा है. यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इटली, आर्थिक सुस्ती की ओर बढ़ रहे हैं. ऊर्जा की बढ़ती क़ीमतों के चलते महंगाई की ऊंची दर और बिना विकास के महंगाई की तलवार भी यूरोपीय संघ पर लटक रही है. ऐसे में यूरोपीय संघ को चाहिए कि वो तेज़ी से विकास कर रहे अपने साझीदारों के साथ मिलकर काम करे. ये न केवल आपसी हितों बल्कि आपसी मूल्यों का भी मेल करना होगा. रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोपीय संघ ऊर्जा की भुखमरी का शिकार है. उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है. सियासी तौर पर यूरोपीय संघ अलग थलग पड़ चुका है. वहीं सामरिक रूप से वो अंदरूनी विस्फोट वाला इलाक़ा बन चुका है. इन सबके मिले-जुले नतीजे ख़तरनाक ही होने वाले हैं. यूरोपीय संघ को अगले कुछ महीनों के दौरान मुश्किलों वाली राजनीति का सर्द दौर झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर यूरोपीय संघ, मुक्त व्यापार समझौते के ज़रिए भारत के साथ व्यापक और गहराई भरे रिश्ते चाहता है. जैसा कि हम इस समझौते के लिए चल रही वार्ता के रूप में देख भी रहे हैं, तो यूरोपीय संघ को चाहिए कि वो भारत से अच्छा से अच्छा बर्ताव करे, न कि ख़राब रवैया अपनाए. वित्तीय निगरानी के अधिकार क्षेत्र जैसे बेमतलब के मुद्दों पर भारत की नाराज़गी मोल लेने से उसका भला नहीं होने वाला है.
अगर यूरोपीय संघ, मुक्त व्यापार समझौते के ज़रिए भारत के साथ व्यापक और गहराई भरे रिश्ते चाहता है. जैसा कि हम इस समझौते के लिए चल रही वार्ता के रूप में देख भी रहे हैं, तो यूरोपीय संघ को चाहिए कि वो भारत से अच्छा से अच्छा बर्ताव करे, न कि ख़राब रवैया अपनाए.
लेकिन इस समस्या को वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अवसर के तौर पर भी देखा जा सकता है, और ऐसा होना भी चाहिए. वैश्विक स्तर पर नियमों के आपसी तालमेल और सभी देशों को एक दूसरे की संस्थाओं की निगरानी के बराबरी के अधिकार ही आगे बढ़ने की राह हैं. अगले कुछ महीनों के दौरान भारत को चाहिए कि वो G20 के एजेंडे को सिद्धांतों पर आधारित आपसी अधिकार क्षेत्र वाली वित्तीय नियामक व्यवस्था खड़ी करने की ओर बढ़ाए. इसका मतलब ये है कि अगर यूरोपीय संघ या अमेरिका के नियामक संगठन भारतीय कंपनियों पर नज़र रखने का हक़ चाहते हैं, तो उन्हें भी भारतीय नियामक संस्थाओं को अपने यहां की कंपनियों पर यही अधिकार देना होगा. अगर ICICI बैंक अपने खाते यूरोपीय बैंकिग अथॉरिटी और फेडरल रिज़र्व को दिखा सकता है, तो डॉयचे बैंक और मेरिल लिंच को भी अपना हिसाब किताब रिज़र्व बैंक से कराने को तैयार रहना होगा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV