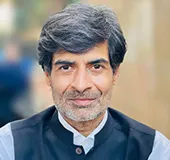अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोक उपयोगी वस्तुएं या सेवाएं मुहैया करवाने या अंतररष्ट्रीय विकास और संवर्धन में सहयोग करने के लिहाज से भारत की भूमिका का आकलन करना हो तो इसके दो तरह के सांचे हो सकते हैं। पहला तो वो है जिसमें पूर्व उपनिवेशों के आजाद होने से शुरू हो कर, 1950 के दशक के दौरान एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के बीच आपसी साझेदारी के लिए बुलाए गए बानडुंग सम्मेलन से होते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन और हाल के दक्षिण—दक्षिण सहयोग (साउथ-साउथ कॉपरेशन) तक एक सतत धारा है। यह मूल रूप से एकता, न्याय, आर्थिक क्षतिपूर्ति और विकास के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही इसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अपने बढ़ते सरप्लस को जी- 77 के मित्रों के बीच साझा करने की हाल के समय में शुरू हुई आकांक्षा भी शामिल है। भारत और इसके विकास के क्षेत्र के विश्लेषकों ने ज्यादातर मामलों में विकासपरक साझेदारी के लिहाज से इसी पैमाने का इस्तेमाल किया है। हाल में गोवा में हुई बिम्सटेक-ब्रिक्स की बैठक भी इसी पर आधारित थी।
भारत की भूमिका को समझने के लिए दूसरा पैमाना ‘उत्थान’ की व्यापक सोच पर आधारित है। यह निरंतरता पर आधारित उपरोक्त विचार से परे जाता है। इसकी बजाय यह भारत (और कुछ अन्य देशों को) एक ऐसे मोड़ पर रखता है, जो एकता और अधिकारों से आगे विकासपरक साझेदारी के एजेंडा में एक विश्व शक्ति के रूप में शामिल होने को अपनी जिम्मेवारी समझता है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय हितों के संदर्भ में इसे नए अवसर मिले हैं तो जिनकी वजह से इसकी नई जिम्मेवारियां भी पैदा हुई हैं। ये विकासपरक साझेदारी को ले कर हमारे प्रयासों की राह तैयार करते हैं। यह रोमांटिसिज्म (प्राकृतवाद) की जगह व्यवहारिकता को तवज्जो देता है और इसलिए इसको ले कर चर्चा भी कम की जाती है। भारत को सावधान रहने की जरूरत है कि यह दुविधा उसके विकासपरक साझेदारी के एजेंडा के दायरे की महत्वाकांक्षा को सिर्फ साउथ-साउथ कॉपरेशन तक सीमित नहीं करती
इसका यह मतलब नहीं है कि साउथ-साउथ कॉपरेशन महत्वपूर्ण नही है या इसने विकास के मौजूदा विमर्श को प्रभावित नहीं किया है। इसने नई वित्तीय और तकनीकी नैतिकता से परिचय करवा कर और ‘साझेदारी’ और ‘राष्ट्रीय स्वामित्व’ की अवधारणा को मानदंड के तौर पर स्थापित कर निश्चित तौर पर ‘मदद’ को नए रूप में परिभाषित किया है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विकास, वित्त और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए नई दक्षिणी साझेदारी ने अपनी निश्चित विकासपरक नीति के एजेंडा और शर्तों पर मिलने वाले वित्त (कंडीशनल फाइनान्सिंग )की मदद से ओईसीडी के निष्क्रिय स्वरूप को झकझोड़ कर रख दिया है। इसने मदद देने वाले पारंपरिक देशों को ज्यादा सतर्क और सजग बना दिया है।
लेकिन अगर साउथ-साउथ कॉपरेशन को ज्यादा खींचा जाए तो वह वैश्विक विकास के लिहाज से भारत जैसे देश की भूमिका और महत्वाकांक्षा को महज दक्षिणी एकजुटता के विस्तार के रूप में काफी सीमित कर सकता है। जैसा कि साउथ-साउथ कॉपरेशन की सीमाओं में निषेध किया गया है और कुछ हद तक दक्षिण के लिए दक्षिण के सिद्धांत में बताया गया है। भारत की विकासपरक साझेदारी में ग्लोबल साउथ बहुत महत्वपू्र्ण और नैतिक बंधन तो हो सकता है लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा या आर्थिक कूटनीतिक दायित्व का दार्शनिक बंधन नहीं हो सकता।
1.3 अरब लोगों के देश के लिए यह बहुत सीमित विश्व दृष्टकोण होगा। खास कर तब जब इसने अपने लिए अगले डेढ़ दशक में आठ खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इसे हर हाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोक उपयोगी वस्तुएं और सेवा मुहैया करवाने वाला देश बनना है। साथ ही मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी तो निभानी ही है साथ ही इस शताब्दी की मांग के अनुरूप नए संस्थानों को खड़ा भी करना है। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही भारत की आर्थिक कूटनीति का आधार बनना चाहिए और नीतियां तैयार करनी चाहिएं। भले ही यह साथ-साथ ऐतिहासिक एकजुटता के राग अलापता रहे।
भारत की भूमिका को इसके ‘उत्थान’ के पैमाने पर देखते हुए नई परिभाषा देने की जरूरत है। जो अपने आर्थिक वजन से बड़ी भूमिका में है और समय के साथ और बहुत बढ़ने वाला है। ऐसा कई कारणों से है। पहला तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय विकास और मौजूदा ढांचागत सुविधाओं के संवर्धन के लिए पूंजी में सबसे बड़ा सहयोग अगले 15 वर्षों में भारत और इसके निगमों की ओर से आने वाला है। अगर यह वृद्धि संबंधी पूंजी कुल विकासपरक वित्त का बहुत छोटा हिस्सा भी हुई तो भी भारत नए सहयोगकर्ताओं में सबसे आगे होगा। इस वजह से जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के दौर में अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। आंकड़ों के आइने में देखें तो सामान्य गणना के मुताबिक विदेशी मदद, सस्ते कर्ज और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए निर्धारित मौजूदा 2.35 अरब डॉलर की रकम वर्ष 2030 तक बढ़ कर 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। उधर, यूके के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआइडी) का वर्ष 2015-16 के लिए सालाना बजट 12 अरब डॉलर है जो आने वाले दिनों में काफी घटने वाला है। जर्मनी की जीआईजेड जैसी दूसरी एजेंसियां भी किसी तरह अपना मौजूदा आंकड़ा भी बनाएं रखें तो काफी है।
दूसरी अहम बात यह है कि संख्या के अलावा भारत एक नया मार्ग भी पेश करेगा और इसके पास साझा करने के लिए विकास की एक नई अवधारणा होगी। पूरी संभावना है कि यह जैविक र्इंधन की सीमा में बंधे और जलवायु को ले कर जागरुक दुनिया में एक निम्न आय से आगे बढ़ कर मध्य-आय अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाए। इस बदलाव की ओर बढ़ते हुए इसे यूरोप और अमेरिका, जापान और चीन की ओर से अपनाई गई नीति से और आर्थिक विकल्प से हट कर सोचना होगा। सस्ते मजदूर, थोक निर्माण, सस्ती ऊर्जा, शोषण पर आधारित आर्थिक नीतियां जिनमें मानवाधिकारों के लिए कोई सम्मान नहीं हो और इन सब के साथ कुछ हद तक उदार व खुली व्यापार व्यवस्था ने ही पिछले दशक के दौरान विकास को परिभाषित किया है। भारत की कहानी, जब तैयार होगी तो वह बिल्कुल अलहदा होगी। जिसका किसी से कोई मेल नहीं होगा। दूसरी ऐसी अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए यह एक उदाहरण होगी। हालांकि अभी से भारत के बदलाव के ब्योरों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ पहलुओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में बदलाव ऐसी खोज पर आधारित होगा जो लागत घटाएगी और सस्ती सेवा उपलब्ध करवाने वाली अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में मदद करेगी। घरेलू के साथ ही विश्व बाजार के लिए भी सस्ती और उच्च श्रेणी की सेवा ही इसकी मुख्य विशेषता होगी। यह न सिर्फ पिछले तीन दशक के दौरान जुड़ी लगभग आधी अरब आबादी के लिए बल्कि तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिहाज से भी कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के इंतजाम का एक नया ढांचा खड़ा कर चुका होगा।
और अंत में, मुमकिन है कि भारत दक्षिण एशिया और विकासशील व उभरती नई दुनिया में व्यापार के नए ढांचे को तैयार करने का रास्ता भी दिखाए। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था बहुत दबाव में है, क्योंकि ओईसीडी और कुछ अन्य देशों की ओर से प्रतिबंधात्मक समझौतों की वजह से डब्लूटीओ की संधि उपेक्षित हो रही है। साथ ही विकासशील देशों का लाभ कम हो रहा है। मौजूदा व्यापार व्यवस्था एक अधूरे खगौलीकरण पर आधारित है। इसमें पूंजी और सामान की आवजाही पर जोर है, लेकिन उस लिहाज से सेवाओं और लोगों की आवाजाही को ले कर वैसी स्थिति नहीं है। 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप चलने को बाध्य विकासशील देश सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहे हैं ऐसे में यह आंशिक खगौलीकरण उनके लिए अलग चुनौती पैदा कर रहा है। भारत, इसके दक्षिण एशियाई पड़ोसी, अफ्रीका और कुछ अन्य के लिए यह मौका है कि वे अपने व्यापार समझौतों को नए सिरे से तैयार करें ताकि 21वीं सदी के अपने विकास पथ पर चल सकें।
उत्थान के पैमाने पर देखते हुए भारत की विकासपरक साझेदारी और आर्थिक कूटनीति पूरी तरह से रुचि और प्रभाव के तीन मुख्य वृत्त के रूप में होनी चाहिए। पहले में भारत के करीबी पड़ोसी और बड़ी शक्तियां माने जाने वाले देश हों, दूसरे में एशिया और हिंद महासागर के तट के बाकी पड़ोसी देश आ जाएं, इनमें कुछ जगहों का महत्व इस लिहाज से होगा कि वहां से हमें क्या मिलता है। तीसरे में भौगोलिक रूप से दूर स्थित देश शामिल हो सकते हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां, अहम मुद्दे और संस्थाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। हर सेट में विकासपरक साझेदारी और आर्थिक कूटनीति के संचालन की अलग क्षमताएं, प्राथमिकताएं और हित सुनिश्चित हों।
इन तीन वृत्त में बंट गई विकासपरक साझेदारी की मदद से भारत को अपने उपयुक्त दिशा तो मिलेगी ही, अपने मुताबिक लचीलापन और खास तरह के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इससे वह भौगोलिक रूप से अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग रवैया भी अपना सकेगा, ऐसी साझेदारियां और संस्थान बना सकेगा जो उत्तर और दक्षिण की दूरियों को समाप्त कर सकें। अपने तात्कालिक आर्थिक और रणनीतिक हित और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेवारियों के बीच संतुलन कायम रख सकेगा। साथ ही खगौलीय विकासपरक आपूर्तिकर्ता की जटिल और बहुल जरूरतों को पूरा कर सकेगा।
हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि साउथ-साउथ कॉपरेशन के बजाय उत्थान के पैमाने की वकालत करने का मतलब यह नहीं है कि भारत आर्थिक कूटनीति समुदायों की अहमियत को और साझा मानकों को दरकिनार कर दे और एकसूत्रीय तर्क पर काम करे। इससे ठीक उलट एक सतत विकासपरक आपूर्तिकर्ता के तौर पर भारत के लिए एक मानदंड स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में सामने आना ज्यादा जरूरी होगा। इसे समुदायों का निर्माण करना होगा, अवसर उपलब्ध करवाने होंगे, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम के युग्म के रूप में मौजूद दूरियों को पाटते हुए विकास की राह तलाशनी होगी। एक अग्रणी शक्ति के रूप में इसे खुद राह दिखानी होगी।
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV