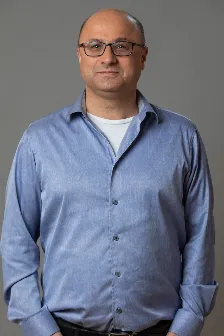कभी जन्नत के बाग़ के तौर पर जाना जाने वाला दक्षिणी इराक़ का इलाक़ा, आने वाले दशकों में जलते हुए बंज़र इलाक़े में तब्दील होने जा रहा है. इस लेखक और इज़राइल की मौसम सेवा के मुख्य रिसर्चर डॉक्टर योआव लेवी ने मिलकर जो अध्ययन किया था, उसमें ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि वो दिन बहुत दूर नहीं, जब इस इलाक़े के लोगों को रोज़ाना घंटों तक 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की झुलस झेलनी पड़ेगी. वैसे तो ये भयानक भविष्यवाणी आने वाले समय के लिए है. लेकिन, तापमान में ये जानलेवा बढ़त कोई अटकल नहीं, बल्कि आज ही इराक़ में एक सच्चाई बन चुकी है.
भयानक भविष्यवाणी आने वाले समय के लिए है. लेकिन, तापमान में ये जानलेवा बढ़त कोई अटकल नहीं, बल्कि आज ही इराक़ में एक सच्चाई बन चुकी है.
2012 से 2019 के बीच किए गए आकलनों में पाया गया है कि साल में कई बार तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के भयानक स्तर तक पहुंच जाता है. पिछले साल, हमने इस इलाक़े में 50 डिग्री सेल्सिय से ज़्यादा तापमान वाली लू चलती देखी थीं, जिससे बार बार बिजली कट जाती थी. इराक़ की जीवन रेखा कही जाने वाली दजला और फ़रात नदियों का पानी बहुत कम हो गया था और इसके साथ ही खाने पीने के सामान की क़िल्लत हो गई थी. नाक़ाबिल-ए-बर्दाश्त गर्मी की वजह से मज़दूरों की उत्पादकता में भारी गिरावट आई थी और रेतीले तूफ़ानों में बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे तेल टैंकर, इराक़ के दक्षिणी इलाक़े के समुद्री बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाते थे. इन चुनौतियों ने न केवल सामाजिक आर्थिक उथल-पुथल मचा दी है, बल्कि इनसे सुरक्षा के मामले में भी गंभीर बाधाएं आ रही हैं. हमने इसका सबूत 2018 में इराक़ में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की शक्ल में देखा था.
मध्य पूर्व की स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का असर लीबिया में भी देखा जा रहा है. भयंकर तबाही वाले एक दशक लंबे गृह युद्ध के बाद, हाल के वर्षों में लीबिया की स्थिति मे कुछ सुधार आता देखा जा रहा था. 2018 में जहां उसका तेल उत्पादन, 315,000 बैरल प्रति दिन था, वो अभी पिछले महीने बढ़कर 12 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था. लेकिन, सितंबर 2023 में आए भयंकर समुद्री चक्रवात ने लीबिया के एक बड़े हिस्से को डुबो दिया था. इस तूफ़ान की वजह से लीबिया के चार अहम समुद्री बंदरगाह बंद हो गए और उसके तेल निर्यात में रुकावट आ गई. इराक़ की तरह, लीबिया में भी जलवायु संबंधी एक तबाही ने हिंसा को भड़का दिया, जब बाढ़ से निपटने में अपने अपर्याप्त इंतज़ामों की वजह से सरकार को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा. इस बाढ़ में पांच हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान चली गई.
मध्य पूर्व में जलवायु संकट
इराक़ और लीबिया में जहां क़ुदरती आपदाओं की वजह से भड़के दंगे सीमित समय के लिए ही हुए थे. लेकिन, सीरिया में तो 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध की एक वजह जलवायु से जुड़ी एक तबाही को भी कहा जाता है. 2010 में सीरिया को हज़ार साल के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से क़रीब आठ लाख लोगों की रोज़ी-रोटी छिन गई और सीरिया की 85 प्रतिशत खेती तबाह हो गई. इस सूखे की वजह से क़रीब 15 लाख लोगों को शहरों की तरफ़ भागना पड़ा, जो पहले से आबादी के बोझ तले दबे हुए थे. इस वजह से असंतोष और अराजकता पैदा हो गई.
लेबनान में विरोध प्रदर्शनों से कुछ हफ़्तों पहले, भयंकर हीट वेव चल रही थी, जिसकी वजह से शुफ की पहाड़ियों में भयंकर आग लग गई. इसका नतीजा ये हुआ कि हवा प्रदूषित हो गई और पानी के कुछ हिस्से को न पीने लायक़ घोषित कर दिया गया.
मध्य पूर्व में एक और देश ईरान को भी हाल के वर्षों में कई बार ऐसे दंगों का सामना करना पड़ा रहा है, जिनका संबंध जलवायु संकट से है. एक ज़माने में ईरान को मध्य पूर्व (पश्चिमी एशिया) की रोटी की टोकरी का जाता था. लेकिन, पिछले कई वर्षों से ईरान जलवायु परिवर्तन की वजह से विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहा है. 2018 और फिर 2021 में भयंकर सूखों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया. लोग, पानी के बेहतर रख-रखाव की मांग लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी सरकार के काम-काज के प्रति नाख़ुशी जताई. दक्षिणी ईरान में लंबे समय से चल रहे सूखे और नियमित पानी की आपूर्ति में कमी आने की वजह से वहां , अगस्त 2023 में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे.
अक्टूबर 2019 में जब लेबनान की सरकार ने टैक्स बढ़ाने के लिए तेल की सब्सिडी में कटौती का इरादा जताया, तो वहां भी हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे. हालांकि, लंबे समय से हिंसक गृह युद्ध के शिकार लेबनान में होने वाला ये कोई पहला उग्र विरोध प्रदर्शन नहीं था. लेकिन, इस हिंसक दंगे के पीछे भी जलवायु परिवर्तन का हाथ था. लेबनान में विरोध प्रदर्शनों से कुछ हफ़्तों पहले, भयंकर हीट वेव चल रही थी, जिसकी वजह से शुफ की पहाड़ियों में भयंकर आग लग गई. इसका नतीजा ये हुआ कि हवा प्रदूषित हो गई और पानी के कुछ हिस्से को न पीने लायक़ घोषित कर दिया गया. जंगल में लगी ये आग उस ज़मीन में भी फैल गई, जिसे ‘लेबनान के पेड़ों की ज़मीन’ कहा जाता है, और जिसे लेबनान के झंडे में भी जगह दी गई है. इसका ये मतलब है कि जो देश हज़ारों वर्षों से अपने देवदार के ऊंचे दरख़्तों की अपनी पहचान बचाकर रखे हुए था, उस विशिष्ट पहचान को भी जंगल की भयंकर आग से नुक़सान ख़तरा पैदा हो गया था. शुफ की पहाड़ियां देवदार के पेड़ों से भरी पड़ी हैं, जिनकी वजह से एक बार आग भड़की तो ये फिर गांव के गांव और कई बार तो शहरों को भी निगल सकती है. इसीलिए, वैसे तो बहुत से लोगों की नज़र में पानी और बिजली की सुविधा पर फ़ौरी ख़तरा ज़्यादा गंभीर मसला है. लेकिन, लेबनान में जलवायु परिवर्तन ने दिखा दिया है कि ये ख़तरा सिर पर आ पहुंचा है.
मध्य पूर्व की जटिल चुनौतियों की सबसे बड़ी मिसाल तो यमन है. यमन, भयंकर ग़रीबी का शिकार है. एक अनुमान के मुताबिक़, यमन में बेरोज़गारी 13.59 प्रतिशत के ख़तरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, यहां भयंकर निरक्षरता और मीठे पानी तक बहुत कम लोगों की पहुंच जैसी चुनौतियां भी हैं. यमन शिया और सुन्नी, दोनों समुदायों के कट्टर इस्लामिक समूहों के अड्डे का काम भी करता है. इन सबके ऊपर, जलवायु परिवर्तन के मामले में यमन दुनिया के सबसे कमज़ोर स्थिति वाले देशों में से एक है ND-GAIN सूचकांक के 181 देशों में यमन 171वें स्थान पर है. सीरिया में गृहयुद्ध की तरह, यमन में भी चल रहे युद्ध और जलवायु परिवर्तन के बीच एक रिश्ता देखा जा सकता है- वहां के लोगों को पीने के पानी की सख़्त ज़रूरत है.
यमन की अराजकता को बढ़ाने में, जलवायु संकट की वजह से पैदा हुए पानी के इस संकट की भूमिका बेहद अहम है और इस संकट के चलते, मौजूदा संघर्ष और भी लंबा खिंच सकता है. यमन में तेल की क़ीमतें, जो पानी के दाम से नज़दीकी से जुड़ी हैं, ने 2014 में विरोध प्रदर्शनों को जन्म देने में योगदान दिया था. यमन, दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है. वो पहले से ही इलाक़े के सूखे और भयंकर गर्म जलवायु का असर झेल रहा है. वैसे तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा युद्ध में पानी के संकट की कितनी बड़ी भूमिका रही थी. लेकिन, 2011 की एक रिपोर्ट में पहले ही उन कारणों को रेखांकित किया गया था, जिनमें आगे चलकर यमन में गृह युद्ध भड़काने क्षमता थी. इसमें पानी की इतनी भयंकर क़िल्लत भी शामिल थी, जो यमन के मुख्य रूप से खेती पर आश्रित लोगों के अस्तित्व और उनकी रोज़ी-रोटी के लिए ख़तरा बन गई है. इसके अलावा, फरवरी 2016 में आई ख़बरों से पता चला था कि सऊदी अरब के विमानों ने एक जलाशय पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया था, उस जलाशय में यमन के 30 हज़ार लोगों की ज़रूरत भर का, लगभग पांच हज़ार क्यूबिक मीटर पानी था. जलाशय पर इस बमबारी ने हमले वाली जगह के पास लड़ाई को और भड़का दिया था. ऐसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन, लोगों के विरोध प्रदर्शन और लगातार बनी हुई क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच आपसी संबंध को रेखांकित करती हैं.
मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सुरक्षा की चुनौतियों से ज़्यादा जोड़कर देखा जाता है. लेकिन, अब यहां जलवायु संकट एक बड़ी चिंता बन गया है. इसकी वजह से हिंसा, ग़रीबी, असमानता और अप्रवास की समस्याएं पैदा होती हैं और इससे क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ावा मिलता है.
मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सुरक्षा की चुनौतियों से ज़्यादा जोड़कर देखा जाता है. लेकिन, अब यहां जलवायु संकट एक बड़ी चिंता बन गया है. इसकी वजह से हिंसा, ग़रीबी, असमानता और अप्रवास की समस्याएं पैदा होती हैं और इससे क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ावा मिलता है. ऊंची जन्म दर और खपत वाले इस क्षेत्र में खाने के सामान की कमी की वजह से बेहद भयंकर गर्मी वाले इलाक़ों से लोग ठंडे इलाक़ों की तरफ भाग रहे हैं. ऐसे में, जलवायु संकट की वजह से मध्य पूर्व की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को रोज़गार देने वाले कृषि क्षेत्र के सामने बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है. इस जलवायु संकट से मध्य पूर्व के सामने पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी हो गई है. इस उथल पुथल से न केवल क्षेत्रीय स्थिरता, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता को ख़तरा है.
आगे की राह
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने जा रहा जलवायु सम्मेलन (COP28), मध्य पूर्व और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए नींद से जगाने वाला मौक़ा है, कि दोनों इस भयंकर ख़तरे से निपटने के लिए मिलजुल कर प्रयास करें. इज़राइल पर हमास के बर्बर हमले और उसके जवाब में इज़राइल के पलटवार और इस इलाक़े में हिंसा भड़क उठने के मंडराते ख़तरे को देखते हुए, ये जलवायु सम्मेलन क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का एक अहम मंच साबित हो सकता है, जिसके ज़रिए समस्या के समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है.
ऐतिहासिक और मौजूदा दुश्मनियों के बावजूद और तेज़ी से हो रहे बदलावों के बीच, मध्य पूर्व के देशों को जलवायु परिवर्तन के साझा ख़तरे को स्वीकार करना होगा. जानकारी साझा करने, आपदा से निपटने की रणनीतियों और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों में निवेश के मामले में क्षेत्रीय सहयोग की काफ़ी संभावना दिखती है.
इस बार जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी एक ऐसा देश कर रहा है, जिसके पास परिवर्तन लाने वाली नीतियों में सफलता का अनुभव है और जिसकी क्षेत्रीय हैसियत बढ़ती जा रही है. जलवायु सम्मेलन (COP28) उस समय हो रहा है जब दुनिया ये मान रही है कि जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी जैसे मसले, और हां युद्ध से निपटने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाधानों की ज़रूरत है. इन हालात को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात विशेष रूप से ऐसी स्थिति में है कि वो उस ख़तरे से निपटने के प्रयासों की अगुवाई कर सके, जिनके बारे में बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ख़तरा इस क्षेत्र के लिए फ़ौरी और अस्तित्व का संकट, दोनों ही है.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV