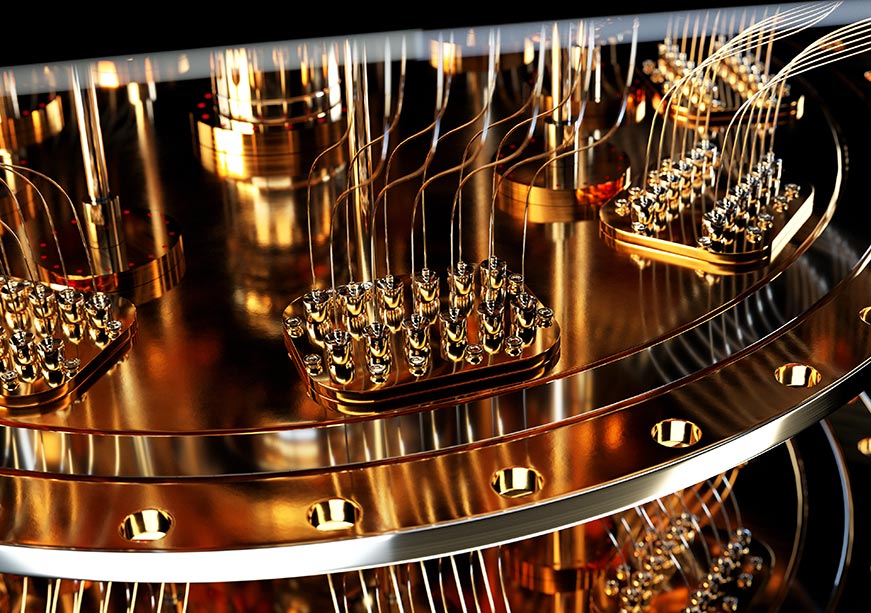सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था और उभर रहे जलवायु संकट के कारण बढ़ते भू-राजनीतिक संकट ने कई बाधाएं पैदा कर दी हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में जेंडर (लैंगिक) की खाई को पाटने की पुख्ता कोशिशें नाकाम हो गई हैं. अक्सर लैंगिक असमानता को बढ़ाने वाली चीज़ें विकास के अलग-अलग क्षेत्रों में सामूहिक रूप से लैंगिक दूरी को बढ़ाती हैं. चूंकि अलग-अलग देश कठोर वित्तीय और कर्ज़ से जुड़ी सीमाओं के तहत घुट रहे हैं, ऐसे में महिलाएं ग़रीबी में डूबी हुई हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा निरक्षर हैं और डिजिटल बंटवारे का उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. दुनिया भर में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां अपने परिवारों के लिए खाना बनाने में लगी हुई हैं लेकिन फिर भी वो भूख, कुपोषण और पानी की कमी के मामले में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं.
ये लेख पूरी तरह व्यापक नहीं है लेकिन प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक भागीदारी, महिलाओं का नेतृत्व एवं राजनीतिक हिस्सेदारी, महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के ख़ात्मे, बनी हुई लैंगिक रूढ़िवादिता को लेकर बदलती सोच और लैंगिक समानता की तरफ प्रगति में बाधा डालने वाली बजट प्रणाली की कम लैंगिक प्रतिक्रिया में त्वरित परिणामों की स्थिति की समीक्षा करता है.
अलग-अलग संस्कृतियों में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का चक्र भी लगातार बना हुआ है. कोविड-19 संकट से इसमें और अधिक बढ़ोतरी हुई है. उच्च शिक्षा जैसे कि STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ) के क्षेत्र, रोज़गार और नेतृत्व एवं निर्णय लेने की भूमिका समेत स्वास्थ्य परिणामों में व्यापक अंतर मौजूद है. इन समस्याओं के बावजूद विकास के एजेंडे के रूप में लैंगिक समानता के लिए प्रगति को संरचनात्मक शक्ति के समीकरण से लगातार चुनौती मिल रही है. ये झटके मानव विकास के साथ-साथ 2030 के सतत विकास के एजेंडे में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्पष्ट धक्का हैं. वैसे तो ये लेख पूरी तरह व्यापक नहीं है लेकिन प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक भागीदारी, महिलाओं का नेतृत्व एवं राजनीतिक हिस्सेदारी, महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के ख़ात्मे, बनी हुई लैंगिक रूढ़िवादिता को लेकर बदलती सोच और लैंगिक समानता की तरफ प्रगति में बाधा डालने वाली बजट प्रणाली की कम लैंगिक प्रतिक्रिया में त्वरित परिणामों की स्थिति की समीक्षा करता है.
लैंगिक समानता: आर्थिक बाधा
कानूनी सुधार, जो महिलाओं के असमान आर्थिक अधिकारों का समर्थन कर सकते थे, की धीमी गति 2022 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. अफसोस की बात है कि इसने अलग-अलग क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया है और अक्सर समानता की तरफ प्रगति को पीछे खींचने में सफल रही है. युवा पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बीच बेरोज़गारी ज़्यादा बनी हुई है. श्रम बल (लेबर फोर्स) में पूर्णकालिक (फुल-टाइम) नौकरियां हासिल करने के मामले में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को आधा अवसर मिलता है और उन्हें अक्सर कामकाज की जगह पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. वैसे तो विकासशील देशों में कृषि श्रम बल में महिलाओं का हिस्सा लगभग आधा है लेकिन ज़मीन पर मालिकाना हक़ का न होना उन्हें सूचना का उपयोग करने, कर्ज़ लेने और किसानों के संघ में सदस्यता से रोकता है. सब-सहारन अफ्रीका (सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित क्षेत्र), लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया और आम तौर पर निम्न एवं निम्न-मध्यम आय (लोअर-मिडिल इनकम) वाले देशों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बिना पर्याप्त अधिकारों के महिलाओं की बहुतायत है. दुनिया भर में घरेलू कामगारों में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए अनौपचारिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता व्याप्त है. महामारी की वजह से उन्हें नौकरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. चूंकि अनौपचारिक रोज़गार के साथ अक्सर उच्च ग़रीबी दर और कम सामाजिक गतिशीलता जुड़ी होती है, ऐसे में महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं.
दुनिया भर में घरेलू कामगारों में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए अनौपचारिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता व्याप्त है. महामारी की वजह से उन्हें नौकरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ.
कोविड-19 महामारी के बाद भी दुनिया के सभी इलाकों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक रोज़गार गंवाया है. इसका आंशिक कारण परिवार की देखभाल को लेकर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी है. दुनिया भर में महिलाएं बिना वेतन लिए देखभाल के काम (अनपेड केयर वर्क) में घंटों जुटी रहती हैं. महामारी से पहले भारत में महिलाएं कथित तौर पर पुरुषों की तुलना में आठ घंटे ज़्यादा अनपेड केयर वर्क में बिताती थीं जो दुनिया भर के तीन घंटे के औसत से बहुत ज़्यादा था. अनपेड केयर वर्क में लैंगिक असमानता को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रम परिणामों जैसे कि श्रम बल में हिस्सेदारी, आय और क्वालिटी जॉब स्टैंडर्ड में लैंगिक अंतर के विश्लेषण में ये ज़रूरी चीज़ है.
हुनर हासिल करने में लैंगिक दूरी, वित्त एवं तकनीक की उपलब्धता और बाज़ार के उतार-चढ़ाव को लेकर सीमित जानकारी की बाधाओं से प्रभावित महिलाओं का प्रतिनिधित्व उद्यम और व्यवसाय में कम है. यहां तक कि कंपनियों में मैनेजर स्तर की भूमिका में भी पुरुषों का दबदबा है और भारत में टॉप पदों पर केवल 15 प्रतिशत तक महिलाएं हैं जो कि G20 के सदस्य देशों जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले काफी कम है.
महिलाएं, नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी
संरचनात्मक लैंगिक पक्षपात और मानदंड दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में महिलाओं की राजनीतिक नुमाइंदगी में प्रगति के मामले में रुकावट बने हुए हैं. इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2023 को दुनिया भर में संसद के एकल या निम्न सदन में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 26.5 प्रतिशत थी. इसमें साल-दर-साल केवल 0.4 प्रतिशत प्वाइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो कि छह वर्षों में सबसे धीमी रफ्तार थी. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने भी पहली और मौजूदा लोकसभा के दौरान महिलाओं की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत होने की कम बढ़ोतरी ही देखी है.
जेंडर के आधार पर हिंसा का ख़ात्मा
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर तीन में से एक महिला एवं लड़की ने अपने जीवनकाल में कम-से-कम एक बार किसी नज़दीकी साथी या गैर-साथी के द्वारा किसी-न-किसी रूप में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है.
महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा की दुर्भावना लगातार बढ़ती जा रही है और महामारी ने जेंडर के आधार पर हिंसा (GBV) को ख़तरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है. लगभग 54 प्रतिशत महिलाओं ने अपने समुदायों में हिंसा में कथित बढ़ोतरी की जानकारी दी है. इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी लैटिन अमेरिका के देशों और सब-सहारन अफ्रीका में बताई गई है. तकनीक का इस्तेमाल करके महिलाओं के ख़िलाफ़ लैंगिक दुर्व्यवहार भी बढ़ रहा है. इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के अनुसार दुनिया भर में 16-58 प्रतिशत महिलाएं इससे प्रभावित हुई हैं. मानव तस्करी, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के जननांग की विकृति (फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन) दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है. महिलाएं काम-काज की जगह पर, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय और सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न के मामले में असुरक्षित हैं जो उनकी उत्पादक आर्थिक हिस्सेदारी पर दीर्घकालीन असर छोड़ सकता है. इसके साथ-साथ मौजूदा समय के दो बेरहम युद्धों ने दिखाया है कि संघर्ष की स्थिति में महिलाएं गंभीर हिंसा का बहुत ज़्यादा शिकार हो सकती हैं.
जेंडर के आधार पर घिसी-पिटी पाबंदियों को तोड़ना
घरेलू लैंगिक भूमिकाओं, ताकत और वर्चस्व को लेकर हमारे समाज में सामान्य रवैया व्याप्त है. ये पिछले दिनों की एक रिसर्च से भी पता चला जो बताती है कि 30 साल के आसपास के मर्दों की तुलना में युवा पुरुष ज़्यादा रूढ़िवादी और पाबंदी वाली सोच रखते हैं. इन पुरातन विचारों का परिणाम चौंका देने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभावों में निकल सकता है जिसकी वजह से अलग-अलग देशों को GDP में खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है. खेद की बात है कि इन भेदभावपूर्ण मानसिकताओं के ख़िलाफ़ बदलाव धीमा है. लैंगिक सामाजिक और व्यवहारिक रवैये को लेकर एक वैश्विक सर्वे रिपोर्ट में 2014 से 2022 के बीच बेहद मामूली बदलाव हुआ है. चिंता की बात है कि महिलाओं के आर्थिक अवसरों से जुड़े पक्षपात बढ़ते ही जा रहे हैं और ये भरोसा बढ़ रहा है कि जब नौकरियां दुर्लभ हो जाएं तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को स्पष्ट लाभ मिलना चाहिए. पहले रेखा-चित्र से भी इसका पता चलता है.
रेखा-चित्र 1: 2014-2021 के दौरान पक्षपात रखने वाले लोगों का प्रतिशत

स्रोत: Inglehart et al. (2022), World Values Survey: All Rounds
लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए वित्त से जुड़े साधन
वैसे तो जेंडर बजटिंग (पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता दूर करने के लिए संसाधनों का आवंटन) की रणनीति व्यापक है लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसका अलग-अलग असर रहा है. एक अध्ययन के अनुसार वित्तीय नीतियों में जेंडर बजटिंग जैसी कोशिशों को शामिल करने के बावजूद G20 देश प्रभावी ढंग से इन साधनों का उपयोग, इनकी समीक्षा और निगरानी में पीछे हो रहे हैं. G20 देशों से इकट्ठा डेटा से जेंडर बजटिंग इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिया गया रेखा-चित्र दिखाता है कि कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और जापान ने दूसरे सदस्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है.
रेखा-चित्र 2: G20 देशों में जेंडर बजटिंग इंडेक्स

स्रोत: IMF, G20 देशों में जेंडर बजटिंग
जेंडर समानता की तरफ सुस्त और असंतुलित कदम
वैसे तो पिछले दशक के दौरान बड़ी मेहनत से कुछ सफलताएं हासिल हुईं जैसे कि लड़कियों की मानव पूंजी अब 90 प्रतिशत देशों में लड़कों के बराबर या उनसे भी अधिक है. ये तीसरे रेखाचित्र में लैंगिक तौर पर उपलब्ध अलग-अलग आंकड़ों में दिखाया गया है. लेकिन ये सफलताएं भी असमान हैं क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग आंकड़े हैं, ख़ास तौर पर माताओं की मृत्यु (मैटरनल डेथ) और माध्यमिक शिक्षा (सेकेंडरी एजुकेशन) के मामले में. कई देशों में मानव सामाजिक पूंजी की सफलता पर वैश्विक महामारी के असर ने पानी फेर दिया है.
रेखा-चित्र 3: मानव पूंजी इंडेक्स और उसके घटकों के लिए लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात, 2020

स्रोत: 2020 के मानव पूंजी इंडेक्स (HCI) के आधार पर विश्व बैंक की गणना
लैंगिक समानता अक्सर सामाजिक रूप से आरोपित और कुछ मामलों में राजनीतिक तौर पर विवादित होती है लेकिन ये एक आधारभूत मानवाधिकार बनी हुई है जो समावेशी और टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है. एक ध्यान देने योग्य प्रयास भारत के द्वारा विकास परिदृश्य में महिलाओं के नेतृत्व के लिए ज़ोर लगाना था. भारत की G20 अध्यक्षता के केंद्र में स्थित ‘महिला के नेतृत्व वाले विकास के एजेंडे’ की एक अनूठी शब्दावली ने लैंगिक प्रतिक्रिया वाले नीति निर्माण में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की. इसने जलवायु परिवर्तन के मामले में राहत और उसके मुताबिक ढलने, लैंगिक आधार पर डिजिटल बंटवारे को दूर करने, शिक्षा में निवेश, उद्यमशीलता एवं कौशल बढ़ाने के उपायों, ग्रामीण नेतृत्व को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में उनकी लाभकारी भागीदारी को बढ़ाने में महिलाओं के अधिकार को प्राथमिकता देने के लिए एक ब्लूप्रिंट का निर्माण किया. ब्लूप्रिंट तैयार हो जाने के बाद अब बदलाव के प्रमुख प्रेरकों के माध्यम से संचालन की योजना बनाने का समय आ गया है, जैसे कि: i) अवसरों, वित्त की उपलब्धता, कौशल, इनोवेशन, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के मामले में महिलाओं को भविष्य के काम-काज में समान हिस्सेदार के रूप में सुनिश्चित करना; ii) अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारियों के ज़रिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और संस्थागत इनोवेशन को बढ़ाना, ख़ास तौर पर महिलाओं की ग़रीबी और कठिन मेहनत को कम करने में; iii) वैश्विक स्तर पर अलग-अलग लैंगिक डेटा तैयार करना जो नीति निर्माताओं और अकादमिक जगत के लोगों के लिए उपलब्ध हो ताकि साक्ष्य आधारित विश्लेषण का विकास और समीक्षा होने के साथ-साथ प्रगति का पता लगाया जा सके और उसकी निगरानी की जा सके; iv) वित्तीय नीतियों, बजट प्रबंधन और ख़रीद की प्रणाली को आसान करना ताकि लैंगिक समानता की राह में आने वाली बाधाओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त फंड का आवंटन किया जा सके; v) नुकसानदायक प्रथाओं को चुनौती देने जैसे कि बाल विवाह को रोकने और जेंडर आधारित हिंसा को ख़त्म करने के लिए प्रमुख किरदारों को शामिल करना जिसका प्रतिबंधात्मक मानसिकता को बदलने पर स्थायी प्रभाव हो सकता है और संतुलित लैंगिक नतीजे मिल सकते हैं. इनमें से कुछ लैंगिक खाई को पाटना विकास के लिए निर्णायक होगा नहीं तो लैंगिक समानता 300 प्रकाश वर्ष दूर बनी रहेगी.
अरुंधति बिस्वास कुंडल ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV