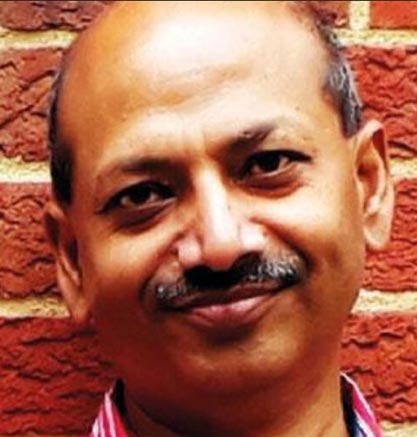Image Source: Getty
यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फ़ॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) की स्थापना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने और उनको सक्षम बनाने वाली एकमात्र एजेंसी के रूप में की थी. यह शीत युद्ध की देन है, जिसकी जड़ें ‘मार्शल प्लान’ (1948) से जुड़ी हैं, जिसे तकनीकी तौर पर 1948 का आर्थिक पुनर्प्राप्ति अधिनियम, यानी इकोनॉमी रिकवरी एक्ट कहा जाता है. इस अधिनियम पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दस्तख़त किए थे, ताकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जा सके. इसने अंतरराष्ट्रीय विकास में मदद करने संबंधी नई परंपरा की शुरुआत की थी. 1970 के दशक में, जिसे ‘विकास का दशक’ कहा जाता है, स्थापित USAID का मुख्य लक्ष्य खाद्य और पोषण, जनसंख्या नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में सहायता करना था. बाद में यह एजेंसी स्वेच्छा से काम करने वाले निजी संगठनों, यानी PVO और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से बड़े-बड़े विकास कार्यक्रम करने लगी. साल 2013 का इसका ‘मिशन स्टेटमेंट’ अमेरिका की ‘सुरक्षा और समृद्धि’ को आगे बढ़ाते हुए अत्यधिक गरीबी को ख़त्म करने और लचीले व लोकतांत्रिक समाजों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी बनाने पर ज़ोर देता है.
भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को USAID से लाभ
हाल ही में पद संभालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि वह USAID को एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में बंद कर देंगे और इसे शायद संघीय विभागों के अधीन कर दिया जाएगा. भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बीते करीब सात दशकों से USAID/ इंडिया हेल्थ ऑफिस काम कर रहा है और अब इसका दायरा काफी बड़ा हो चुका है. यह भारत के स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डालने वाली एक अहम साझेदारी के रूप में काम कर रहा है. जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस एजेंसी के साथ मिलकर भारत काम कर रहा है, वे हैं- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, पोलियो उन्मूलन, टीकाकरण, तपेदिक (टीबी), एचआईवी/ एड्स, रोग निगरानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, शहरी स्वास्थ्य सहित पूरी स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और महामारी की तैयारी.
यहां दो मुद्दे काफी प्रासंगिक हैं- पहला, अगर यह मदद मिलनी बंद होती है, तो क्या केंद्रीय बजट में इस कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय हैं, जो करीब 12 से 13 अरब रुपये होते हैं, और दूसरा, इन कार्यक्रमों पर कितना असर पड़ेगा?
आंकड़े बताते हैं कि साल 1990 और 2000 के बीच भारत को हर वर्ष औसतन करीब 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद मिली. कोविड-19 के दौरान इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई. हालांकि, 2024 में घटने के बावजूद यह राशि लगभग 15.2 करोड़ डॉलर थी. 2023 में हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 12 करोड़ डॉलर की मदद मिली थी. यहां दो मुद्दे काफी प्रासंगिक हैं- पहला, अगर यह मदद मिलनी बंद होती है, तो क्या केंद्रीय बजट में इस कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय हैं, जो करीब 12 से 13 अरब रुपये होते हैं, और दूसरा, इन कार्यक्रमों पर कितना असर पड़ेगा?
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 26 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर 959.58 अरब रुपये का प्रावधान किया है. बेशक, बीते वर्षों की तुलना में इसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी की गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की ज़रूरतों को देखते हुए आलोचक इस रक़म को पर्याप्त नहीं मानते. अब भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का करीब दो प्रतिशत ही ख़र्च किया जा रहा है, जबकि हमारी तरह की अर्थव्यवस्थाएं तीन से पांच प्रतिशत राशि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को आवंटित करती हैं. चूंकि स्वास्थ्य संबंधी बजट के लिए भारत की बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम है, इसलिए इस अंतर को पाटने में आसानी होने की बात विश्लेषक कहते हैं. इसकी पुष्टि के लिए हाल ही में जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़े पेश किए जाते हैं, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बाहरी राहत या मदद के रूप में मिलने वाली राशि मौजूदा स्वास्थ्य ख़र्च (CHE) का सिर्फ 0.66 प्रतिशत है, जो संकेत है कि बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम है. हालांकि, यह सब केवल सैद्धांतिक रूप से है.
वास्तव में, कोरोना महामारी के दौरान USAID ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक मदद की है. कोविड-19 से प्रभावित वर्षों में यह सहायता बढ़ाकर 22.82 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दी गई थी, जबकि उसके पिछले तीन वर्षों में यह राशि औसतन 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर सालाना थी. पहले चरण (अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2022) में ‘निष्ठा’ (स्कूल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल) परियोजना द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मज़बूत करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और 13 राज्यों में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मदद दी गई. दूसरे चरण (मई, 2021 से मई, 2023) में आपातकालीन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने पर ध्यान दिया गया. अप्रैल, 2021 में जब देश डेल्टा लहर का सामना कर रहा था, तब ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग से 50 लाख डॉलर आवंटित किए गए.
USAID ने भारत के संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में भी लगातार मदद की है और बीमारी की जांच-पड़ताल करने, ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल, सामुदायिक जुड़ाव के लिए टूल किट बनाने, साझेदारी संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने, कार्यस्थल पर नीतिगत दखल और टीबी चैंपियन का नेटवर्क बनाने में अपना योगदान दिया है.
उल्लेखनीय है कि खाद्य और कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय महामारी कार्यालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (FAO-OIE-WHO) ‘वन हेल्थ ’ (एक स्वास्थ्य) पहल के माध्यम से मिलकर सहयोग कर रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य से जुड़े हर क्षेत्र को बीमारियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. USAID महामारी के उभरते ख़तरों से निपटने के लिए प्रेडिक्ट (PREDICT) परियोजना चलाती है, जो जूनोटिक वायरस का पता लगाने और खोज करने की इनकी क्षमता बढ़ा रही है. इस कार्यक्रम के तहत महामारी की आशंका का पता तो लगाया ही जाता है, साथ ही प्रमुख वन्यजीव व पशुधन की निगरानी की जाती है और खाद्य सुरक्षा, आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए उन पर निर्भर मानव समुदायों पर नज़र भी रखी जाती है. भारत में इसने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (जब रोगाणु इस तरह खुद को मज़बूत बना लेते हैं कि उन पर रोगाणुरोधी दवाएं, यानी एंटीबायोटिक बेअसर साबित होने लगती हैं) पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने और छह राज्यों में इसके नियंत्रण को मज़बूत करने में भी योगदान दिया है.
‘समग्र’ (SAMAGRA) अभियान शहरी स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो न सिर्फ प्रभावशाली, किफ़ायती और न्यायसंगत कार्यक्रम है, बल्कि इसके तहत कमज़ोर समुदायों पर ध्यान देते हुए शहरी गरीबों को गुणवत्तापूर्वक इलाज और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
इसी तरह, टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, ख़ास तौर से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में. हाल ही में रोटावायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन जैसे नए टीकों की शुरुआत भी की गई है. ‘समग्र’ (SAMAGRA) अभियान शहरी स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो न सिर्फ प्रभावशाली, किफ़ायती और न्यायसंगत कार्यक्रम है, बल्कि इसके तहत कमज़ोर समुदायों पर ध्यान देते हुए शहरी गरीबों को गुणवत्तापूर्वक इलाज और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
आगामी बदलाव और इससे जुड़ी आशंकाएं
भले ही यह मान लिया जाए कि संसाधनों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को फिर से व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती होगी. नेतृत्व और शासन, लक्ष्य तक सेवाओं को पहुंचाना, वित्तपोषण, कार्यबल, चिकित्सा उत्पाद, टीके, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सूचना प्रणाली जैसे कुछ बुनियादी क्षेत्र हैं, जहां हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों में आदर्श बदलाव उसे कहा जाता है, जब उसकी तकनीकी, प्रबंधकीय और राजनीतिक जटिलताओं को दूर करके उनका संचालन आसान बनाया जाता है. इसके लिए ख़ास रणनीति बनाने की ज़रूरत होती है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के पास इस तरह के बदलाव के लिए चरण-दर-चरण रणनीति मौजूद है, जिसमें पहले से ही योजनाएं बनाने का काम होता है. मगर आनन-फ़ानन में प्रशासन और वित्तपोषण को लेकर किया जाने वाला बदलाव कोई आदर्श नहीं माना जाता. अभी ऐसी ही परिस्थिति हमारे सामने है. हम चाहें, तो इससे सबक लेकर पहले से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं. सवाल यही है कि कौन सी राष्ट्रीय या राज्य संस्थाएं इनका प्रबंध करेगी? क्या सरकार और नागरिक समाज आपस में ज़रूरी तालमेल बिठा सकेंगे? अनुमोदन प्रक्रियाएं क्या होगी? क्या सभी कामों में बदलाव होगा? और अगर नहीं, तो कौन-कौन से कामों में बदलाव किए जाएंगे और ये कब होंगे?
इस तरह के बदलावों से जुड़े सभी विकल्पों पर केंद्र और राज्य स्तर पर नीति-निर्माताओं को चर्चा कर लेनी चाहिए और आपस में सहमति बनानी चाहिए. कानूनी संदर्भ और आवश्यकताएं, क्रियान्वयन से जुड़ी राष्ट्रीय नीतियों और उन पर सामाजिक स्वीकृति, देखभाल को सुनिश्चित करते हुए लाभार्थी समुदायों तक पहुंचने की क्षमता और प्रमुख सामाजिक वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले मॉडल का निर्माण- कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर चर्चा अनिवार्य है.
इस राह में कुछ चुनौतियां भी हैं और उनको दूर करना बहुत आसान नहीं है. हमें प्रबंधन की नई व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें कर्मचारियों के अनुबंध, माल एवं सेवाओं की डिलीवरी से जुड़े अनुबंध और कार्यक्रम व वित्त से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तक पहुंच आदि नए सिरे से सुनिश्चित करना होगा. इन अभियानों से जुड़ी एजेंसियां, जो अपना काम जारी रखना चाहेंगी, उनको अपने अनुबंध को लेकर किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़े, इसका भी ख़्याल रखना होगा. उन्हें कार्यक्रम को लेकर नए प्रबंधकों की ज़रूरत पड़ सकती है. बदलाव-प्रक्रिया की समय-सारिणी और अहम बदलावों के संकेतक भी तैयार करने होंगे. जहां तक संभव हो, बाधाओं को टालना होगा और ख़तरों से पार पाने के लिए योजनाएं पहले से तैयार करनी होंगी. वित्त, रिपोर्टिंग, संपत्ति प्रबंधन, खरीद और सॉफ्टवेयर में बदलाव सहित संचालन के नए मैनुअल और प्रक्रियाओं के मानकों (SOP) पर काम करने की भी आवश्यकता होगी.
जहां तक संभव हो, बाधाओं को टालना होगा और ख़तरों से पार पाने के लिए योजनाएं पहले से तैयार करनी होंगी. वित्त, रिपोर्टिंग, संपत्ति प्रबंधन, खरीद और सॉफ्टवेयर में बदलाव सहित संचालन के नए मैनुअल और प्रक्रियाओं के मानकों (SOP) पर काम करने की भी आवश्यकता होगी.
यह कहना गलत नहीं होगा कि ये गंभीर चुनौतियां हैं और हालात बिगड़े, तो कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं. बेशक, भारत का सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक स्कोर कुल 100 में अब बढ़कर 71 हो गया है, जो पिछली बार 66 था. मगर, हमारा देश अब भी कई प्रमुख संकेतकों में पीछे है, जिसमें सुधार के लिए तत्काल काम किए जाने की ज़रूरत है. जिन प्रमुख संकेतकों में पिछड़ने से हम लक्ष्य पाने से चूक सकते हैं, वे हैं- बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, कमज़ोर व अधिक वजन वाले बच्चे, एनीमिया, बाल विवाह, जीवनसाथी द्वारा हिंसा, तंबाकू का उपयोग और आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व ओडिशा के कई जिले इनमें पिछड़े हुए हैं। ऐसे में, USAID बंद होने से कई तरह के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं, जो इन संकेतकों में सुधार में मददगार माने जाते हैं. सवाल है कि जो लाभ हमने अब तक हासिल किया है, क्या हम वहीं तक रुक जाएंगे और असामानताएं बढ़ जाएंगी?
कोरोना के बाद वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. इससे जुड़ी कई गतिविधियों में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन (CDC) मदद करता है, जैसे- एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (IPHL) के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, ‘वन हेल्थ’ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रमुख संक्रामक रोगों से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, AMR के लिए निगरानी व रिपोर्टिंग को मज़बूत करना और फील्ड एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम ( FETP) के माध्यम से कार्यबल के विकास में मदद करना आदि. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल (IHIP) से संबंधित विकास और प्रशिक्षण में भी USAID मदद करता है. कुल मिलाकर, वन हेल्थ संबंधी सोच को मज़बूत बनाने और रोगजनकों के सीमा-पार प्रसार को रोकने पर ज़ोर दिया गया है. क्या इन कार्यक्रमों में अमेरिकी मदद बंद होने के बाद ख़ास बीमारियों में मृत्यु दर बढ़ जाएगी?
अनिश्चितताओं से निपटना
USAID को ‘42 अरब अमेरिकी डॉलर का सॉफ्ट पावर दस्ताना’ कहा जाता है, जो पेंटागन की लगभग ‘900 अरब अमेरिकी डॉलर की हार्ड पावर मुट्ठी’ से बंधी हुई है. USAID की भूमिका को लेकर पूरे दक्षिण एशिया में राजनीतिक विवाद उभर रहे हैं, ख़ास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में. यह तूफ़ान जल्द शांत होने वाला नही है. इसी कारण, केंद्र और राज्य सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि जनहित के स्वास्थ्य कार्यक्रम व प्रतिबद्धताएं दांव पर लगी हैं और बदलाव संबंधी योजनाओं हमें तुरंत तैयार कर लेनी चाहिए. क्या सरकारें कुछ तत्परता के साथ प्रतिक्रियाएं देंगी या सबक सीखने में अब भी अनिच्छा दिखाएंगी?
इबोला संकट ने स्वास्थ्य तंत्र के लचीला होने की ज़रूरत बताई है. लचीला का अर्थ है, मानव जीवन की रक्षा करने में सफल होने और स्वास्थ्य-संकट के दौरान व उसके बाद भी लोगों की सेहत सुधारने वाला तंत्र बनाना. नियमित स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में लचीले स्वास्थ्य तंत्र की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, जिससे सकारात्मक नतीजे मिलते हैं. इसे ‘लचीलापन लाभांश’ कहा जाता है. यह सही है कि भारत के स्वास्थ्य तंत्र में कुछ प्रणालीगत कमजोरियां हैं, लेकिन पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम या कोविड-19 के समय दिखाई गई प्रतिक्रिया इसके लचीलेपन होने का संकेत है. यह लचीलापन स्वास्थ्य तंत्र में जवाबदेही, कार्यबल की प्रतिबद्धता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्निहित अनुकूल तंत्र के रूप में दिखता है. लचीली प्रणालियां ‘वैश्विक स्वास्थ्य में विकास का अगला पायदान’ है. उस लक्ष्य को पाना हमारी ज़रूरत है और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त अवसर भी हैं.
(राजीव दासगुप्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामाजिक चिकित्सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं. वह राष्ट्रीय AEFI, यानी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव संबंधी समिति के सदस्य भी हैं )
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.





 PREV
PREV