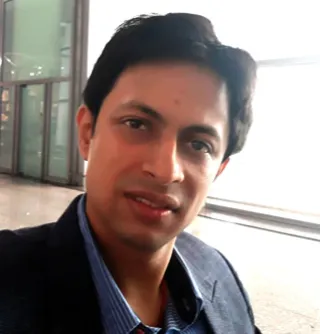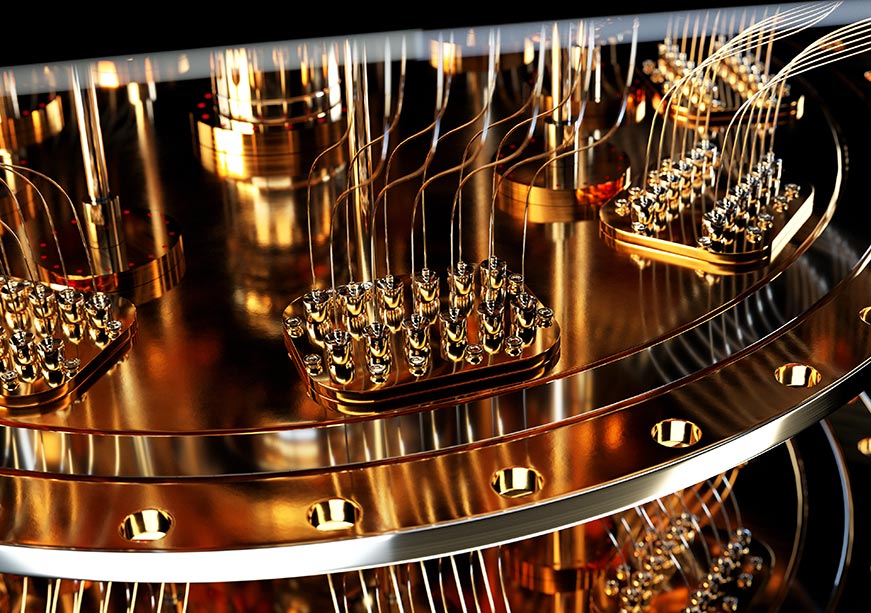रूस के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि तेल निर्यातों से हासिल होने वाले राजस्व में जनवरी में सालाना स्तर पर 46 प्रतिशत की गिरावट हुई है. पड़ोसी यूक्रेन के साथ जारी टकराव के बीच रूस ने ये ख़ुलासा किया है. चीन, भारत और तुर्किए के ख़रीदारों को 15-20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की रियायत दिए जाने के बीच ऐसे हालात सामने आए हैं. इसके साथ-साथ जहाज़ों के द्वारा परिवहन ख़र्च के मद में 15-20 अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वसूली की गई है. हालांकि, व्यापारियों के मुताबिक पहले से ज़्यादा तादाद में जहाज़ संचालकों के प्रवेश से टैंकरों की उपलब्धता बढ़ने के चलते फ़रवरी के महीने से माल ढुलाई दरों में नरमी दिखाई देने लगी है. उधर, हाल के महीनों में यूराल क्षेत्र से समुद्री रास्ते होने वाले निर्यातों का आधे से ज़्यादा हिस्सा जुटा लेने वाले भारतीय निर्यातक ऊंची क़ीमतें देने को तैयार हैं. चीन की ओर से लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते ऐसे हालात बने हैं, क्योंकि चीन भी रूसी कच्चे तेल का आयात करने को तत्पर है. चीन में घरेलू मांग में दोबारा उछाल के चलते ऐसे हालात बने हैं.
रूसी कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात में कटौती की ख़बर ने यूराल की क़ीमतों में उछाल को बढ़ावा दिया. हालांकि मार्च 2022 में रूस ने तेल के उत्पादन में रोज़ाना 5 लाख बैरल की कटौती करने का एलान कर दिया था. उत्पादन में ये कटौती रूस के कच्चे तेल उत्पादन का 5 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 0.5 फ़ीसदी है. ऐसा लगता है कि रूस अब अपने पश्चिमी बंदरगाहों से भी तेल निर्यात में कमी लाने की योजना बना रहा है. फ़रवरी के मुक़ाबले मार्च के आंकड़ों से इसकी तस्दीक़ हो सकती है.
यूक्रेन संकट का पहला साल बीतने के बाद रूस और अमेरिका, दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने पुरज़ोर तरीक़े से कहा है कि वो इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं. पुतिन ने रूस को लंबा खिंचने वाले सैन्य अभियान के लिए "क़दम दर क़दम" तैयार किया है. उधर, बाइडेन ने ज़ोर देकर कहा है कि लोकतांत्रिक यूक्रेन की हिफ़ाज़त की क़वायद में "हम बिना थके" आगे बढ़ते रहेंगे. यूक्रेनी राष्ट्रपति बोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कीव में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान दावा किया कि उनके देश की जीत "निश्चित" और इसे टाला नहीं जा सकता. उनकी इस बात में कितना दम है, ये एक अलग मसला है. हालांकि किसी भी नेता ने युद्ध में अपनी विरासतों को जोड़ते हुए ये साफ़ नहीं किया कि उनके हिसाब से हासिल की जा सकने वाली जीत में कौन-कौन से कारक शामिल रहेंगे. इस जंग का कोई स्पष्ट अंत भी दिखाई नहीं दे रहा.
अमेरिका के पूर्व ख़ुफ़िया अधिकारी और वॉशिंगटन स्थित कार्नेगी एंडाउमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल पीस में रूसी कार्यक्रम के निदेशक यूजीन रोमर के मुताबिक, "रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी शानदार जीत को लेकर हमेशा की तरह वचनबद्ध हैं" जबकि "यूक्रेनी भी पुतिन को परास्त करने को लेकर पहले से कहीं ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, चाहे इसके लिए सबसे ख़तरनाक क़ीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े." हालांकि जीत की अपरिहार्यता पर ज़ोर देना इसे हासिल करने के लिए ज़रूरी साधन और सहायता जुटाने से कहीं ज़्यादा आसान है. युद्ध ख़त्म होने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे में तेल क़ीमतों के अन्य निर्धारक उभरकर सामने आ जाते हैं.
फ़रवरी में चीन की विनिर्माण गतिविधियों में पिछले एक दशक में सबसे तेज़ उछाल दिखाई दी. इसने तेल की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीदों को हवा दे दी है.
फ़रवरी में चीन की विनिर्माण गतिविधियों में पिछले एक दशक में सबसे तेज़ उछाल दिखाई दी. इसने तेल की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीदों को हवा दे दी है. चीन का आधिकारिक मैनुफ़ैक्चरिंग परचेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) फ़रवरी में बढ़कर 52.6 हो गया, जो एक महीना पहले 50.1 के स्तर पर था. नतीजतन तेल की मांग में भारी उछाल की उम्मीद जताने वाले विश्लेषकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. मिसाल के तौर पर IG में तैनात बाज़ार रणनीतिकार का कहना है कि "चीन की PMI में चौंकाने वाला एक और उछाल आने से आर्थिक गतिविधियों में मज़बूती की उम्मीदों को और बल मिला है. इससे तेल की मांग से जुड़ी उम्मीदों में पहले से ज़्यादा आशाजनक परिदृश्य को हवा मिलती है".
दाम पर लगाम
5 दिसंबर 2022 को G7, ऑस्ट्रेलिया और 27 यूरोपीय देशों ने सामूहिक रूप से रूस से जहाज़ों के ज़रिए कच्चे तेल के निर्यात पर क़ीमतों के रूप में लगाम आयद कर दी. इस क़वायद का मक़सद यूक्रेन में संघर्ष के लिए ज़रूरी रकम जुटाने की रूस की क़ाबिलियत को कम करना और वैश्विक स्तर पर स्थिर क़ीमतों को बरक़रार रखना था. यूरोपीय संघ ने पहले से ही समुद्र के रास्ते रूसी कच्चे तेल की ख़रीद पर प्रतिबंध लगा रखा है. क़ीमतों के मोर्चे पर ताज़ा पाबंदी इन क़वायदों को और आगे ले गई है. सैद्धांतिक रूप से इस क़दम का मक़सद तीसरे-पक्ष वाले देशों को रूसी तेल की ख़रीद का मौक़ा देना था, बशर्ते उसके दाम मूल्य स्तर से बाहर ना हों. काफ़ी विचार-मंथन के बाद जनवरी 2023 के मध्य में मूल्य स्तर को 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर तय किया गया. साथ ही हर दो महीने में इसकी समीक्षा किए जाने का भी फ़ैसला लिया गया.
अमेरिका और भारत के बीच इस मसले पर निरंतर परिचर्चा होती आ रही है. इसके बावजूद भारत द्वारा भारी तादाद में रूसी कच्चे तेल का आयात किए जाने का फ़ैसला दोनों देशों के बीच कलह का कारण नहीं बना है. इसकी वजह ये है कि ये तमाम ख़रीद 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की मूल्य सीमा से भारी रियायत पर पूरी हुई. यहां तक कि रूस पिछले साल भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया. दरअसल पश्चिम की ताबड़तोड़ पाबंदियों ने रूस को नए बाज़ारों की खोज करने को प्रेरित किया है.
अमेरिका और भारत के बीच इस मसले पर निरंतर परिचर्चा होती आ रही है. इसके बावजूद भारत द्वारा भारी तादाद में रूसी कच्चे तेल का आयात किए जाने का फ़ैसला दोनों देशों के बीच कलह का कारण नहीं बना है.
बहरहाल, सस्ते तेल से लाभ प्राप्त करने की भारत की क़ाबिलियत के सामने अब मूल्य सीमा से जुड़े उपायों के कठोर क्रियान्वयन की बाधा खड़ी हो गई है. इसमें कोई शक़ नहीं कि भारत शुरू से ही मूल्य सीमा से जुड़े नियमों की पालना करने का इच्छुक नहीं रहा है. ऐसे में तेल की मार्केटिंग करने वाली देसी कंपनियों को भुगतान से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. आयातों के सामने संभावित रुकावटों से बचने के लिए अब उनके द्वारा मूल्य सीमाओं से जुड़े नियमों की पालना के प्रमाण देना ज़रूरी हो गया है. तेल शोधक इकाइयां और बैंकिंग से जुड़े अधिकारी इस दिशा में लगातार बढ़ते उपायों और सत्यापनों का हवाला देने लगे हैं.
कच्चे तेल का मुश्किलों भरा परिदृश्य
2022 में यूक्रेन संघर्ष के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति में आपूर्ति पक्ष से बाधाएं आईं, लेकिन चीन की ओर से मांग में नरमी आने के चलते इसका आसानी से निपटारा हो गया. बहरहाल, अब हालात बदल रहे हैं. लिहाज़ा 2023 में चीनी अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की रफ़्तार और वहां की आर्थिक गतिविधियों का स्तर, तेल क़ीमतों का एक अहम निर्धारक साबित होगा. वैसे तो वर्तमान क़ीमतों में मोटे तौर पर मौजूदा युद्ध के प्रभावों को कारक के तौर पर सामने रखा गया है, लेकिन निकट भविष्य में चीनी मांग से जुड़ी अनिश्चितता के बरक़रार रहने के आसार हैं. स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा के स्रोतों की ओर दुनिया चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है. ऐसे में दीर्घस्तरीय अस्थिरता की संभावना निम्न है.
पिछले कुछ महीनों में मूल्य के स्तर पर भारी-भरकम रुकावटों का अभाव रहा है, ऐसे में आसार यही हैं कि तेल की क़ीमतें 85-90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल (तंग लेकिन ऊंचे स्तर) के इर्द-गिर्द बरक़रार रहेंगी. यहां तक कि मूल्यों में बदलावों से आम परिस्थितियों (जैसा युद्ध की ग़ैर-मौजूदगी में देखने को मिलता) की झलक मिल सकती है. हालांकि व्यापार मार्गों में बदलावों के चलते परिवहन की ऊंची लागतों के बरक़रार रहने के आसार हैं. निश्चित रूप से ये भारत के लिए बद से बदतर हालातों की झलक नहीं दिखाता. बहरहाल, मूल्य सीमा से जुड़े पहले से ज़्यादा कठोर प्रावधानों के अमल के साथ जोड़े जाने पर बेहद सस्ती दरों पर कच्चे तेल की उपलब्धता बहुत जल्द बीते दिनों की बात बन सकती है.
प्रभाव और अनिवार्यता
कच्चे तेल की क़ीमतों में इज़ाफ़े से भारत के चालू खाते के घाटे (CAD) का विस्तार हो सकता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ पड़ सकता है. नतीजतन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाज़ारों में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट का दबाव बन सकता है. वैसे तो भारतीय अर्थव्यवस्था और देश की आर्थिक वृद्धि से जुड़ी क़वायद अब तक मोटे तौर पर लचीली बनी रही है, लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से आर्थिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है. नतीजतन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा बेपटरी हो सकती है. ये हालात कॉरपोरेट सेक्टर की आय और पारिवारिक व्यय में नरमी के रूप में सामने आ सकती है.
महंगे आयातों का मुद्रास्फीति पर होने वाला असर, भारत के 35 करोड़ परिवारों को महसूस होगा. हालांकि निम्न से मध्यम आय वाली श्रेणियों पर इसकी ज़्यादा मार पड़ने की आशंका है. ईंधन की क़ीमतों में उछाल के साथ-साथ रोज़मर्रा के उत्पादों की लागत में बढ़ोतरी के रूप में ऐसे आर्थिक दबावों की झलक मिल सकती है.
महंगे आयातों का मुद्रास्फीति पर होने वाला असर, भारत के 35 करोड़ परिवारों को महसूस होगा. हालांकि निम्न से मध्यम आय वाली श्रेणियों पर इसकी ज़्यादा मार पड़ने की आशंका है. ईंधन की क़ीमतों में उछाल के साथ-साथ रोज़मर्रा के उत्पादों की लागत में बढ़ोतरी के रूप में ऐसे आर्थिक दबावों की झलक मिल सकती है. कच्चे माल की क़ीमतों में बढ़ोतरी के चलते कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों की ऊंची क़ीमतों के ज़्यादातर हिस्से को उपभोक्ताओं तक हस्तांतरित किए जाने की आशंका बनी रहेगी.
किसी भी सूरत में राजकोषीय व्यय में भारी-भरकम बढ़ोतरी से दोहरे घाटे की समस्या पैदा होने का ख़तरा रहेगा. एक ओर उत्पाद करों से हासिल राजस्व में कमी के चलते राजकोषीय घाटे का स्तर ऊंचा रहेगा, दूसरी ओर चालू खाते का घाटा भी ऊंचे स्तरों पर रहेगा. बहरहाल परिवारों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए सरकार को डीज़ल और गैसोलीन पर उत्पाद शुल्क में कटौती करनी पड़ सकती है. ऊंची स्पॉट क़ीमतें तेल डेरिवेटिव क़ीमतों को भी आसमान तक पहुंचा सकती हैं. ऐसे में इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व सक्रियता दिखाते हुए फ़ॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़कर इन जोख़िमों का किसी तरह निपटारा किया जा सकता है. इसके तहत क्रेता और आपूर्तिकर्ता भविष्य के अवसर पर पूर्वनिर्धारित क़ीमतों पर कच्चे तेल को प्राप्त करने या बेचने पर सहमत हो सकते हैं. हालांकि, इस कड़ी में सामने आने वाले प्रतिकूल प्रभावों को अर्थव्यवस्था के तमाम किरदारों को आपस में साझा करना होगा. अकेले सरकार द्वारा इसका असर झेले जाने की उम्मीद लगाना नामुनासिब सोच होगी. लिहाज़ा बचावकारी उपाय के तौर पर राजकोषीय और मौद्रिक मोर्चे पर पूरी सतर्कता के साथ नीतियां तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV