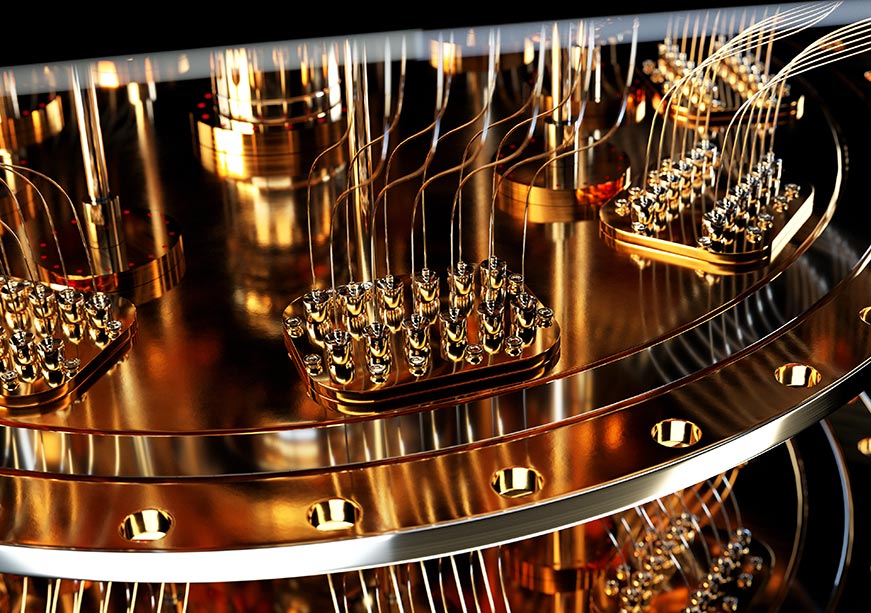कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए लगे मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन का एक प्रभाव ये हुआ है कि वायु प्रदूषण में नाटकीय ढंग से कमी आई है. नासा के हालिया आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पिछले बीस साल में सबसे कम हो गया है. दिल्ली में नुक़सानदेह छोटे कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर लॉकडाउन लागू होने के बाद काफ़ी गिर गया. 20 मार्च को दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 91 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (mg/m3) थी जो 27 मार्च को घटकर 26 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (mg/m3) रह गई.
गाड़ियों के धुएं के साथ और बिजलीघरों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में भी भारी गिरावट देखी गई है. 20 से 27 मार्च के दौरान इसमें 71 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली की हवा अब साफ़ है. आसमान चटख़ नीला दिखता है और हम अपने घर आंगन में दोबारा परिंदों का शोर सुन पा रहे हैं.
एक फ़ौरी चेतावनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ताज़ा अध्ययन से मिली है. इस अध्ययन से साबित हुआ है कि लंबे समय तक प्रदूषित वायु में सांस लेने का सीधा संबंध कोविड-19 से मरने की दर से है. इस अध्ययन से पता चला है कि जो लोग प्रदूषित शहरों में रह रहे हैं, उनके दिल, सांस लेने और अन्य शारीरिक सिस्टम में कमज़ोरी आ जाती है और वो कोविड-19 का सामना कर पाने में कमज़ोर साबित होते हैं
मगर, दुर्भाग्य से ये अस्थायी लाभ हैं. और इन्हें देखकर हमें वायु प्रदूषण के ख़तरों से आंखें नहीं फेर लेनी चाहिए.
वायु प्रदूषण से होने वाले नुक़सान की एक फ़ौरी चेतावनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ताज़ा अध्ययन से मिली है. इस अध्ययन से साबित हुआ है कि लंबे समय तक प्रदूषित वायु में सांस लेने का सीधा संबंध कोविड-19 से मरने की दर से है. इस अध्ययन से पता चला है कि जो लोग प्रदूषित शहरों में रह रहे हैं, उनके दिल, सांस लेने और अन्य शारीरिक सिस्टम में कमज़ोरी आ जाती है और वो कोविड-19 का सामना कर पाने में कमज़ोर साबित होते हैं.
इस स्टडी के नतीजों के बाद, हम भारत के लोगों को बेहद चिंतित होना चाहिए. क्योंकि, दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत के ही नगर हैं. हमारे देश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों से दस गुने से भी ज़्यादा ख़राब है. और कुछ अनुमानों के अनुसार हर साल वायु प्रदूषण के कारण भारत में दस लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है.
इसीलिए, एक तरफ़ अगर भारत कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ़्तार धीमी करने में सफलता प्राप्त करता है. तो, दूसरी ओर हर नीति नियंता के लिए वायु प्रदूषण की रोकथाम करना एक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए. आज के साफ़ सुथरे आसमान हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को मिलना चाहिए. और अगर भारत ये लक्ष्य हासिल करने में सफल रहता है, तो इसके कई लाभ देश को मिलेंगे. हम विश्व स्तर पर प्रतिद्वंदिता के लिए न केवल और सक्षम होंगे, बल्कि, 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत हम जलवायु परिवर्तन रोकने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफल होंगे.
ऐसे कई तरीक़े हैं जिनकी मदद से आर्थिक वृद्धि के लिए दिया जाने वाला पैकेज इस हरित मोर्चे पर सफलता दिला सकता है. उदाहरण के लिए, नए निवेशों को नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगाया जा सकता है. इसके लिए नेशनल सोलर मिशन जैसी योजनाओं के लिए अधिक फंड आवंटित किया जा सकता है. हम भारत स्टेज 4 के मानक समय पर लागू कर सकते हैं. और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इसके बुनियादी ढांचे के विकास की समय सीमा को और कम कर सकते हैं.
बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरियां बनाने वाले कारखानों की स्थापना करके ऊर्जा के स्थानीय विकल्प विकसित किए जा सकते हैं. ऑटो, उड्डयन और निर्माण क्षेत्र की मदद के लिए दिए जाने वाले पैकेज में ऐसे प्रोत्साहन शामिल किए जा सकते हैं, जिनसे साफ हवा और स्वच्छ ऊर्जा के संसाधनों के इस्तेमाल के लक्ष्य निर्धारित हों. रिहाइशी इलाक़ों में ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड (ECBC) को लागू किया जा सकता है. इसके अलावा मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग के क्षेत्र में ऊर्जा कुशलता के नए मानक लागू करने वाली 2011 की एक नीति को इस क्षेत्र की वित्तीय मदद के साथ जोड़ा जा सकता है.
दुनिया का अनुभव ये बताता है कि किसी भी संकट से बदलाव लाने वाला एक राजनैतिक अवसर पैदा करता है. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद चीन ने अपने 568 अरब डॉलर के स्टिमुलस पैकेज का एक तिहाई हिस्सा ऐसे प्रोजेक्ट पर ख़र्च किया था, जो पर्यावरण से संबंधित लक्ष्य हासिल करने में मददगार थे. उसके बाद से चीन आज सौर व पवन ऊर्जा और पनबिजली के क्षेत्र में दुनिया का अगुवा बन गया है.
उस वित्तीय संकट के बाद ब्रिटेन और जर्मनी ने भी पर्यावरण संरक्षण वाले प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया था. इसी तरह, भारत भी कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट का लाभ उठाकर, दूरगामी परिणाम लाने वाले हरित ऊर्जा के सुधार ला सकता है.
आज नीति निर्माताओं, बैंकरों और निवेशकों को इस बात के लिए राज़ी करना आसान हो गया है कि गर्म होते वायुमंडल के कारण दुनिया को आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है. ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित करने वाले पैकेज दुनिया भर में तैयार किए जाएंगे. और पूरी दुनिया की वित्त व्यवस्था इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेगी
हमें इसके लिए समर्थन भी मिल जाएगा. कोविड-19 की महामारी के बाद एक बार फिर से इस बात की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि इससे लगने वाले आर्थिक झटके के कारण बहुत सी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी और अरबों ख़रबों डॉलर के आर्थिक उत्पाद बर्बाद हो जाएंगे. ऐसे में आज नीति निर्माताओं, बैंकरों और निवेशकों को इस बात के लिए राज़ी करना आसान हो गया है कि गर्म होते वायुमंडल के कारण दुनिया को आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है. ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित करने वाले पैकेज दुनिया भर में तैयार किए जाएंगे. और पूरी दुनिया की वित्त व्यवस्था इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेगी.
भारत पहले ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है. यहां तक कि यथार्थवादी पूर्वानुमान ये कहते हैं कि अगले लगभग एक दशक इन गैसों का हमारा उत्सर्जन दोगुना हो जाएगा. ऐसे में अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले पैकेज को अगर पर्यावरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा कि कोविड-19 के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी, तो उससे वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी. इसे पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करने और उससे भी आगे जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी पहल के तौर पर प्रचारित किया जाना चाहिए.
इससे वैश्विक वित्तीय समुदाय के बीच अपना प्रभाव जमाने में भारत को काफ़ी मदद मिलेगी. इस कारण से वैश्विक वित्तीय संगठन भारत को लेकर व्यवहारिक जोखिम लेने का साहस कर सकेंगे. भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग ऐसी करेंगे कि उसे क़र्ज़ लेने में आसानी हो. साथ ही साथ ये संगठन नियामक बाधाओं को दूर करेंगे, जिनके कारण विकासशील देशों में हरित प्रोजेक्ट के लिए पूंजी निवेश में बाधा आती है.
साफ़ हवा के लिए संघर्ष संस्थागत सुधारों की मांग करता है, जो हर क्षेत्र, संस्थान और प्रक्रिया में होने चाहिए.
इसके लिए हर दिशा से निजी और सरकारी निवेश को हरित प्रोजेक्ट की ओर बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
लॉकडाउन के कारण, ज़हरीली गैसों के उत्सर्जन में आई अस्थायी कमी निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है. लेकिन, ये भारत जैसे देश के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है. क्योंकि भारत के सामने पांच ख़रब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है. और वो भी कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा दिए बग़ैर. और हमें बिना सांस रोके इस दिशा में बढ़ चलना चाहिए.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV