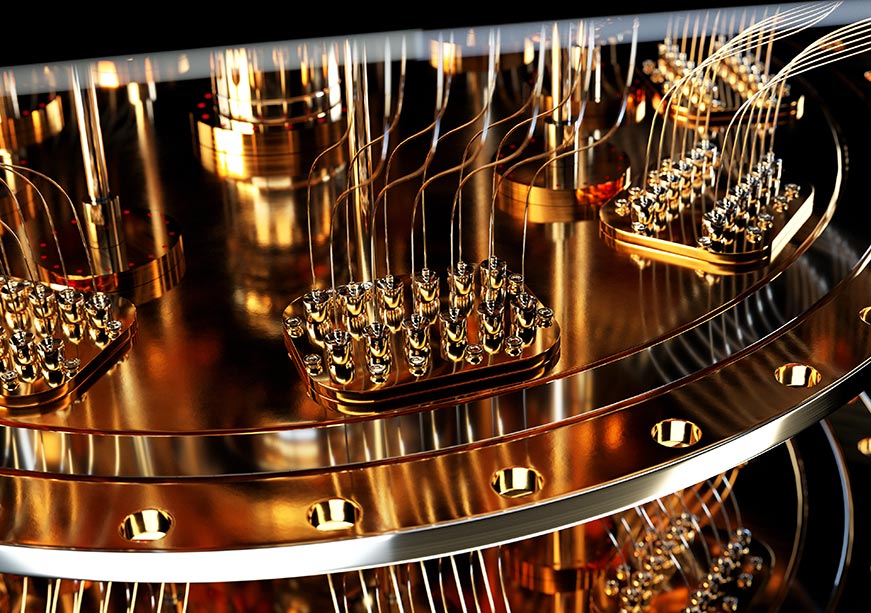Image Source: Kenzo Triboullard — AFP via Getty
(ये लेख ओआरएफ़ के वीडियो मैगज़ीन इंडियाज़ वर्ल्ड के एपिसोड –‘व्यवस्था और उस पर गहराता संकट’, में चेयरमेन संजय जोशी और नग़मा सह़र के बीच हुई बातचीत पर आधारित है).
कोरोना का नया वेरियेंट ओमिक्रोन (omicron) फिर से सुर्खियां बना रहा है. दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसकी खोज की खब़र आते ही जिस तरह से दुनिया के बाकी देश हरकत में आए, उससे सवाल उठता है कि इस महामारी से दुनिया ने अब तक आख़िर कुछ सीखा भी या नहीं?
वैज्ञानिक समुदाय ने COVID-19 के बारे में जो अब तक जो भी सीख ली हो, स्पष्ट है कि शासन तंत्र ने शायद ही कुछ सीखा. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जिस प्रकार ताबड़तोड़ कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाए उस से लगता है वही पुरानी घिसी-पिटी निराशात्मक प्रतिक्रियाएँ दोहराई जाने वाली हैं. लगता है वही देश जो चीन को कोविड के मामले में हमेशा कटघरे में खड़े करने को लालायित रहते थे वे ही स्वयं चीनी हथकंडों के सबसे बड़े अनुयायी बन गए हैं.
वैज्ञानिक समुदाय ने COVID-19 के बारे में जो अब तक जो भी सीख ली हो, स्पष्ट है कि शासन तंत्र ने शायद ही कुछ सीखा. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जिस प्रकार ताबड़तोड़ कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाए उस से लगता है वही पुरानी घिसी-पिटी निराशात्मक प्रतिक्रियाएँ दोहराई जाने वाली हैं
बेचारे दक्षिण अफ्रीका ने तो केवल जिनोम का विश्लेषण कर सबसे पहले ओमिक्रोन जिनोम का अनुक्रम सुनिश्चित कर डाला, वह इस विपदा का रचनाकार कहाँ से बन गया? विपदा तो पहले ही अनेक देशों में, जिनमें अमेरिका और यूरोपीय देश भी शामिल हैं, प्रवेश कर चुकी थी. जिस तरह से तमाम अफ्रीकी देशों को अछूत करार कर उन पर प्रतिबधों की झड़ी लगी, ऐसा लगा मानो कुलीन ब्राह्मणों को भोज कराने में चूक हो गयी. दक्षिण अफ्रीका की ग़लती इतनी भर थी कि जीनोम के अनुक्रम की सूचना उसने तत्काल दूसरे देशों से सांझा कर उन्हें आगाह करने का प्रयास भर किया. बस फिर क्या था. तड़ातड़ इज़रायल, कनाडा, यूके और अमेरिका ने न सिर्फ़ दक्षिण अफ्रीका बल्कि चुनिन्दा अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिये. इनके कारनामों को देखकर तो ये होगा कि भविष्य में शायद ही कोई देश कोविड के संबंध में सूचना सांझा करने के लिये आगे आयेगा. आखिर ये देश अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सूचना क्या देना चाहते हैं? यही न की दक्षिण अफ्रीका के लिए भी चीन सरीखे सूचना देने में आना-कानी का मार्ग ही सर्व-श्रेष्ठ मार्ग होता. बात करिए अब चीन के इन उपासकों से.
WHO ने साफ़ किया है कि इन परिस्थितियों में ट्रैवल बैन जैसे कदमों से कोई लाभ नहीं है. ओमिक्रोन नाम की चिड़िया का वास अफ्रीका नहीं है वह तो न जाने कब की अपने जन्म स्थान से उड़कर फरार हो दुनिया में वास कर रही है. और देखा भी यही गया. सब प्रतिबंधों के बावजूद देशों में रोज़ाना इसके नए नए मामले सामने आने लगे हैं.
कोविड को तो दुनिया में आए अब दो वर्ष होने को हैं. ये क्या आनन फानन में लिए गए निर्णयों का समय है. वास्तव में अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो जो मर्यादाएँ सर्व मान्य हैं उनमें ढिलाई की गुजाईश नहीं है – मास्क का लगातार इस्तेमाल हो, टेस्टिंग की गति बराबर कायम रखी गए, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो.
विज्ञान की राय तो स्पष्ट है – कोविड सरीखे वायरस में म्यूटेशन लगातार होगा, और बार-बार होगा. इस स्थिति का सामना करने को हमें तैयार रहना चाहिए . अंतत: सबसे dominant या प्रमुख वेरियेंट वही रह जाएगा जो मानव के लिए कम घातक हो उसके साथ वास करे. पर प्रकृति की इस प्रक्रिया में समय कितना लगेगा यह बताना असंभव है. संभवतः ओमिक्रॉन ही वह स्ट्रेन हो और संभव है न भी हो. लेकिन ऐसे समय तक हमें लगातार एहतियात बरतनी पड़ेगी – स्पेनिश फ्लू का यही हश्र रहा. इसमें कितना समय लगे? हो सकता है तीन-चार-पांच साल भी लगे. लेकिन इतनी अवधि तक जीवन की गति थामी नहीं जा सकती, हाँ इतना ज़रूर किया जा सकता है कि हर संभव मर्यादा का पालन कर तब-तक बसर किया जाए और जीवन की गति जैसे-तैसे कायम रखी जाए.
कोविड को तो दुनिया में आए अब दो वर्ष होने को हैं. ये क्या आनन फानन में लिए गए निर्णयों का समय है. वास्तव में अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो जो मर्यादाएँ सर्व मान्य हैं उनमें ढिलाई की गुजाईश नहीं है – मास्क का लगातार इस्तेमाल हो, टेस्टिंग की गति बराबर कायम रखी गए, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो. और हाँ, वैक्सीनेशन के मामले में तो गांठ बांध लीजिये कि जब तक सब सुरक्षित नहीं, सब असुरक्षित हैं. कोई भी देश ये सोचने कि ज़ुर्रत न करे कि वह अपनी आबादी के 80% का टीकाकरण कर जंग जीत लिया. सच तो यह है की भले ही नेतागण ताल ठोंके कि दुनिया की एक तिहाई आबादी के वैक्सीन लगाया जा चुका है, अफ्रीका में तो मात्र 6% आबादी को ही वैक्सीन लगाया जा सका है. साल भर से भारत और दक्षिण अफ्रीका की अगुआई में कई देश वैक्सीन की आईपीआर सांझा करने का ज़ोर डाल रहे हैं. वैक्सीन का निर्माण सिर्फ़ चंद देशों या कंपनियों के हाथों में न रहे और इसके निर्माण को और व्यापक किया जाए. विश्व स्वास्थ्य संगठन तो गुहार लगातार लगाता आ रहा है कि बड़े देश टीकों की जमाखोरी बंद करें ताकि ये दूसरे देशों में भी समुचित टीके उपलब्ध कराये जा सकें.
कोरोना तो इस चरमराती विश्व व्यवस्था को चेतावनी है. कोरोना के अलावा आगे और भी गंभीर समस्यायें दुनिया के सामने मुंह बाये खड़ी है जिन से न सिर्फ़ दुनिया का स्वरूप बदल रहा है और चुनौतियां भी जटिल बन रहीं हैं. अगर हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो वास्तव में भविष्य अंधकारमय है.
ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना नए अवतार में प्रकट हो बार-बार आयेगा – अर्थात किसी को भी ककड़ी-खीरा मत समझिए नहीं तो वही बिच्छु बन कर आपको डंक मारेगा. भलाई इसी में है की वैक्सीनेशन में स्पष्ट नजर आ रही परस्पर विषमताओं का जल्द से जल्द अंत हो. सिर्फ एक दूसरे के सहयोग और तालमेल से ही इस महामारी का अंत संभव है. अफसोस आज की विश्व राजनीति और वैश्विक नेतृत्व में अगर कमी है तो यही.
यूं समझिए की कोरोना तो इस चरमराती विश्व व्यवस्था को चेतावनी है. कोरोना के अलावा आगे और भी गंभीर समस्यायें दुनिया के सामने मुंह बाये खड़ी है जिन से न सिर्फ़ दुनिया का स्वरूप बदल रहा है और चुनौतियां भी जटिल बन रहीं हैं. अगर हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो वास्तव में भविष्य अंधकारमय है.
शीत युद्ध के बाद कहीं दुनिया हॉट वॉर की तरफ़ तो नहीं बढ़ रही
चीन और अमेरिका के बीच चले घमासान के मूल में भी यही समस्या है. प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग की शिखर वार्ता अंततः हो तो गयी, पर लगा की दोनों एक दूसरे से कम, अपने-अपने घरेलू दर्शकों को अधिक संबोधित करने में ज्यादा तल्लीन थे. ऐसे में शिखर-वार्ता के दोनों किरदारों को नाटक मंडली के सफ़ल आयोजन का तमगा मिलना चाहिए. दोनों पक्ष सफ़ल हुए यह दिखाने में कि कोई भी किसी से कम नहीं, और दोनों का पलड़ा ऊपर है.
पर भविष्य के बारे में संकेत असपष्ट थे. चीनी दृष्टिकोण से सफ़लता मिली कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी पर अपनी श्रद्धा बरकरार रखी – चीन एक है और ताइवान उसका मात्र एक बिखरा हिस्सा – चीन चाहता भी यही था. वह अपनी वन चाइना पॉलिसी पर अड़ा रहा है और और बाइडेन के आश्वासन से उसे राहत ही मिली होगी. पर साथ ही अमेरिका ने चीन को चेताया ज़रूर कि यदि वह ताइवान पर कोई भी एकपक्षीय कार्रवाई करेगा तो अमेरिका उसका विरोध करेगा – विरोध तो स्पष्ट था पर विरोध सिर्फ़ विरोध ही रहेगा या फिर हस्तक्षेप में परिवर्तित होगा, स्पष्ट नहीं किया गया. मतलब कूटनीति की भाषा में – सियासी धुंध बरकरार रहेगी.
दोनों ही मान गए कि सहयोग करने का ये वक्त नहीं है क्योंकि वर्तमान में दोनों में से किसी भी देश की अंदरूनी राजनीति इस तरह के सहयोग का समर्थन नहीं करेगी. ऐसी स्थिती में यथास्थिति बनी रहे, स्टे-ऑर्डर लगा रहे, बस यही समाधान है और इसी में सम्मान भी.
चीन अपनी ओर से कह ही रहा है कि एकीकरण तो होगा ही, पर शांतिपूर्ण तरीके से. साथ ही यह कि उसे स्वतंत्र ताइवान वाली किसी भी उठी आवाज से परहेज़ रहेगा और ऐसे में व कार्यवाही करेगा.
तो समझिया ताइवान के मसले पर कूटनैतिक धुंध के बीच यथास्थिति कायम है – शिखर वार्ता में स्टे-ऑर्डर मिल गया.
पर नोक-झोंक भी बरकरार है. शिखर सम्मेलन से छूटते ही बाइडेन ने प्रजातांत्रिक देशों के अंतरराष्ट्रीय समिट की घोषणा कर दी – न्योता ताइवान को मिला, चीन को नहीं.
शिखर वार्ता के बाद दोनों ने अपने अलग अलग वक्तव्य जारी किए. अमेरिकी वक्तव्य में लिखा की दोनों देशों की तकरार के मद्देनज़र ज़रूरी था की “गार्ड रेल्स” (Guardrails) स्थापित हों. मतलब अमेरिका और चीन दोनों की तेज़ दौड़ के जोश में कहीं कोई दुर्घटना न कर बैठें. दो कारों की रेस जारी है, दोनों के अपने-अपने दर्शक बैठे हैं, भयानक प्रतिस्पर्धा है, बस ऐसा न हो की स्पर्धा की आंच में दर्शक ही झुलस जाएँ.
दोनों ही मान गए कि सहयोग करने का ये वक्त नहीं है क्योंकि वर्तमान में दोनों में से किसी भी देश की अंदरूनी राजनीति इस तरह के सहयोग का समर्थन नहीं करेगी. ऐसी स्थिती में यथास्थिति बनी रहे, स्टे-ऑर्डर लगा रहे, बस यही समाधान है और इसी में सम्मान भी.
उधर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय प्रजातंत्रों क जमावड़ा कर रहा है इधर चीन चुटकी ले रहा है पश्चिमी प्रजातंत्रों की स्थिति पर. यूरोप की सीमाओं पर भरी संख्या में प्रवासियों ने दस्तक दे रखी है और यूरोप पसोपेश में हैं की इनका किया क्या जाए?
यूरोप पर मंडराता प्रवासियों का सैलाब
आजकल पोलैंड और बेलारूस के बीच यूरोप की सीमा पर खड़े हजारों बेबस प्रवासियों की तस्वीरें समाचारों में छाई हैं. कहा जा रहा है के बेलारूस प्रवासियों का इस्तेमाल यूरोप के खिलाफ़ हथियार के रूप में कर रहा है. वास्तव में यूरोपीय माइग्रेंट क्राइसिस 2021 की देन नहीं है. यह समस्या तो पिछले कई सालों से यूरोप के दरवाजे खटखटा यूरोपीय संघ की नीव हिला रही है. वर्ष 2014-15 से लगातार यूरोप के दरवाज़े पर शरणार्थी दस्तक दे रहे हैं. कई तो समुद्री मार्ग की जोख़िम भरी यात्रा में जल समाधि भी ले चुके है.
इतने निस्सहाय मर्द, औरतों और बच्चों के पलायन का कारण समस्त पश्चिम एशिया और अफ्रीका में फैली अस्थिरता है. आख़िर यह अस्थिरता बढ़ी और फैली क्यों? वास्तव में बड़े और खासकर पश्चिमी देश इस अस्थिरता की ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. 2001 से आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी जंग हो या उसके पहले उपनिवेशवाद के अंत में उपनिवेशकों द्वारा किए गए देशों के अनसुलझे विघटन – कारण कई हैं जिन से इन क्षेत्रों में अशासित भौगोलिक इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि ही हुई है. कई लोग लाचारी में भागने को मजबूर हैं, और इन्हीं की मजबूरी पर सियासी दांव पेंच चल रहे है. याद रहे सीरिया की बदहाली के दौरान तुर्की भी यूरोप को धमका रहा था कि अगर पाश्चिमी ताक़तें सीरिया में उसके हितों को नजरंदाज करेंगी तो वह शरणार्थियों का ऐसा सैलाब तुर्की से वहाँ भेजेंगे कि यूरोप संभाल नहीं पाएगा. बेलारूस और पोलैंड भी उसी क्रम का हिस्सा है. और बेलारूस ही क्यों, इसी दरमियान इंग्लिश चैनल में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच झगड़ा हुआ. यूके और फ्रांस के बीच इंगलिश चैनल में जान गंवा चुके प्रवासियों पर भयानक तू-तू मैं-मैं चली.
2001 से आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी जंग हो या उसके पहले उपनिवेशवाद के अंत में उपनिवेशकों द्वारा किए गए देशों के अनसुलझे विघटन – कारण कई हैं जिन से इन क्षेत्रों में अशासित भौगोलिक इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि ही हुई है. कई लोग लाचारी में भागने को मजबूर हैं, और इन्हीं की मजबूरी पर सियासी दांव पेंच चल रहे है.
आज हम प्रवासियों और शरणार्थियों के दबाव में यूरोप या फिर यूरोपीय संघ के देशों के नैतिक मूल्यों, मूल नियमों, और राजनीति – इन सब में उथल-पुथल होते देख रहे है. शरणार्थी समस्या को लेकर मानो यूरोप का स्वरूप बदलता जा रहा है. यूरोपीय देश जो मानवीय मूल्यों, और अधिकारों की दुहाई देते फिरते थे, एशियाई देशों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने से कभी नहीं चूकते थे, आज अपनी सीमाओं पर खड़े बेसहारा लोगों को मानव तस्करों के शिकार होने का कथा वाचन कर रहे हैं. शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए बनाई गयी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं , जैसे UNHCR और UNHRC, इन देशों की आपसी रस्साकशी में अपने को लाचार पा रही हैं. यूरोपी देश पूरे मसले को मानव तस्करी की समस्या से जोड़ने चाहते हैं, यहाँ तक की ऐसी स्वयं- सेवी संस्थाएं जो इन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हैं उनको भी मानव तस्कर घोषित करने को तत्पर दिख रही हैं. मूल समस्या जिसके कारण पूरी दुनिया में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है उसपर कोई भी देश सीधे तौर पर समाधान तो दूर, चर्चा करने तक को तैयार नहीं. बस आपसी तनातनी के बीच अपनी अपनी रोटियाँ सेकने का काम बदस्तूर जारी है चाहे वो बेलारूस हो या फिर, पोलैंड, या रूस, या फ्रांस और यूके.
जड़ में जाएँ तो पाएंगे की तमाम देशों में, चाहे वे यूरोप, या फिर अमेरिका अथवा एशिया; सब जगह वहाँ स्थित राज्यों के शासन तंत्र नियंत्रण खोते जा रहे हैं, व्यवस्था की देख-रेख करने के लिए निर्मित संस्थाएं कमज़ोर दीख रही हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है.
यूरोपीय संघ लगातार बेलारूस और पोलैंड के बीच लड़ाई को ‘हाइब्रिड युद्ध’ की संज्ञा दे रहा है. रूस और यूरोप पिछले कुछ समय से वन-अपमैनशिप के खेल में लगे हुए हैं और बेलारूस का प्रवासी संकट निश्चित रूप से इस सियासत में काम आया है. लेकिन इस सियासत के बीच फंसे है असहाय महिलाएं और बच्चे जो मात्र एक फेसबुक की पोस्ट के सहारे आस लगाए पोलैंड की सीमा पर उमड़ पड़े . इस अराजकता के भँवर-जाल में सोशल मीडिया भी एक हथियार बन गया है.
प्रवासियों की भीड़ यूरोपीय देशों में फिर से नस्लवाद को जन्म देती दिख रही है और एक बार फिर से नस्लवादी दक्षिण-पंथी दलों का वहाँ उदय हो रहा है. यूरोपीय संगठन के कई देश अपने ही संगठन के मूल्यों से तकरार में हैं – एक सुसंगत इकाई के रूप में यूरोपीय संघ की अखंडता को अभूतपूर्व चुनौती मिल रही है. अभी अभी यूके इस संघ को छोड़ अलग हुआ, और अगर यही हालात रहते हैं तो और देश भी अलविदा कह सकते हैं.
पर समस्या सिर्फ़ यूरोप तक ही सीमित नहीं है.
जिधर नज़र दौड़ाएँ आलम वही
चाहे कोविड-19 की आपदा हो, या अमेरिका-चीन का गहराता द्वंद, या फिर यूरोप की सीमाओं पर उमड़े शरणार्थियों के सैलाब – सब की जड़ में वही पसोपेश है. राज-व्यवस्था की सिमट रही क्षमताओं का क्या उपाय किया जाए? विडम्बना यह की साफ़ झलक आने पर भी इस विषय पर कोई विचार करने को तैयार नहीं. वास्तव में आज विश्वभर के दरवाज़े पर दस्तक देता दैत्य न तो COVID है, न ही यूरोप की सीमाओं पर तैनात शरणार्थी, और न ही अमेरिका और चीन की व्यापारिक तना-तनी. दरवाज़े पर बैठा दैत्य है वैश्विक व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं की चरमराती नींवें, और उन संस्थानों के लगातार अक्षम हो रहे सदस्य-राष्ट्र.
COVID-19 तो मात्र एक अंतिम चेतावनी है – 21 वीं सदी ललकार रही है 20 सदी के लिए निर्मित की गयी राज्य-व्यवस्थाओं को – ललकार रही है कि अशासित खंडित भौगोलिक इकाइयाँ मात्र पश्चिम एशिया, उप-सहारा अफ्ऱीका या अफ़ग़ानिस्तान तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं. वे हर जगह हैं – वे लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की सड़कों पर हैं, वे सभी देशों में मौजूद हैं, वे आज हमारे भीतर घर कर गयी हैं.
COVID-19 तो मात्र एक अंतिम चेतावनी है – 21 वीं सदी ललकार रही है 20 सदी के लिए निर्मित की गयी राज्य-व्यवस्थाओं को – ललकार रही है कि अशासित खंडित भौगोलिक इकाइयाँ मात्र पश्चिम एशिया, उप-सहारा अफ्ऱीका या अफ़ग़ानिस्तान तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं. वे हर जगह हैं – वे लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की सड़कों पर हैं, वे सभी देशों में मौजूद हैं, वे आज हमारे भीतर घर कर गयी हैं.
क्या हम ये ललकार सुन रहे है?
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.




 PREV
PREV