
यह लेख रायसीना फाइल्स 2023 सीरीज़ का हिस्सा है.
वर्तमान दौर में चुनावी लोकतंत्र पर ख़तरा मंडरा रहा है, जैसा कि अमेरिका के दो सबसे बड़े देशों में हाल-फिलहाल में हुई घटनाओं से स्पष्ट होता है. चाहे जनवरी 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स (US) की कैपिटल बिल्डिंग में आक्रोशित लोगों का ज़बरदस्त हमला हो, या फिर हाल ही में ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया में तीन प्रमुख सरकारी इमारतों पर दंगाइयों का हमला. इस घटनाओं से साफ है कि आज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंसा और आतंकवाद के साए में है या फिर कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों की गहरी घुसपैठ हो चुकी है.
अगर संक्षेप में इस पूरे मामले को समझा जाए, तो चुनावी लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें नागरिकों को अपने नेताओं का चुनाव करने और अपनी सोसाइटी की बेहतरी के बारे फ़ैसला में लेने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में भाग लेने का अधिकार मिला हुआ है. आधुनिक राजनीति के एक मज़बूत स्तंभ के रूप में इसकी व्यापक तौर पर मान्यता के बावज़ूद, यह प्रणाली आज ऐसी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जो इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता दोनों को ख़तरे में डालने वाली हैं.
दुनिया में एक बाद एक, जो ताज़ा लोकतंत्र विरोधी घटनाएं सामने आई हैं, उसी कड़ी में Woke के उदय जैसे घटनाक्रम को राजनीतिक के हालिया परिदृश्य के माध्यम से समझा जा सकता है. “Wokeness” या जन जागृति को सामान्य तौर पर इस प्रकार से समझा जा सकता है, जिसमें सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जाती है और एक्टिविज़्म के ज़रिए जनता के बीच चर्चा-परिचर्चाओं से उन मुद्दों के प्रति ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जाती है. देखा जाए, तो इस तरह का आंदोलन वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठानों को चुनौती देने के साथ ही, नस्लवाद, लिंगवाद और होमोफोबिया जैसे मुद्दों को संबोधित करके एक ज़्यादा न्यायसंगत सोसाइटी के निर्माण का प्रयास करता है.
जागरूकता से जुड़ी ‘वोक टॉक’
एक लिहाज़ से जागरूकता से जुड़ी इन ‘वोक टॉक’ में ज़्यादातर 'राजनीतिक रूप से सही' अभिव्यक्तियों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाता है, इसमें प्रतीकात्मकता और किसा ख़ास पहचान, वर्ग, जाति या मजहब से जुड़ी राजनीति को शामिल नहीं किया जाता है. इस सब को न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत अंज़ाम दिया जाता है, जिसके मुताबिक़ प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. जब वोक मुहिम ने अपनी पहुंच, पकड़ और ज़मीन हासिल करना शुरू कर दिया और यह पश्चिम ही नहीं, दुनिया के दूसरे स्थानों पर भी लोगों के दिलो-दिमाग़ पर अपनी छाप छोड़ने लगी, तो अति-दक्षिणपंथी गुटों ने इसको लेकर ना सिर्फ़ अपनी तीखी प्रतिक्रिया जताई, बल्कि इससे मुक़ाबला करने के लिए तत्परता के साथ एकजुट हो गए और राजनीतिक विवादों को पारंपरिक संस्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर भी ले गए. ज़ाहिर है कि पिछले दशक के दौरान सामाजिक ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ऐसे में शायद इस तरह के मुक़ाबले ने हमें इस मौज़ूदा स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया है.
कहा जाता है कि ट्रम्प शासन के दौरान अमेरिका में और बोलसोनारो के सरकार के दौरान ब्राज़ील में शीर्ष अधिकारियों ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया. अगर इस दौरान इन सरकारों ने सरकारी पदों पर अधिकारियों की संदिग्ध नियुक्तियां नहीं की, तो यह निश्चित है कि नौकरशाहों पर दबाव डाला गया और उन्हें उनके मन के मुताबिक़ कार्य नहीं करने के लिए मज़बूर किया गया।
राजनीति में भ्रष्टाचार हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार यह मुद्दा ज़ाहिर तौर पर सभी सीमाओं को पार कर चुका है. कहा जाता है कि ट्रम्प शासन के दौरान अमेरिका में और बोलसोनारो के सरकार के दौरान ब्राज़ील में शीर्ष अधिकारियों ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया. अगर इस दौरान इन सरकारों ने सरकारी पदों पर अधिकारियों की संदिग्ध नियुक्तियां नहीं की, तो यह निश्चित है कि नौकरशाहों पर दबाव डाला गया और उन्हें उनके मन के मुताबिक़ कार्य नहीं करने के लिए मज़बूर किया गया। इतना ही नहीं जब चुनाव का वक़्त आया तो मतदाताओं को लुभाने, डराने, धमकाने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने का भी प्रयास किया गया.
अमेरिका में वर्ष 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनावों में विदेशी ताक़तों पर प्रत्यक्ष रूप से दख़ल देने का आरोप लगाया गया था और जिसमें मुख्य रूप से रूस की विवादास्पद भूमिका शामिल थी. ब्राज़ील के बोलसोनारो को लेकर नई बात यह है कि उन्होंने अपने देश की चुनावी प्रणाली को ही तहस-नहस कर दिया. इस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दूसरे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में खूब शिकायतें कीं, ताकि अगर वो चुनाव हार जाते हैं, तो यह दावा कर सकें कि चुनावों में धोखाधड़ी हुई है. अक्टूबर 2022 में जब वह चुनाव हार गए, तो ठीक ऐसा ही हुआ और उन्होंने कभी अपनी हार नहीं मानी.
चुनाव के नतीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिशें
राष्ट्रपति चुनाव के नतीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए भारी मात्रा में पैसा भी जुटाया गया है, ख़ासकर ब्राज़ील में. वहां के प्रमुख उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने अपने फायदे के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए अलोकतांत्रिक क़दमों और अपमानजनक कृत्यों के प्रति अपनी आंखें मूंद लीं. देश के उद्योगपतियों ने तब तक ऐसा करना जारी रखा, जब तक वे अपेक्षाकृत मज़बूत नागरिक-सैन्य गठजोड़ से मुनाफ़ा कमा सकते थे और जिस पर पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो बहुत अधिक भरोसा करते थे.
अमेरिका और ब्राज़ील दोनों ही देशों में इस बेहद परेशानी वाले परिदृश्य में और इज़ाफा किया, वहां के मीडिया संस्थानों ने, जिन पर ग़लत और मनगढ़ंत सूचनाओं को प्रसारित करने का आरोप है. इन मीडिया संस्थानों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बड़े-बड़े संचार उद्यमों का 'स्वतंत्र' पत्रकारिता के स्रोतों के साथ घालमेल कर एक नए तरह का सूचना इकोसिस्टम बनाने का काम किया, जो कि विश्वसनीय स्रोतों और आंकड़ों पर आधारित होने के बजाए सिर्फ़ ख़ास विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित था.
अगर इस पर ज़ल्द काबू नहीं पाया जाता है, तो यह लहर इस तरह की तबाही लाने वाली साबित हो सकती है, जो आख़िरकार लोकतंत्र को ही पूरी तरह से बदल कर रख देगी, उस लोकतंत्र को, जिसे हम कभी जानते और मानते थे.
आर्थिक असमानता का सवाल इन सभी बातों से ऊपर है. ब्राज़ील और अमेरिका दोनों ही ऐसे देश हैं, जहां कोविड महामारी के दौरान आर्थिक असमानता एक समान तौर पर बढ़ गई, ज़ाहिर है कि ये दोनों कोविड से उपजे स्वास्थ संकट से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में से थे. यह चुनावी लोकतंत्र की मौज़ूदा स्थिति को और भी ज़्यादा ख़तरे में डाल सकता है, क्योंकि सरकार के प्रति असंतोष और अविश्वास बढ़ गया है. उल्लेखनीय है कि संसाधनों के असमान वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुंच के साथ ही तमाम दूसरे तरह के आर्थिक संकटों की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है और जन सामान्य के बीच इसको लेकर ग़लत धारणाएं बनने लगती हैं.
हाल ही में वाशिंगटन और ब्रासीलिया में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए आगे की राह और नागरिकों की रक्षा करने एवं क़ानून का राज बरक़रार रखने के लिए क़ानून लागू करने की क्षमता को लेकर गहरी चिंताएं पैदा की हैं. ये घटनाएं ऐसी हैं, जो समकालीन बहुलतावादी सोसाइटियों की स्थिरता को बनाए रखने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में सशस्त्र बलों, पुलिस व न्यायपालिका जैसे मज़बूत एवं कारगर संस्थानों के महत्त्व को प्रदर्शित करती हैं.
लोकतंत्र विरोधी घटनाएं सिर्फ़ पश्चिमी दुनिया तक ही सीमिति नहीं
हालांकि सच्चाई यह है कि इस तरह की विकृत एवं शर्मनाक लोकतंत्र विरोधी घटनाएं सिर्फ़ पश्चिमी दुनिया तक ही सीमिति नहीं है. चुनावी लोकतंत्र पर सुनियोजित हमले का अगला उदाहरण यूरोप (हंगरी?), एशिया (म्यांमार?) या अफ्रीका में दिखाई दे सकता है. राजनीतिक से जुड़े लोगों के बीच टकराव जहां अतिवाद का रूप ले सकता है, वहीं इस प्रकार की अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिसे कई देशों में पहले कभी नहीं देखा गया है. अगर इस पर ज़ल्द काबू नहीं पाया जाता है, तो यह लहर इस तरह की तबाही लाने वाली साबित हो सकती है, जो आख़िरकार लोकतंत्र को ही पूरी तरह से बदल कर रख देगी, उस लोकतंत्र को, जिसे हम कभी जानते और मानते थे.
सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए यह बेहद अहम हो जाता है कि वे सतर्क एवं सजग बने रहें, साथ ही लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा एवं उनकी मज़बूती के लिए सक्रियता के साथ क़दम उठाएं. ज़ाहिर है कि यह लोकतांत्रिक संस्थान फिलहाल जीवित भी हैं और क्रियाशील भी हैं.
ज़ाहिर है कि इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक समाज और देश ना केवल अपने संस्थानों को मज़बूत करने का काम करें, बल्कि अपने चुनावों की अखंडता और निष्पक्ष की रक्षा करने के साथ अधिक समावेशी और भागीदारी वाली राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भी काम करें. इसे हासिल करने के लिए कई तरह के व्यावहारिक उपायों को अमल में लाया जा सकता है, जैसे कि विश्वसनीय सूचना एवं जानकारी तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना, राजनीतिक प्रक्रिया में आम जनता की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देना. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाए, आर्थिक दिक़्क़तों के मूल कारणों को संबोधित किया जाए और तकनीकी साक्षरता बढ़ाने के लिए निवेश किया जाए.
इन सभी मुद्दों का समाधान तलाशने की दिशा में कार्य करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चुनावी लोकतंत्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की बुनियाद बना रहे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशा की किरण भी बना रहे. इसलिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए यह बेहद अहम हो जाता है कि वे सतर्क एवं सजग बने रहें, साथ ही लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा एवं उनकी मज़बूती के लिए सक्रियता के साथ क़दम उठाएं. ज़ाहिर है कि यह लोकतांत्रिक संस्थान फिलहाल जीवित भी हैं और क्रियाशील भी हैं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.





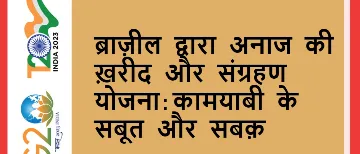
 PREV
PREV


